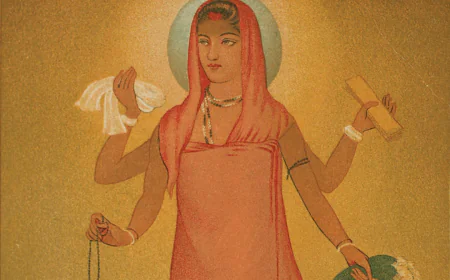कुंभ में कल्पवास की प्राचीन परंपरा
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने भी 1954 में प्रयागराज में कल्पवास किया था। उस समय उनके लिए, किले की छत पर विशेष रूप से एक कैंप स्थापित किया गया था। यह स्थान अब 'प्रेसिडेंट व्यू' के नाम से जाना जाता है।

कुंभ भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं पवित्र आध्यात्मिक समागम है जिसका सनातन धर्म में अपना एक विशिष्ट महत्व है। कुंभ का आयोजन विश्व का सर्वाधिक वृहद धार्मिक समायोजन माना जाता है, जिसमें विश्वभर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। कुंभ मेले में अनेक प्रकार के यम, नियम, दान, ध्यान, स्नान, पूजन आदि आध्यात्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन बहुत निष्ठापूर्वक किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रत्येक 12 वर्ष बाद, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का एवं प्रत्येक 3 वर्ष बाद सामान्य कुंभ का आयोजन भी इन्हीं स्थानों पर किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगने वाले कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है और जब 12 महाकुंभ पूर्ण होते हैं, तो उस कुंभ को पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 वर्ष बाद आता है। वर्तमान में जनवरी 2025 में आयोजित कुंभ मेला पूर्ण महाकुंभ है। भारत में कुंभ की आयोजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। चीनी यात्री ह्यूवेन सांग ने भी अपनी भारत यात्रा के विवरण में कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है।
कुंभ मेले का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। बृहस्पति और सूर्य की खगोलीय स्थिति का कुंभ मेले से बहुत गहन संबंध है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में आने में 12 वर्ष का समय लगता है अर्थात, बृहस्पति द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते है। इसीलिए 12 वर्ष बाद ही पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष का चक्र मानव जीवन में भी विशेष ऊर्जा परिवर्तन को परिलक्षित करता है। यह समय आत्म शुद्धि ध्यान आदि के लिए उत्तम माना जाता है।
कुंभ के मेले का अपना वैज्ञानिक महत्व भी है। वास्तव में पृथ्वी पर जीरो डिग्री से लेकर 300°डिग्री तक जो भी भू-भाग है उस स्थान पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज (centrifugal forces) बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर रहकर घूमने की क्षमता रखता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स( centrifugal forces) कहते हैं और भारत इसी लेटिटूयड (latitude) के अंतर्गत आता है। यहां के कुछ स्थानों पर इस इस बल का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही यह तथ्य जान लिया था। उन्होंने किसी आधार पर ऐसे चार स्थान और खोज निकाले, जहां पर यह बल और भी अधिक है। इन्हीं चार स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन स्थानों की भौगोलिक स्थिति और खगोलीय गणना वातावरण को अत्यंत सकारात्मक और ऊर्जावान बना देती है। यह स्थिति और समय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को उर्ध्वगामी बनाने में सहायक होता है। अतः इन निश्चित स्थानों पर निश्चित समय में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला में बृहस्पति का भी अपना महत्व है। इसका जोवियन इफेक्ट (jovian effect) जब पृथ्वी पर पड़ता है तो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा का ह्रास होता है। जब बृहस्पति की खगोलीय स्थिति के परिवर्तन अनुसार यह प्रभाव हट जाता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा पुनः पृथ्वी पर आने लगती है। इस प्रकार बृहस्पति की अवस्था का भी इस मेले पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति की खगोलीय स्थिति के अनुसार आयोजित मेले में सर्वस्व संत समाज स्नान, ध्यान कर ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। वैसे भी जब हम गीले होते हैं, तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है इसी कारण कुंभ में स्नान का विधान रखा जाता है। मान्यता है कि, इस दिन उच्च लोको के अर्थात स्वर्ग के द्वार भक्तों के लिए खुल जाते हैं। उस समय गंगा का जल औषध पूर्ण एवं अमृतमय हो जाता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के समय ही यह विशेष स्थिति बनती है।
हिंदू समाज के आध्यात्मिक जगत में इस आयोजन का अत्यंत महत्व है। वैदिक मान्यता अनुसार कुंभ में स्नान पर पुण्य प्राप्त होता है जिससे मानव जीवन धन्य हो जाता है। लोगों को मकर-रवि मुहूर्त में, जिसे देवों का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, में स्नान का अवसर प्राप्त होता है। स्नान से पापों का प्रक्षालन और पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः संत समाज, देवताओं के साथ डुबकी लगाने का यह लोभ संवरण नहीं कर पाता और अधिक से अधिक लोग कुंभ में स्नान कर पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं।
पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के पश्चात समुद्र से अनेकों रत्न प्राप्ति के अवसर पर अमृत कलश भी निकाला था। इसी अमृत प्राप्ति हेतु देवों और असुरों में संघर्ष हुआ और इसी छीना-झपटी में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। जिन चार स्थानों पर (प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार एवं नासिक) यह बूंदे गिरी वहीं पर कुंभ का आयोजन सदियों से चला आ रहा है। कल्पवास इसी कुंभ मेले का एक गहन किंतु, कुछ कम प्रसिद्ध आयाम है। यद्यपि कल्पवास सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण साधना है जिसका प्रमुख उद्देश्य आत्म शुद्धि एवं मोक्ष प्राप्ति है। यह साधकों के मानसिक और शारीरिक कायाकल्प की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
कल्पवास
कल्पवास एक संस्कृत शब्द है जिसमे कल्प का अर्थ है ब्रह्माण्डीय युग और वास का अर्थ है निवास करना। कुंभ के संदर्भ में कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर निवास करते हुए नियम पूर्वक ध्यान, साधना, पूजन संकीर्तन व विद्याध्यन करना। प्रयाग राज के कुंभ मेले में कल्पवास का विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है जिसमें गहन आध्यात्मिक अनुशासन के साथ, नियत अवधि में उच्च चेतना की खोज को समर्पित संयमित दैनिक दिनचर्या को महत्व दिया जाता है, जो सामान्य दिनचर्या से नितांत पृथक उस असीम अनंत के साथ तादात्म्य स्थापित करने के अभ्यास का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति को एक नितांत पृथक दिव्य आध्यात्मिक अभ्यास की अनुभूति होती है। साधक तापसिक जीवन शैली अपना कर पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है ।
यद्यपि कुंभ मेला चार प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है किंतु, केवल प्रयागराज ही एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां कल्पवास की परंपरा का विधि पूर्वक निर्वहन किया जाता है। संगम के तट पर एक नियत अवधि का संयमित एवं साधना पूर्ण निवास ही कल्पवास कहलाता है। कल्पवास पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। प्रयागराज में कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है माना जाता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ आरंभ होने वाले लगभग एक माह के कल्पवास में साधक को एक कल्प (ब्रह्मा का एक दिन) के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है । कल्पवास की परंपरा रामायण एवं महाभारत में भी भिन्न-भिन्न नामों से वर्णित है।
वस्तुत: कल्पवास वैदिक संस्कृति की एक अनुपम देन है जिसकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। इसके अंतर्गत अनेक मुनि-मनीषियों द्वारा संगम के तट पर अपनी साधना स्थली का निर्माण कर जप, तप, ध्यान, संकीर्तन आदि का अभ्यास किया जाता था। ऋषि मुनियों ने गृहस्थों के लिए भी कल्पवास का विधान रखा, जिसकी उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास का संकल्प लेने वाले गृहस्थ के लिए संगम तट पर, एक अस्थाई पर्णकुटी निर्मित कर, उसमें नियमबद्ध संयमित निवास करने का नियम है। उपवास करते हुए धैर्य एवं संयम पूर्वक जप, ध्यान, संकीर्तन और भक्ति भाव में संलिप्त रहने का प्रावधान है। पद्म पुराण में भी कल्पवास का उल्लेख मिलता है। कल्पवासी व्यक्ति के लिए सदाचारी, संयम एवं शांत मनोभाव अपेक्षित होता है। जिसे स्नान, दान, हवन आदि सत्कार्यों में ही संलग्न रहना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार कल्पवास का संकल्प करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में, राजा के रूप में जन्म प्राप्त होता है तथा जो मोक्ष की कामना से कल्पवास करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य होती है। कुंभ में कल्पवास के माध्यम से ऋषि मुनि, संत समाज एवं विद्वत समाज एक साथ एकत्रित होकर एक दिव्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समन्वय का सजीव वातावरण निर्मित करते हैं। परिणामस्वरूप कल्पवास में विभिन्न सकारात्मक उर्ध्वगामी ऊर्जा का स्पंदन परिलक्षित होता है। मध्यकाल में यह एक राजकीय संरक्षण प्राप्त महत्वपूर्ण आयोजन बन गया था। राजकीय संरक्षण एवं विभिन्न वर्गों की सहभागिता के कारण कुंभ का सांस्कृतिक महत्व और अधिक समृद्ध होता चला गया। वर्तमान में तो बढ़ती संचार सुविधाओं एवं सामाजिक गतिविधियों ने इस आयोजन को एक वैश्विक समारोह बना दिया है जिसमें समस्त विश्व के कोने-कोने से लोग आकर महाकुंभ का पुण्य लाभ उठाते हैं। इस प्रकार कल्पवास एक प्रतिष्ठित और धार्मिक अनुष्ठान के रूप में विख्यात हो गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी उच्च आत्मिक चेतना को उर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करता है।
यह भी पढ़े- https://sahityanama.com/Meera-and-Krishna-Bhakti
कल्पवास के नियम
कल्पवास सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण साधना है जिसका उद्देश्य आत्म-शुद्धि, आत्म- चिंतन तथा मोक्ष प्राप्ति है जो व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक कायाकल्प की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत संयम, नियम एवं अनुशासन आवश्यक है। संपूर्ण अनुष्ठान में व्यक्ति को सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं और विलासिताओं को त्याग कर, अस्थाई आश्रमों में निवास कर, शुद्ध सात्विक सादा भोजन पर निर्वाह करते हुए भौतिक आकर्षणों से विलग होकर, आंतरिक चेतना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधक नित्य प्रति के दैनिक अनुष्ठान, स्नान, ध्यान, मंत्रों का लयबद्ध उच्चारण, सत्संग, संकीर्तन, आदि द्वारा दिव्य वातावरण एवं आध्यात्मिक पर्यावरण के निर्माण में सहयोग करता है। वैदिक यज्ञ एवं हवन आदि भी कल्पवास का अभिन्न अंग है। हवन की अग्नि का उपयोग पर्यावरण शुद्ध और व्यक्ति की उच्च चेतना के संवर्धन हेतु किया जाता है। कल्पवास के संपूर्ण अनुष्ठान के समय व्यक्ति का सत्यवादी एवं ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। उसमें प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा अपेक्षित है। प्रत्येक दिनचर्या में गंगा स्नान, जप-तप, संकीर्तन, सेवा आदि कार्य अपेक्षित माने जाते हैं। कल्पवासी के लिए भूमि शयन एवं उपवास अथवा एक समय भोजन एवं दान पुण्य आदि शुभ कार्य करने का प्रावधान है। कल्पवास की पूरी अवधि में निद्रा -त्याग आवश्यक है। नियमानुसार संयमित दिनचर्या से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शुद्धता की प्राप्ति होती है एवं उस विराट के प्रति आस्था भक्ति व समर्पण की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।
कल्पवास एक कठिन विधि विधान वाली मोक्षदायनी साधना है जिसमें संयम एवं नियंत्रण की परम आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों पर विस्तृत चर्चा की है। जिसके अनुसार लगभग 45-50 दिनों के कल्पवास के दौरान व्यक्ति को 21 नियमों का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार है- सत्यवादिता, अहिंसा, संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य पालन, व्यसन त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, नित्य प्रति तीन बार गंगा स्नान, त्रिकाल संध्या, पितरों का पिंडदान, अंतर्मुखी जप, सत्संग, दान, संकल्पित क्षेत्र में निवास, निंदा त्याग, साधु सन्यासी आदि संत समाज की सेवा, संकीर्तन, एक समय भोजन या उपवास, भूमि शयन अथवा निद्रा त्याग, अग्नि सेवन का त्याग, देव पूजन, आदि जिसमें व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, देव पूजन, सत्संग और दान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कल्पवास में साधक को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। जिसमें मौन रहकर केवल भजन कीर्तन हुए सत्संग करना चाहिए। सत्य और अहिंसा की संकल्पना के द्वारा व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की मानसिक, शारीरिक हिंसाओं से दूर रहते हुए संयम द्वारा आत्मिक शुद्धि का निर्वहन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य साधक के जीवन को शुद्ध व सात्विक बनता है। दान एवं भिक्षा भी कल्पवास का एक महत्वपूर्ण भाग है जो, व्यक्ति में करुणा और सेवा आदि मानवीय गुणों का संचार करता है। सादा एवं सात्विक भोजन तामसिक प्रवृत्ति को दूर कर व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास का साधन बनता है।
शास्त्रानुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि एक रात्रि की होती है। वहीं तीन रात्रि, 3 महीने, 6 महीने, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। यह साधक की इच्छा और उसके आध्यात्मिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है।
कल्पवास के दौरान तुलसी रोपण का महत्वपूर्ण कार्य भी अवश्य ही संपन्न किया जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। अतः तुलसी रोपण की प्रक्रिया व तुलसी की पूजा कल्पवास का अभिन्न अंग माना जाता है।
कल्पवास का महत्व
कल्पवास एक कठिन भागवत् साधना है जिसमें, व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जहां वह साधना, ईश्वर के प्रति समर्पण द्वारा तन मन एवं आत्मिक शुद्धि का मार्ग खोजता है। कल्पवास करने वाले नदी के तट पर रहते हुए कल्पवास के नियमों का पालन कर ध्यान, संकीर्तन, पूजन करते हुए संत समाज की संगति का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मान्यता अनुसार कल्पवासी के कायिक, वाचिक ,एवं मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुसार किसी व्यक्ति को 100 वर्षों तक अन्न त्याग कर तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य फल के बराबर फल, एक माह के कल्पवास से प्राप्त हो जाता है।
कल्पवास व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है। इस समय व्यक्ति भौतिक सुविधाओं का त्याग कर आत्मिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे ध्यान एवं चेतना की एक उच्च अवस्था की प्राप्ति होती है। इस अवधि में साधक ईश्वरीय अनुकंपा हेतु भक्ति एवं समर्पण के साथ वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा अनंत ब्रह्मांड के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार कल्पवास का अनुभव एक सतत् आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया बन जाता है। जिससे व्यक्ति संयम, अनुशासन, भक्ति जैसे अलौकिक एवं उदात्त गुणों से परिपूर्ण होकर उच्च चेतना का एक प्रकाश पुंज बन सकता है। अतः कल्पवास एक पवित्र एवं दिव्य आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना के विकास एवं शाश्वत सत्य की खोज की ओर अग्रसर होता है। कल्पवास जीवन में अनुशासन एवं संयम को प्रोत्साहन देता है जिसका उद्देश्य मानसिक शुद्धता स्थापित कर जीवन में संतुलन बनाना है।
उद्यापन
कल्पवास की अवधि के पूर्ण होने अर्थात कल्पवास व्रत के समापन के पश्चात उद्यापन का विशेष महत्व होता है। कल्पवास के व्रत समापन के पश्चात गंगा तट पर विशेष पूजा होती है जिसमें कलश पूजन, दीप प्रज्वलन एवं ब्राह्मणों में तिल लड्डुओं का दान आदि सम्मिलित होता है। यह अनुष्ठान समर्पण, संयम, पूजा, एवं संपूर्णता का एक धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक है। उद्यापन के समय साधक गंगा तट पर केले के मंडप में विशेष पूजा का आयोजन करता है। जिसमें सफेद तिल डालकर स्नान किया जाता है। दीप प्रज्वलन के पश्चात संकीर्तन पूजन आदि होता है। यदि पूरा कल्पवास अर्थात 12 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई हो तो, संझियां दान भी किया जाता है। जिसमें ऋषियों अथवा आचार्यों को गृहस्थी की सभी वस्तुओं का दान देकर, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उद्यापन के दौरान एक, तीन या 33 कलश की व्यवस्था कर उनका पूजन किया जाता है। मंत्र जाप के साथ 33 लड्डुओं को घी एवं सोने के साथ दान किया जाता है। कल्पवास से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है एवं व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। मान्यतानुसार कल्पवासी मोक्ष की दिशा की ओर अग्रसर होता है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने भी 1954 में प्रयागराज में कल्पवास किया था। उस समय उनके लिए, किले की छत पर विशेष रूप से एक कैंप स्थापित किया गया था। यह स्थान अब 'प्रेसिडेंट व्यू' के नाम से जाना जाता है।
इस प्रकार कल्पवास की प्राचीन परंपरा मठों एवं आश्रम में गहनता से निहित होने के बावजूद वर्तमान काल में भी सहजता से अनुकरणीय हो गई है। कल्पवास वर्तमान में भी मानव जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर देता है साथ ही सांस्कृतिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित करता है। जिसमें पर्यटक स्वयं को सामान्य पर्यटन स्थलों से पूर्णतया भिन्न संसार में पाता हैं जो उन्हें एक अद्वितीय धार्मिक जीवन और दिव्य सांस्कृतिक अनुष्ठान का अनुभव प्रदान करता है। कल्पवास व्यक्ति को आंतरिक यात्रा की ओर अग्रसर करता है जहां व्यक्ति 'आत्म' की ओर लौटने का प्रयास करता है, ताकि स्वयं को पहचान सके। कल्पवास एक अद्वितीय अनुभव भी है और दिव्य अभ्यास भी। सामान्यतः माना जाता है कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए। यह भारतीय परंपरा की चार आश्रम परंपराओं में से एक वानप्रस्थ की अवस्था वाले गृहस्थों के लिए नियत माना जाता है। कल्पवास सनातन की एक महत्वपूर्ण साधना है जिसमें साधक एवं भक्तगण एक महीने तक नदियो के तट पर संयमित जीवन जीते हैं। कल्पवास साधना के लिए एक नियत अवधि होती है जिसके अंतर्गत संयम एवं अनुशासन से शारीरिक मानसिक कायाकल्प किया जा सकता है। संगम के कल्पवास की सदियों पुराने परंपरा माघ मेले का मुख्य आकर्षण है, जो भक्तों को एक नवीन दिशा प्रदान करती है। कल्पवास व्यक्ति को संन्यास आश्रम का भी अनुभव करवाता है। जहां प्रत्येक दिन एक नियम एक अनुशासन पालना होता है, जो व्यक्ति को संयम, साधना द्वारा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस प्रकार कुंभ मेला और कल्पवास हमारी एक महान सांस्कृतिक विरासत है जो सनातन के शाश्वत मूल्यों की गौरवशाली स्थापना करते हैं।
सीमा तोमर
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0