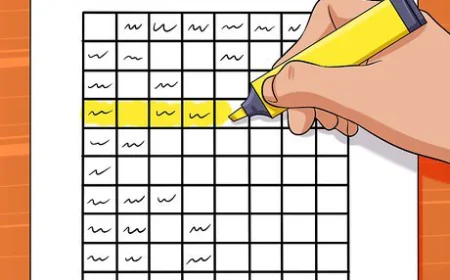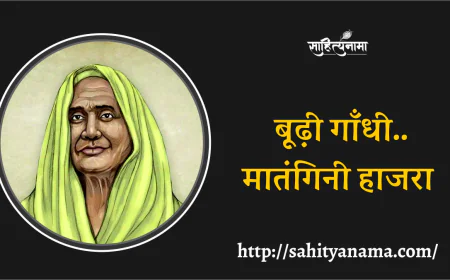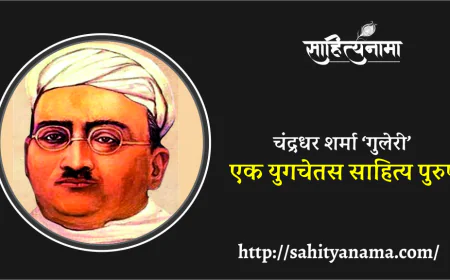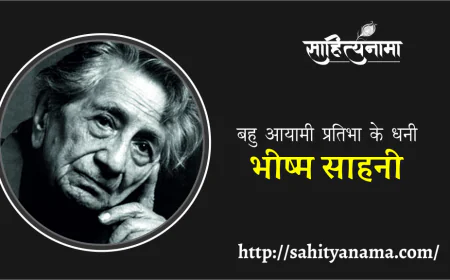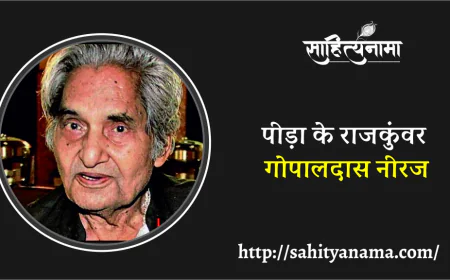आदि शंकराचार्य : भारतीय दर्शन के महान दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक | Adi Shankaracharya: The Great Indian Philosopher and Founder of Advaita Vedanta
Adi Shankaracharya, the founder of Advaita Vedanta, was a great Indian philosopher, saint, and spiritual teacher. He unified Sanatan आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक, भारत के महान दार्शनिक, संत एवं अध्यात्म गुरु थे। उन्होंने सनातन धर्म की एकता स्थापित की और चार प्रमुख मठों की स्थापना कर भारतीय आध्यात्म को सशक्त किया। उनके जीवन, दर्शन और शिक्षाओं का गहन परिचय। Dharma, established four major monasteries, and strengthened Indian spirituality. Explore his life, philosophy, and teachings in depth.

Adi Shankaracharya : आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन और धर्म के इतिहास में एक महान विचारक, संत और दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आचार्य शंकर का जन्म केरल राज्य के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम आर्यम्बा और पिता शिवगुरु थे। अद्वैत वेदांत की पारंपरिक मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य का समय ५वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन अधिकांश आधुनिक विद्वान आदि शंकराचार्य को ८वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध का आचार्य मानते हैं। यह काल निर्धारण (७८८–८२० ई.) सर्वप्रथम के.पी. टिएले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बाद में इसे मैक्स मूलर, मैकडोनेल, पैथोक, डेउसेन और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे विद्वानों ने स्वीकार किया। हाल के वर्षों में अनेक विद्वानों ने (७८८–८२० ईस्वी) की तिथियों पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। उनका तर्क है कि यह काल निर्धारण ऐतिहासिक साक्ष्यों की सीमाओं तथा विभिन्न मठों की परंपराओं से मेल नहीं खाता। अतः शंकराचार्य के काल निर्धारण को लेकर विद्वत-जगत में मतभेद अभी भी विद्यमान हैं। शंकर जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। बचपन से ही उन्हें धर्म, अध्यात्म, दर्शन तथा ज्ञान के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने मात्र आठ वर्ष की अवस्था में वेद-शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया था। पिता शिवगुरु का निधन शंकर के बाल्यकाल में ही हो गया था, शंकर बचपन से ही संन्यास लेना चाहते थे, किंतु माँ इसके लिए तैयार नहीं थीं। एक दिन वह नदी में स्नान कर रहे थे। अचानक एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकर ने माँ से कहा कि यदि वह संन्यास की अनुमति प्रदान करें तो शायद वह बच जाए। माँ ने सहमति दी तभी मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। अपनी माता से संन्यास की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश) जाकर गोविंद भगवत्पाद से संन्यास दीक्षा ली और अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया। कथा के अनुसार जब बालक शंकर गोविंदपादाचार्य के आश्रम पहुँचे, तब गुरु ने उनसे एक गूढ़ प्रश्न किया कि- तुम कौन हो? तब शंकर ने तत्काल छह श्लोकों की रचना की, जिसे निर्वाणषट्कम् कहा जाता है। निर्वाण षट्कम् में उन्होंने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को दर्शाया है अर्थात् आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। आदि शंकराचार्य निर्वाण षट्कम् में कहते हैं- मैं मन नहीं हूँ, न बुद्धि हूँ, और न चित्त। मैं न इंद्रियाँ हूँ, न यह शरीर। मैं न प्राण हूँ, न पंचवायु। न मैं धर्म में बंधा हूँ, न अर्थ, काम या मोक्ष की आकांक्षा रखता हूँ। मैं न सुख-दुख से प्रभावित होता हूँ, न पुण्य-पाप से। मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य स्वरुप हूँ, आत्मा किसी भी लौकिक पहचान से परे है। निर्वाणषट्कम् के ही एक श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं-
‘न मे मृत्युशंका न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः।
न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥‘
अर्थात मुझे न तो मृत्यु का भय है, न ही किसी जाति से भेदभाव है। मेरा न तो कोई पिता है और न ही माता, न ही मैं कभी जन्मा। मेरा न तो कोई भाई है, न मित्र, न शिष्य और न ही गुरु। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि, अनंत शिव हूँ।
शास्त्रों के अध्ययन के साथ भारतवर्ष की परिस्थिति का अध्ययन कर उन्होंने देखा कि संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के मत-मतान्तर है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि उनको संगठित कर एकसूत्र में बाँधा जाये। आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंद भगवत्पाद से संन्यास दीक्षा प्राप्त करने के तत्पश्चात वे अद्वैत वेदांत के प्रचार-प्रसार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ वाराणसी से किया। यहाँ पर उनके ग्रंथों की चर्चा होने लगी। विद्वान पंडित इनकी विद्वत्ता से प्रभावित हुए। विद्वानों से शास्त्रार्थ, चर्चा का क्रम शुरू हुआ। वे भारत के विभिन्न बौद्ध, जैन तथा अन्य दर्शनों के विद्वानों एवं मतावलंबियों के साथ शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदांत की तात्त्विक श्रेष्ठता को स्थापित किया। उस समय भारत विविध धार्मिक संप्रदायों, रूढ़ियों और जातीय भेदभावों से ग्रस्त था। शंकराचार्य ने इन विभाजनों के मध्य एकात्मता स्थापित करने का प्रयास किया और सनातन धर्म को दार्शनिक आधार पर संगठित कर उसे एक सूत्र में बांधने का कार्य किया।
वाराणसी में एक दिन आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक चांडाल अपनी पत्नी और चार कुत्तों के साथ सामने से आ रहा था। उनसे चाण्डाल छू न जाय, अन्यथा वे अपवित्र हो जायेंगे। अतः वे उच्च स्वर में बोले, ‘दूर हटो! दूर हटो!’ यह सुनकर चाण्डाल ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो वेदान्त के अद्वैतवादी मत का प्रचार करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। फिर आपके लिये यह अस्पृश्यता का बोध, भेद-भाव दिखाना कैसे सम्भव हो सकता है? मेरा शरीर छू जाने से आप अपवित्र हो जायेंगे, यह सोच कर आप आशंकित हैं। किन्तु क्या हम दोनों का शरीर एक ही पचतत्त्व के उपादानों से निर्मित नहीं है? आपके भीतर जो आत्मा हैं और मेरे भीतर जो आत्मा हैं, क्या वे एक नहीं है? हम दोनों के भीतर, सभी प्राणियों के भीतर क्या एक ही शुद्ध आत्मा विद्यमान नहीं हैं? आत्मा तो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। फिर यह भेदभाव क्यों? उस चांडाल के इन गहरे और तत्वों से भरे प्रश्नों को सुनकर शंकराचार्य चकित रह गए। उनके भीतर आत्मचिंतन जागा और उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान तो वही है जो इस द्वैत और भेदभाव से परे हो। उसी क्षण उन्होंने पाँच श्लोकों की रचना की, जिन्हें ‘मनीषापंचकम’ कहा जाता है। शंकराचार्य ने स्वीकार किया कि और कहा-
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते,
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी ।
सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्,
चण्डालोस्तु स तु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम।।
जो चेतना जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि तीनों अवस्थाओं के ज्ञान को प्रकट करती है, जो चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित हो रहा है, वहीं चैतन्य चींटी आदि क्षुद्र जन्तुओं तक में स्फुरित है। जिस दृढबुद्धि पुरुष कि दृष्टि में सम्पूर्ण विश्व आत्मरूप से प्रकाशित हो रहा हो. वह चाहे ब्राह्मण हो अथवा चाण्डाल हो, वह वन्दनीय है यह मेरी दृढ़ निष्ठा है। जिसकी ऐसी बुद्धि और निष्ठा है कि मैं चैतन्य हूँ यह दृश्य जगत नहीं वह चाण्डाल हो अथवा ब्राह्मण हो, पर वह मेरा गुरु है।
शंकराचार्य सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी और विनम्र साधक थे। वे जात-पात, ऊँच-नीच के भेद से ऊपर थे और जहाँ कहीं उन्हें आत्मबोध दिखाई देता था, वहाँ वे श्रद्धा से नत हो जाते थे। आदि शंकराचार्य के समय समाज में तांत्रिक क्रियाएँ, चमत्कारवाद, बलि प्रथा तथा विभिन्न अंधविश्वासों का बोलबाला था। वैदिक अनुष्ठानों का महत्व कम होता जा रहा था। हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव, तांत्रिक, कापालिक, पाशुपत, आजीवक आदि में विभाजित होकर विकृत हो चुका था, जिससे धार्मिक और सामाजिक अराजकता फैल गई थी। शंकराचार्य ने इस विघटन और भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु अनेक संप्रदायों के आचार्यों को तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ में पराजित किया और उन्हें अपने अद्वैत दर्शन से प्रभावित कर शिष्य बनाया। कश्मीर के पंडितों, मंडन मिश्र एवं उनकी विदुषी पत्नी भारती, रामेश्वरम के मद्यप ब्राह्मणों, विदर्भ के भैरव अनुयायियों, कापालिकों, जैनाचार्यों, बौद्धाचार्यों और तांत्रिकों तक से उन्होंने शास्त्रार्थ किए और वैदिक धर्म के मूल तत्वों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। शंकराचार्य ने न केवल तांत्रिक व चमत्कारपूर्ण कुप्रथाओं का खंडन किया, बल्कि वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जैसे दार्शनिक ग्रंथों के जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा और सहज तर्कों द्वारा जनसामान्य तक पहुँचाया। उन्होंने मूर्तिपूजा की बाह्य विधियों, धर्म के आडंबर, कर्मकांड के अतिरेक का विरोध करते हुए आंतरिक साधना, निःस्वार्थ सेवा, भक्ति और ज्ञान को धर्म का मूल स्वरूप बताया। उनके अनुसार धर्म अनेक रूपों में हो सकता है, किंतु उसका सार तत्व सत्य, एकात्मता और आत्मबोध ही है। उन्होंने अखिल भारतीय यात्रा कर न केवल शास्त्रार्थों के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, बल्कि यह एक सांस्कृतिक अभियान बन गया, जिसने विभिन्न भाषाओं, संप्रदायों, परंपराओं और जातियों को जोड़ते हुए भारत को आध्यात्मिक एकता के सूत्र में बाँध दिया। उन्होंने सैकड़ों तीर्थ स्थलों, मंदिरों और सांस्कृतिक केन्द्रों का पुनरुद्धार किया तथा देवी-देवताओं की उपासना को आंतरिक साधना से जोड़ते हुए भक्ति को ज्ञान की भूमिका में प्रतिष्ठित किया।
आचार्य शंकर द्वारा रचित लगभग २८० ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद (ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद्), भगवद्गीता आदि पर भाष्य लिखे, और अनेक स्रोतों और ग्रंथों की भी रचना की। शंकर ने बहुत से छोटे अद्वैत ग्रंथों की रचना की है, जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इन ग्रंथों का उपयोग अक्सर शुरुआती लोगों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। शंकर ने बहुत से स्रोत (भजन) भी लिखे हैं। इनमें प्रसिद्ध भज गोविंदम भजन से लेकर दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम तक शामिल हैं। उनके ग्रंथों में विवेकचूडामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेशसाहस्त्री, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, दशश्लोकी, सर्ववेदान्तसिद्धांतसारसंग्रह, वाक्सुधा, पंचीकरण, प्रपंचसारतन्त्र, आत्मबोध, मनिषपंचक और आनन्दलहरीस्त्रोत्र आदि शामिल हैं।
आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थायित्व, एकता और बौद्धिक परंपरा को सुदृढ़ करने हेतु भारत के चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की, वेदों के प्रचार-प्रसार के निमित्त प्रत्येक मठ को एक वेद के अध्ययन-अध्यापन का दायित्व दिया। पूर्व में गोवर्धन पीठ, पुरी (उड़ीसा) के आचार्य पद्मपादाचार्य बनाए गए, यहाँ का वेद ऋग्वेद और महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म है। पश्चिम में शारदामठ, द्वारका (गुजरात) के आचार्य हस्तामलकाचार्य बनाए गए। यहाँ का वेद सामवेद और महावाक्य तत्त्वमसि है। उत्तर में ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ (उत्तराखंड) के आचार्य तोटकाचार्य बनाए गए। यहाँ का वेद अथर्ववेद और महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। दक्षिण में शृंगेरी शारदापीठ, कर्नाटक के आचार्य सुरेश्वराचार्य बनाए गए। यहाँ का वेद यजुर्वेद और महावाक्य अहं ब्रह्मास्मि है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये मठ सनातन धर्म की बौद्धिक, धार्मिक परम्परा के स्तंभ बन गए। मठों का कार्य वेद, उपनिषद और वेदान्त का प्रचार, धर्मशास्त्रों की रक्षा और व्याख्या करना, सनातन परंपरा के अनुसार संन्यासियों को दीक्षा देना और उनका मार्गदर्शन करना, विभिन्न मठों के माध्यम से धर्म की एकता बनाए रखना और विविधता में समरसता का भाव जागृत करना है। शंकराचार्य ने अपने संन्यासियों के लिए एक विशेष अनुशासित व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे दशनामी संप्रदाय कहा जाता है। दशनामी का अर्थ है- दस नामों वाला संप्रदाय। इसके अंतर्गत उन्होंने दस उपाधियों की परंपरा प्रारंभ की जो संन्यासियों को उनकी योग्यता, क्षेत्र, कार्य और मठ परंपरा के अनुसार दी जाती थीं। ये दस उपाधियाँ गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, भारती, पूरी, सरस्वती।
आदि शंकराचार्य का अपनी माता के प्रति प्रेम अत्यंत गहरा था। वे प्रारंभ में ही संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, परंतु यह कदम उन्होंने अपनी माता की अनुमति से ही उठाया। शंकराचार्य ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वे उनका अंतिम संस्कार स्वयं करेंगे। एक संन्यासी के लिए अंतिम संस्कार करना तत्कालीन सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध था। किंतु शंकराचार्य ने इन रूढ़ियों को चुनौती दी और अपनी मां का अंतिम संस्कार स्वयं करके यह सिद्ध किया कि मां के प्रति प्रेम और भावुकता संन्यास के मार्ग में बाधा नहीं है। माता के प्रति इसी भाव को उन्होंने ‘मातृपञ्चकम’ नामक स्रोत में अभिव्यक्त किया है। पाँच श्लोकों के इस स्रोत में उन्होंने मातृत्व की महिमा, अपनी माता के प्रति कृतज्ञता और करुणा के भाव को अत्यंत मार्मिकता से प्रस्तुत किया है।
आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं
तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी ।
एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्य क्षमः
दातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः ।।
अर्थात मुझे जन्म देते समय, हे माता! असहनीय दर्द। आपने अपनी पीड़ा के बारे में नहीं बताया शरीर और न ही आपकी दर्दनाक स्थिति के लिए बिस्तर पर लेटते समय लगभग पूरे साल। उन कष्टों में से एक के लिए भी जो आपने झेले हैं गर्भावस्था के दौरान, हे माँ!, एक बेटा प्रायश्चित करने में असमर्थ है। उस माता को मैं प्रणाम करता हूँ!
आचार्य शंकराचार्य ने वेदांत के अद्वैत मत की स्थापना की। ‘अद्वैत’ का शाब्दिक अर्थ है- द्वैत नहीं, अर्थात केवल एक है। आत्मा (जीव) और परमात्मा (ब्रह्म) वास्तव में एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। आत्मा और परमात्मा अलग-अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, किंतु अज्ञान और माया के कारण आत्मा स्वयं को परमात्मा से पृथक समझती है। शंकराचार्य ने कहा- ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह संसार मिथ्या है। उन्होंने ‘ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः’ का सूत्र दिया। ब्रह्म उस परम सत्ता का नाम है जो नित्य, अपरिवर्तनीय, निराकार और सर्वव्यापक है। ब्रह्म को न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है; वह इंद्रियातीत है, किंतु सब में व्याप्त है। शंकराचार्य माया का सिद्धांत रखते हुए स्पष्ट करते हैं कि माया वह शक्ति है जो ब्रह्म की एकता को छिपा देती है और हमें संसार को भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाती है। जैसे रात में रस्सी को साँप समझने का भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञानवश हम इस संसार को यथार्थ मान बैठते हैं। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह ब्रह्म है, तब उसे मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त हो जाती है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है- ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ। यही आत्म-साक्षात्कार अद्वैत वेदांत का लक्ष्य है।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत की परंपरा आज भी भारतीय अध्यात्म का एक सशक्त स्तंभ बनी हुई है। उन्होंने भारत के चारों कोनों में चार प्रमुख मठों की स्थापना की थी, जिन्हें शंकराचार्य पीठ कहा जाता है। इन मठों के अतिरिक्त देशभर में अनेक उपमठ, अखाड़े, तपोभूमियाँ और आश्रम कार्यरत हैं, जो अद्वैत वेदांत के प्रचार-प्रसार एवं आध्यात्मिक जागरण का कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों के माध्यम से वेद, उपनिषद, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र और अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। साथ ही, यहाँ से अनेक साधक संन्यास ग्रहण कर आचार्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संन्यास परंपरा में दीक्षित होते हैं। वर्तमान समय में इस परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित `आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास' एक उल्लेखनीय पहल है।
इस न्यास का उद्देश्य शंकराचार्य के जीवन-दर्शन एवं अद्वैत ज्ञान का लोकव्यापीकरण कर विश्व में एकात्मता स्थापित करना हैं। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष अनेक प्रतिष्ठित वेदांती गुरुओं के आश्रमों में `अद्वैत जागरण युवा शिविर' का आयोजन किया जाता है, जिसमें १८ से ४० वर्ष की आयु के युवाओं को चयनित कर शिविरों में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को ‘शंकरदूत’ बनाया जाता है, जो पहले स्वयं अद्वैत परंपरा से लाभान्वित होते हैं, आत्मकल्याण करते हैं और फिर उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। अब तक इन शिविरों के माध्यम से हजारों युवा लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर में भाग लेने हेतु ‘एकात्मधाम’ की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य की दीक्षाभूमि ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आचार्य शंकर के जीवन-दर्शन पर आधारित संग्रहालय, ‘अद्वैतलोक’ और अद्वैत वेदांत दर्शन के अध्ययन, शोध एवं विस्तार हेतु ‘आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान’ की स्थापना की जा रही है। यह संस्थान आने वाले समय में शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा को युवाअों एवं आम जनमानस तक पहुंचाएगा, और इसके माध्यम से यह परंपरा एक बार फिर से जीवंत होगी।
राघवेन्द्र प्रताप सिंह
वाराणसी, उत्तर प्रदेश
What's Your Reaction?
 Like
1
Like
1
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0