डिजिटल गिरफ्तारी
पीड़ित को उसके द्वारा किए गए तथाकथित अपराधों के परिणामस्वरूप दंड भुगतने का डर दिखाकर उस पर मानसिक रूप से दबाव डाला जाता है और अंत में घोटालेबाजों द्वारा पीड़ितों को जुर्माने का भुगतान कर मामले से निपटने या फिर कभी-कभी तो कुछ ले देकर मामला रफादफा करने का मार्ग दिखाया जाता है। और ऐसा करने के लिए उनसे कुछ डमी अकाउंट्स में भुगतान कराया जाता है।
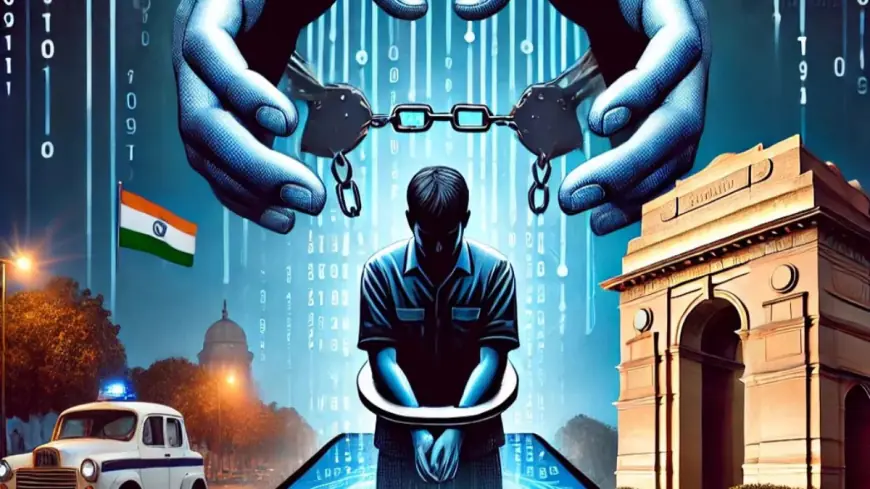
आजकल देश के अलग अलग हिस्सों से कभी समाचार पत्रों तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से डिजिटल गिरफ्तारी के मामले सामने आ रहे हैं। तकनीक व प्रौद्योगिकी प्रधान आज के युग में कई तरह की धोखाधड़ी के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। यूँ तो धोखाधड़ी संभवतः हर युग में होती ही रही होगी किंतु विज्ञान और प्रौद्यौगिकी के इस वर्तमान दौर में इसका स्वरूप भी काफी हद तक बदल गया है। इंटरनेट के इस युग में आजकल धोखाधड़ी भी इंटरनेट के माध्यम से होने लगी है जो साइबर धोखाधड़ी के नाम से जानी जाती है। किंतु इस साइबर धोखाधड़ी के साधनों में भी अब आमूलचूल परिवर्तन होता प्रतीत हो रहा है। गौरतलब है कुछ समय पहले तक ये अपराध किसी से गूगल पे या वाट्सअप पर कोई क्यू आर कोड भेज कर, ओटीपी माँग कर, कोई लिंक भेज कर या फिर क्रेडिट कार्ड इत्यादि से जुड़ी जानकारी माँग कर अंजाम दिए जाते थे किंतु आजकल डिजिटल गिरफ्तारी नामक साईबर अपराध की खबरें धड़ल्ले से सुनने को मिल रही हैं। एक जानकारी के मुताबिक, इस साल डिजिटल गिरफ्तारी की 6000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। यह आँकड़ा इतना चिंताजनक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की है। और तो और गृह मंत्रालय तक को चेतावनी जारी करने और परामर्शी निकालने आवश्यकता पड़ गई है।
डिजिटल गिरफ्तारी ठगी का एक ऐसा नया साधन है जिसे डिजिटली अर्थात् आभासी मंच से अंजाम दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में डिजिटल रूप से मतलब आभासी मंच का प्रयोग कर गिरफ्तारी का झाँसा दिया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो इसमें किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से यह कहकर डराया धमकाया जाता है कि वह किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से गिरफ्तार हो गया है और उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि डिजटल गिरफ्तारी जैसी कोई भी शब्दावली कानून की किसी किताब में नहीं है किंतु आपराधियों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के बढ़ते अपराधिक मामलों के कारण इस शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा है। डिजिटल गिरफ्तारी में लोगों को दो-दो तीन-तीन दिनों तक मोबाइल के सामने बिठा कर रखा जाता है और उनसे बड़ी मात्रा में रकम वसूली जाती है। किंतु आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी किसी को भी इस प्रकार झाँसा दे जाए। सुनने में शायद अटपटा लगे किंतु सच्चाई यह है कि इस प्रकार के अपराध में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि लोग वाकई यह यकीन करने को बाध्य हो जाते हैं कि जो फोन उन्हें आया है वह ठीक है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस तरह के अपराध में अपराधी स्वयं को पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्योरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रवर्तन निदेशालय सहित किसी अन्य सरकारी एजेन्सी के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं। कभी किसी मामले में किसी परिजन के फँसे होने का डर दिखा कर तो कभी कोई ऐसी कहानी गढ़ कर पीड़ित को यह मानने हेतु बाध्य कर दिया जाता है कि वास्तव में उससे या उसके परिजन से कोई अपराध हो गया है।
स्वरूप
डिजिटल गिरफ्तारी में ठगी को अंजाम देने के लिए अपराधियों द्वारा चार-पाँच तरीकों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसमें अपराधी पीड़ित को फोन करके यह बताता है कि वह व्यक्ति या फिर उसका कोई प्रियजन किसी कानूनी मामले में फँस गए हैं। सामान्यतः अपराधी पीड़ित को इन चार-पाँच बातों में उलझाकर ही इस अपराध को अंजाम देता है जैसे कि किसी कुरियर का नाम लेकर कहा जाता है कि आपके नाम एक कुरियर आया है और उसमें गलत अर्थात् प्रतिबंधित सामान है। कुरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से वह फँस सकता है। या फिर यह कहा जाता है कि आपके बैंक खाते से इस तरह के लेनदेन हुए हैं जो वित्तीय धोखाधड़ी के दायरे में आते हैं। इस तरह के मामलों में पीड़ितों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है अर्थात पीड़ित को एक कॉल प्राप्त होती है जिसमें उस पर किसी न किसी अवैध गतिविधि जैसे कि ड्रग्स या नकली पासपोर्ट रखने या कहीं भेजने का, अपने अकाउंट्स से किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठन के साथ पैसों का लेनदेन करने का, किसी प्रतिबंधित वस्तु को कहीं भेजने जैसी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही जाती है। किसी किसी मामले में पीड़ित से यह भी कहा जाता है कि उसके आधार कार्ड से फर्जी सिम निकाली गई है जिसका प्रयोग फर्जी पासपोर्ट बनवाने, जालसाजी करने, मनीलान्ड्रिंग करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स बेचने इत्यादि के लिए किया गया है। तत्पश्चात, वे साक्ष्य मिटाने अथवा बेल के नाम पर पीड़ित से मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। आरोपी द्वारा पीड़ितों पर इतना मानसिक दबाव बना दिया जाता है कि कुछ कुछ मामलों में तो लोगों की मृत्यु तक हो गई है। अभी कुछ समय पहले ही एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एक अध्यापिका को आठ मिनट के अंतराल में दस बार वाट्सअप कॉल आती है जिसमें उन्हें यह कहा जाता है कि उनकी बेटी को पुलिस द्वारा किसी मामले में पकड़ा गया है और यदि वे एक लाख रूपया जमा नहीं करती हैं तो उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला को इस बात का इतना झटका लगा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में वाट्सअप से कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और उसने इस महिला को करीब चार घंटे तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर के रखा था। लोग अक्सर इस तरह के आरोपों से धबरा जाते है और जालसाज उस मामले को बंद करने के लिए पैसों की माँग करते हैं। घ्यातव्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकांश तौर पर पढ़े-लिखे और कानून के जानकार लोगों को फँसाया जाता है और फिर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती माँगी जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी प्रोफेसर जैसा पढ़ा लिखा तबका ज्यादा हो रहा है। सम्पूर्ण भारत से इस प्रकार की मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सेवानिवृत व ऐसे व्यक्ति जिनके परिजन किसी दूसरे शहर या देश में बसे हैं वे इसका शिकार अधिक हो रहे हैं।
कार्यशैली
डिजिटल गिरफ्तारी जैसे अपराध को अंजाम देते समय अपराधी नकली पुलिस अधिकारी या नकली सीबीआई अधिकारी बन कर कॉल करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कॉल भारतीय नम्बर से नहीं की जाती। इस प्रकार की कॉल या तो विदेश के किसी नम्बर से या फिर वाट्सअप के माध्यम से की जाती है। आजकल इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाईट उपलब्ध हैं जहाँ से बड़े आराम से किसी फर्जी नम्बर को जेनरेट किया जा सकता है। इस प्रकार की कॉल अमूमन इसी तरह के फर्जी नम्बरों द्वारा ही की जाती हैं। अपराधी बात करते समय पीड़ित पर कॉल न काटने का दबाव बनाता है और यदि किसी तरह पीड़ित किसी दबाव में आए बिना फोन काट भी देता तो भी बार बार अलग अलग माध्यमों से उसे फोन किया जाता है ताकि उस पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। अक्सर इन कॉल्स में पीड़ित के बच्चे या किसी अन्य प्रियजन के किसी ऐसे मामले में फँस जाने की बात भी की जाती है जिसे छुड़ाने के लिये पैसे दिए जाने की आवश्यकता हो।
इसके अतिरिक्त किसी कुरियर कम्पनी से भी कॉल किया जा सकता है कि आपके नाम से कोई ऐसा पार्सल बाहर भेजा जा रहा है या फिर आया है जिसमें प्रतिबंधिंत वस्तुएँ मिली हैं। इसके अलावा बच्चों के अपहरण जैसी बात भी इन फोन कॉल्स के माध्यम से की जाती हैं। ज़ाहिर है कि कोई भी आम व्यक्ति इस प्रकार की बातों से धबरा ही जाएगा। गौरतलब है कि सामने वाले की भाषा शैली इस प्रकार की होती है कि कोई भी व्यक्ति आराम से उनके झाँसे में आ जाता है। आमतौर पर कानूनी पचड़े में फँसने के डर से या गिरफ्तारी व बदनामी के डर से लोग बिना सोचे पैसे भेज देते हैं। जितनी देर के लिये इन साइबर अपराधियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कॉल काटे डराया धमकाया जाता है तथा जितनी देर तक यह प्रक्रिया चलती है उसे डिजिटल गिरफ्तारी कहा जाता है। डिजिटल गिरफ्तारी में गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीडित को अपने ही घर में कैद कर लिया जाता है। यह डर डिजिटल साधनों मुख्यतौर पर विडीयो कॉल का प्रयोग कर के उत्पन्न किया जाता है इसीलिए इसे डिजिटल गिरफ्तारी कहा जाता है। घोटालेबाज पीडित के बारे में सभी व्यक्तिगत जानकारी जुटा कर रखते है। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराओं का बार बार उल्लेख कर पीड़ित पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं। वे वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन का या फिर ईडी या सीबीआई जैसी किसी सरकारी एजेन्सी जैसा दिखाकर पीड़ित को विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास जो कॉल आई है वह वास्तव में किसी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से ही की गई है। यह यकीन दिलाने के लिए कि जो कॉल वह कर रहे हैं वह फर्जी कॉल नहीं है उनके द्वारा पीड़ितों से ऐप डाउनलोड करवा कर फर्जी डिजिटल फार्म तक भरवाए जाते है। उन्हें डराया जाता है कि आपके पास दो विकल्प हैं कि या तो वे यहीं पर अर्थात् डिजिटल माघ्यम से ही उनसे बात करे यानी की तथाकथित कार्यवाही में सहयोग करें अन्यथा वे वास्तविक रूप से उन्हें गिरफ्तार कर अपने सेन्टर (थाने इत्यादी) में ले जाकर उनसे पूछताछ करेंगें। संभवतः लोक मर्यादा के कारण लोग उनकी बातों में आकर डिजिटल रूप से उनसे तब तक जुड़े रहते हैं जब तक घोटालेबाज स्वयं उन्हें कॉल बंद करने को न कहे या वह स्वयं कॉल न समाप्त कर दे। यह वीडियो कॉल कोई एक दो घंटे नहीं अपितु कई कई घटनाओं में तो तीन-तीन चार-चार दिनों तक चलती रहती है। आरोपी पीडितों की ऑनलाईन मानीटरिंग करते है। इस स्थिति को डिजिटल कारावास कहा जाता है।
डिजीटल कारावास, डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान उत्पन्न हुई वह स्थिति होती है जहाँ स्कैमर्स द्वारा पीड़ितों को उनके साथ तब तक डिजिटल तौर पर जुड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है जब तक की उनकी माँगे पूरी न हो जाँए। कॉल के दौरान घोटालेबाज पीड़ित पर कई गंभीर आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर लिए जाने व उन पर अन्य गंभीर कार्रवाई किए जाने आदि का डर दिखाता है। उसे डराया धमकाया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक की घोटालेबाजों की स्वार्थ सिद्धि न हो जाए।
पीड़ित को उसके द्वारा किए गए तथाकथित अपराधों के परिणामस्वरूप दंड भुगतने का डर दिखाकर उस पर मानसिक रूप से दबाव डाला जाता है और अंत में घोटालेबाजों द्वारा पीड़ितों को जुर्माने का भुगतान कर मामले से निपटने या फिर कभी-कभी तो कुछ ले देकर मामला रफादफा करने का मार्ग दिखाया जाता है। और ऐसा करने के लिए उनसे कुछ डमी अकाउंट्स में भुगतान कराया जाता है।
पहचान कैसे करें
सबसे पहले यह गौर करना है कि आपके पास कॉल किस नम्बर से आ रहा है। जैसे कि यदि कोई भी नम्बर +91 से शुरू हो रहा है तो वह भारतीय नम्बर है और संभवतः उस भारतीय नम्बर से फोन उठाया जा सकता है। इसी प्रकार यह पता लगाया जा सकता है कि जिस नम्बर से फोन आ रहा है वह भारतीय नम्बर है भी अथवा नहीं। किसी भी संदिग्ध नम्बर से की गई कॉल को न उठाने में ही भलाई है। गौरतलब है कि कोई भी सरकारी विभाग जैसे कि पुलिस विभाग या सीबीआई इत्यादि फोन पर इस प्रकार किसी मामले में न तो कोई पूछताछ ही करता ना न ही डरा धमका कर पैसे माँगता है। आमतौर पर डिजिटल गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति सामने वाले को डराता धमकाता है और फोन न काटने की धमकी देता है। ऐसे में सजग रहने की आवश्यकता है कि कोई भी सरकारी प्राधिकारी ऐसा नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कॉल को तुरंत काट कर ब्लॉक करना और तत्काल पास के पुलिस थाने में जाकर इस विषय में जानकारी लेना परमावश्यक हो जाता है। गौरतलब है कि किसी भी स्थिति में अपने बैंक खाते की जानकारी आपको सामने वाले को नहीं देनी है क्योंकि कोई भी सरकारी प्राधिकरण इस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी कभी नहीं माँगता। सजगता और सही समय पर लिया गया विवेकपूर्ण निर्णय ही इससे बचाव का एकमात्र सशक्त साधन है।
निवारण
सर्वप्रथम लोगों को इस मसले के प्रति जागरूक करना ही इसका सबसे कारगर उपाय है। जनता में यह जागरूकता अवश्य ही होनी चाहिए कि साइबर अपराध के दायरे में डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामले भी आते हैं। गौरतलब है कि आज भी लोगों को इस अपराध की कोई जानकारी ही नहीं है और ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में तो इस बाबत स्थिति बहुत ही गंभीर है। कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ लोगों को डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में जागरूकरता होने के बावजूद भी वह ठगी का शिकार हो गए हैं। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कानून प्रवर्तन एजेन्सी डिजिटल गिरफ्तारी नहीं करती। हमारी कानून व्यवस्था में फोन पर गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पुलिस कभी भी किसी को कोई वॉट्सअप कॉल नहीं करती है और न ही कभी भी वॉट्सअप पर एफ आई आर की कॉपी किसी को भेजती है। पुलिस कभी भी पैसे की माँग नहीं करती न ही पैसे व व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए डराती धमकाती है। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बातचीत करने से भी नहीं रोकती।
निवारक कदम
गृह मंत्रालय ने डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों में वृद्धि को देखते हुए एक चेतावनी तो जारी की ही है बल्कि एक परामर्शी भी निकाली है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) का उद्घाटन किया गया है। इस योजना को भारत भर में लागू किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र 14 सी , माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस संगठित अपराध का सक्रिय रूप से सामना कर रहा है। इस कवायद में स्काइप खातों (धोखाधड़ी करने वाले खातों) को ब्लॉक कर दिया जाता है। 14 सी इन धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए गए सिमकार्ड, मोबाइल डिवाइस और मूल खातों को ब्लॉक कर देता है। गृह मंत्रालय ने यह पहचान भी की है कि यह मामले क्रॉस बार्डस अपराध सिंडिकेट के माध्यम से भी किए जाते है अतः इस दिशा में भी सरकार लगातार सक्रिय कदम उठा रही है। सरकार द्वारा साइबर दोस्त नामक एक मंच भी उपलब्ध कराया गया है और ऐसी कोई कॉल आने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर और वेबसाइट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर घटना के संबंध में तुरंत रिपोर्ट किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
यह भी पढ़े -
देवउठनी एकादशी और मांगलिक महत्व
https://sahityanama.com/Devuthani-Ekadashi-and-auspicious-significance
निष्कर्ष
नेहा राठी
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0









































