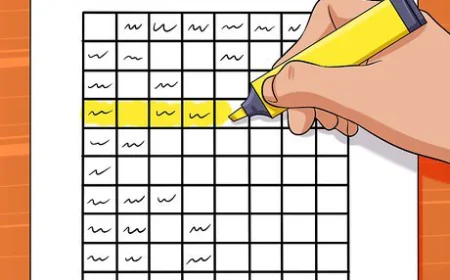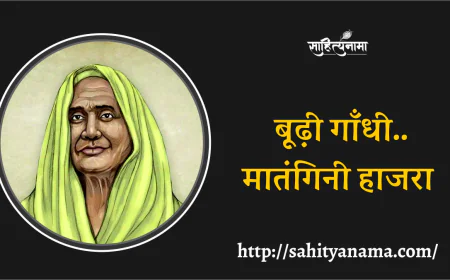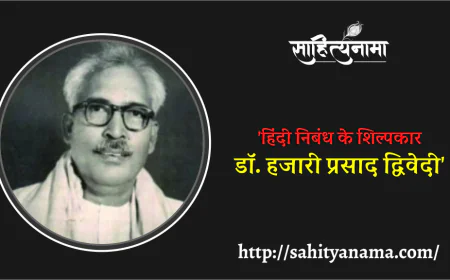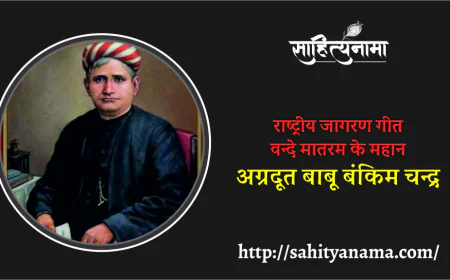साझा पाठशालाएँ गाँव-शहर के बच्चों को एक मंच पर लाने की ज़रूरत : Shared schools are a need to bring children from villages and cities on one platform :
This article highlights the importance of shared schools as a powerful medium to bridge the educational, cultural, and experiential gap between rural and urban children. It fosters tolerance, collaboration, and social understanding among students, promoting inclusive education and social harmony. गांव और शहर के बच्चों के बीच की दीवारें केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी हैं। शहर के बच्चे अक्सर निजी स्कूलों, डिजिटल लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और सांस्कृतिक गतिविधियों से लैस होते हैं। उनके पास इंटरनेट, लैपटॉप और वैश्विक मंचों तक पहुँच होती है। दूसरी ओर, गाँव के बच्चे सरकारी स्कूलों में टूटी बेंचों पर बैठकर, कई बार बिना शिक्षक के, या बिना बिजली के पढ़ाई करते हैं।

Shared schools are a need to bring children from villages and cities on one platform : अक्सर हम सोचते हैं कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित है, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत उसमें छिपी होती है कि वह हमें एक-दूसरे से जोड़ती है, अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को साथ लाती है। पर आज का यथार्थ कुछ और ही कहता है। गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे, दोनों की दुनिया अलग हो चुकी है। एक तरफ जहां शहर के बच्चे तकनीकी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं, वहीं गांव के बच्चे अक्सर संसाधनों की कमी और अवसरों की अभाव में घिरे रहते हैं। क्या हम यही चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई की किताबें ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और संस्कृतियों का संगम भी हो? इसीलिए ‘साझा पाठशालाएँ’ एक अति आवश्यक विचार है, जो इस असमानता की खाई को पाटने का सशक्त माध्यम बन सकती हैं। जब एक गाँव का बच्चा अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए अपनी कहानियाँ सुनाता है और शहर का बच्चा अपनी चकाचौंध भरी दुनिया का अनुभव साझा करता है, तो वह पल सिर्फ दो बच्चों का मिलन नहीं, बल्कि दो अलग-अलग दुनियाओं का संगम होता है। यह संगम केवल शिक्षा को नहीं, बल्कि हमारे समाज को भी समृद्ध करता है।
गांव और शहर के बच्चों के बीच की दीवारें केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भी हैं। शहर के बच्चे अक्सर निजी स्कूलों, डिजिटल लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और सांस्कृतिक गतिविधियों से लैस होते हैं। उनके पास इंटरनेट, लैपटॉप और वैश्विक मंचों तक पहुँच होती है। दूसरी ओर, गाँव के बच्चे सरकारी स्कूलों में टूटी बेंचों पर बैठकर, कई बार बिना शिक्षक के, या बिना बिजली के पढ़ाई करते हैं। यह असमानता केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहती; यह उनके सपनों, आत्मविश्वास और भविष्य को भी प्रभावित करती है। साझा पाठशालाएँ इस खाई को पाटने का एक मौका देती हैं। यदि गाँव और शहर के बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर एक-दूसरे से सीखें, तो न केवल उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि वे एक-दूसरे की जिंदगी, चुनौतियों और सपनों को भी समझेंगे। एक शहर का बच्चा गाँव के बच्चे से खेती, प्रकृति और परंपराओं के बारे में सीख सकता है, जबकि गाँव का बच्चा तकनीक और वैश्विक दृष्टिकोण से परिचित हो सकता है। यह आदान-प्रदान दोनों को समृद्ध करता है और उनके बीच की दूरी को कम करता है।
साझा पाठशालाएँ केवल एक स्कूल भवन में बच्चों को एकत्र करने की बात नहीं हैं; यह एक सामाजिक क्रांति का विचार है। यह वह मंच है जहाँ बच्चे अपनी विभिन्नताओं को सेलिब्रेट करना सीखते हैं। जब एक गाँव का बच्चा अपनी लोककथा सुनाता है और शहर का बच्चा अपनी बनाई डिजिटल कहानी साझा करता है, तो वे एक-दूसरे की दुनिया में झाँकते हैं। यह प्रक्रिया उनके पूर्वाग्रहों को तोड़ती है और उन्हें सहानुभूति, सहयोग और सम्मान की भावना सिखाती है। भारत जैसे देश में, जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और परंपराएँ बदल जाती हैं, साझा पाठशालाएँ एकता की मिसाल बन सकती हैं। यहाँ का बच्चा न केवल अपनी किताबों से सीखता है, बल्कि अपने सहपाठी की जिंदगी से भी सीखता है।
भारत की विविधता इसकी ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी सार्थक है जब इसे एकजुट करने का प्रयास हो। साझा पाठशालाएँ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये स्कूल न केवल शिक्षा को समावेशी बनाते हैं, बल्कि बच्चों को बचपन से ही सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूल में गाँव और शहर के बच्चों के लिए सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जाए, जहाँ दोनों अपनी कला, नृत्य, संगीत और कहानियाँ पेश करें, तो यह उनके बीच की दूरी को कम करता है। ऐसी गतिविधियाँ बच्चों में यह भावना पैदा करती हैं कि उनकी विभिन्नताएँ उनकी ताकत हैं, न कि कमजोरी। इसके अलावा, साझा पाठशालाएँ बच्चों को नेतृत्व, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुण सिखाती हैं, जो भविष्य में एक मजबूत समाज के निर्माण में मदद करते हैं। लेकिन साझा पाठशालाओं का विचार लागू करना इतना आसान नहीं है। कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। भाषाई अंतर एक बड़ी बाधा है। गाँव के बच्चे अक्सर अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, जबकि शहर के स्कूलों में अंग्रेजी या हिंदी का बोलबाला होता है। इसके अलावा, आर्थिक असमानता भी एक चुनौती है। शहर के बच्चे महँगी यूनिफॉर्म और गैजेट्स लाते हैं, जबकि गाँव के बच्चे इनके अभाव में हीन भावना महसूस कर सकते हैं। सांस्कृतिक मतभेद और सामाजिक पूर्वाग्रह भी बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। सरकार और शिक्षण संस्थानों को समावेशी नीतियाँ बनानी होंगी। उदाहरण के लिए, एक समान ड्रेस कोड, डिजिटल संसाधनों का समान वितरण, और शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। इसके अलावा, साझा पाठशालाओं में ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए जो गाँव और शहर की संस्कृतियों को समान महत्व दें।
साझा पाठशालाओं का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह बच्चों को बचपन से ही भेदभाव से दूर रखता है। जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं और एक-दूसरे की मदद करते हैं, तो वे जाति, धर्म, या आर्थिक स्थिति जैसे भेदों को भूल जाते हैं। यह भावना उनके बड़े होने पर भी उनके साथ रहती है, और वे एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो सहिष्णु और समावेशी हो। उदाहरण के लिए, यदि एक गाँव का बच्चा और शहर का बच्चा मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो वे एक-दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। यह अनुभव उन्हें भविष्य में बेहतर सहयोगी बनाता है। आज की वैश्वीकृत दुनिया में, जहाँ सीमाएँ धुंधली पड़ रही हैं, साझा पाठशालाएँ बच्चों को वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करती हैं। वे उन्हें न केवल तकनीकी और शैक्षिक कौशल देती हैं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और सहानुभूति भी सिखाती हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो न केवल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देता है।
साझा पाठशालाएँ केवल एक शैक्षिक प्रयोग नहीं, बल्कि एक सामाजिक सपना है। यह वह सपना है जहाँ गाँव का बच्चा अपनी मिट्टी की ताकत और शहर का बच्चा अपनी आधुनिकता का गर्व एक साथ लेकर चलता है। यह वह सेतु है जो दो अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ता है, और एक ऐसे भारत का निर्माण करता है जो अपनी विविधता में एकता को गले लगाता है। हमें इसे केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानना होगा। क्योंकि जब हम गाँव और शहर के बच्चों को एक मंच पर लाते हैं, तो हम सिर्फ स्कूल नहीं बनाते, बल्कि एक मजबूत, प्रगतिशील और सहानुभूतिपूर्ण समाज की नींव रखते हैं। यह वह समाज है जो न केवल अपने बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि उन्हें एक-दूसरे का सम्मान करना भी सिखाता है। और यही शिक्षा का असली मकसद है।
प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
बड़वानी (म.प्र.)
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0