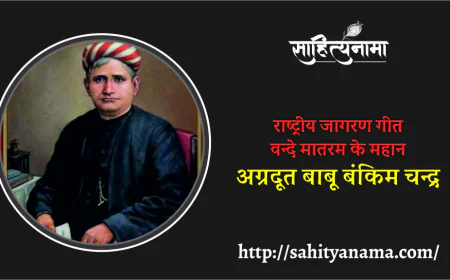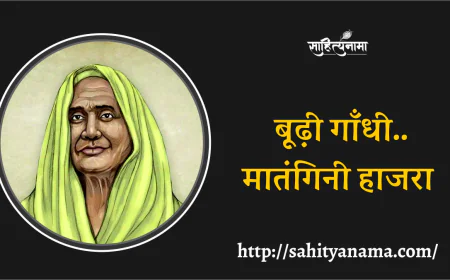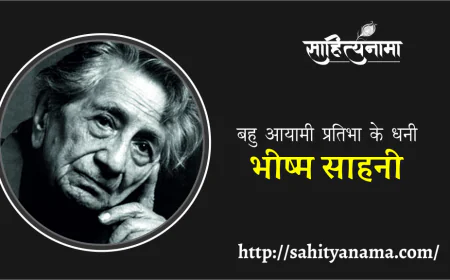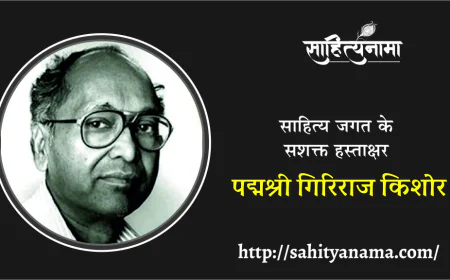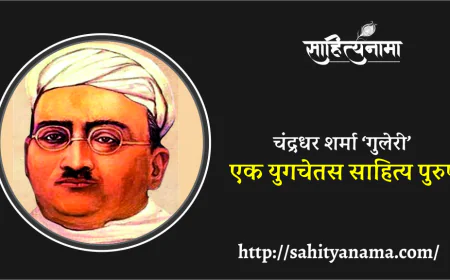भारतीय राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता के प्रेरक :- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
तिलक ने भारतीय समाज के अंदर एकजुटता और जागरूकता लाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उपयोग किया। गणेश उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्होंने भारतीयों को एकत्र किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनके अनुसार स्वराज प्राप्ति के साधन भी स्वराज की धारणा के समान ही शाश्वत सत्य पर आधारित है।
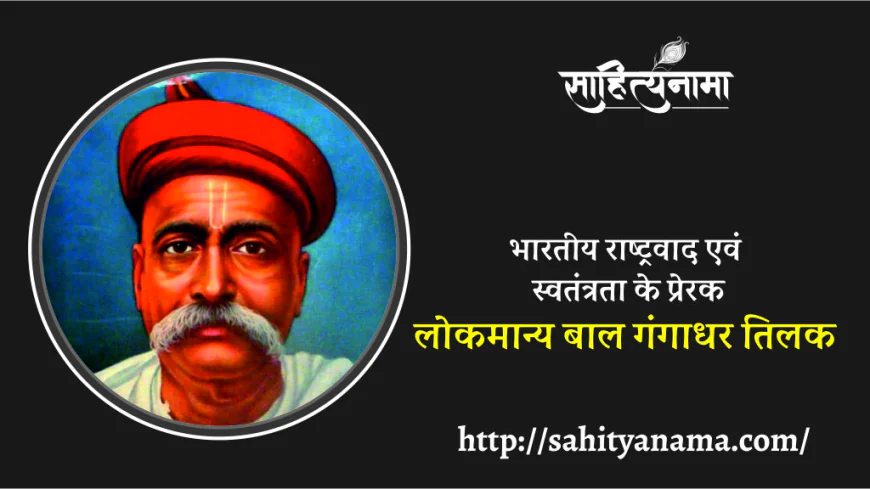
भारतीय राष्ट्रवाद के जनक एवं भारत के स्वातंत्र्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म २३ जुलाई १८५६ ई को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र प्रांत में रत्नागिरी जनपद के एक गांव चिकली में हुआ था। यह आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया। ब्रिटिश शिक्षा के ये घोर आलोचक थे, और मानते थे कि यह भारतीय संस्कृति के प्रति अनादर सिखाती है इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी' की स्थापना की। ताकि भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। तिलक ने अंग्रेजी में `मराठा' तथा मराठी में `केसरी' नाम से दो दैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किया जो जनता में काफी लोग प्रिय हुआ। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता एवं भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की आलोचना की, उन्होंने मांग किया कि ब्रिटिश सरकार तुरंत ही भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी समाचार पत्र में छपने वाले उनके लिखे की वजह से अनेक बार उन्हें जेल भी भेजा गया लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए लेकिन शीघ्र ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। १९०७ ईस्वी में कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में विभक्त हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय एवं श्री विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इन तीनों को `लाल बाल पाल'के नाम से जाना जाता था। १९०८ ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। जिसकी वजह से उन्हें बर्मा स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छुटकर वे पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए एवं १९१६ ईस्वी में एनी बेसेंट जी एवं मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होमरुल लीग की स्थापना की। लोकमान्य तिलक १८९० ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े।अल्पायु में विवाह करने के व्यक्तिगत रुप से विरोधी होने के बावजूद तिलक १८९१ ईस्वी के `एज ऑफ कंसेन्ट' एक्ट के विरुद्ध थे,क्योंकि वे उसे हिन्दू धर्म के अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रुप में देख रहे थे। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को दस वर्ष से बढ़ाकर १२ वर्ष कर दिया। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र `केसरी' में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिखा जिसमें ब्रिटिश नीतियों का बिरोध किया उनको भारतीय दंड संहिता की धारा १२४-ए के अर्न्तगत राज द्रोह के अभियोग में २७ जुलाई १८९७ ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया तथा ६ वर्ष के कठोर कारावास के अर्न्तगत माण्डले (बर्मा) के जेल में बन्द कर दिया गया। ब्रिटिश कारावास के अर्न्तगत तिलक को ६ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।सजा पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल १९१६ ईस्वी में एनी बेसेन्ट की मदद से होमरुल लीग की स्थापना की। इस दौरान उन्हें काफी प्रसिद्ध भी मिली, इस कारण उन्हें 'लोकमान्य' की उपाधि प्राप्त हुई।इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में 'स्वराज्य' की स्थापना करना था। इसमें चार या पांच लोगों की टुकड़ियों बनाई जाती थी जो संपूर्ण भारत में बड़े-बड़े राजनेताओं एवं वकीलों से होमरुल का मतलब समझाया करते थे। लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम ब्रिटिश राज्य के दौरान पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई उन्होने जन जागृति कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए महाराष्ट्र में 'गणेश उत्सव' तथा 'शिवाजी उत्सव' सप्ताह भर मनाना प्रारंभ किया इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम एवं अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरा गया। नागरी प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए तिलक ने संपूर्ण भारत के लिए समान लिपि की समस्या ऐतिहासिक आधार पर नहीं सुलझाई जा सकती। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से दलील दी कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है ।१९०५ ईस्वी में नागरिक प्रचारिणी सभा में उन्होंने कहा था- देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। सन १९१९ ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में भाग लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मान्टेग्यू --चेम्सफोर्ड सुधारो के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल (विधायी परिषद) के चुनाव के बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध ही नहीं किया इसके बजाय लोकमान्य तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारो को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके प्रत्युत्तर पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें । तिलक के लिए स्वराज केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था बल्कि यह आत्मनिर्भर भारतीय संस्कृति की पुर्नस्थापना और भारतीय जनमानस की जागरूकता का भी प्रतीक था। उनका मानना था कि 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' और इसका तात्पर्य था कि भारतीयों को स्वयं अपने देश की सरकार बनाने का हक है ।मांडले जेल से बाहर आने पर तिलक ने स्वराज की मांग को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से होम रुल की स्थापना की सन १९०६ में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग की। परंतु तिलक की धारणा का स्वराज दादा भाई नौरोजी व अन्य उदारवादियों की परिकल्पना के स्वराज से बहुत भिन्न था। स्वराज से तिलक का तात्पर्य था, जनता को सत्ता का तुरंत हस्तांतरण करना जबकि उदारवादी ऐसे छोटे-छोटे सुधारो से संतुष्ट हो जाते थे जिसे विधान मंडलों का विस्तार एवं उनमें निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि आदि। दूसरे तिलक ने स्वराज की मांग को एक ऊंचे नैतिक स्तर पर रखा। उनके लिए स्वराज एक नैतिक अनिवार्यता था। यह मनुष्य के नैतिक स्वभाव की एक अदम्य मांग थी। तिलक ने स्वराज की मांग को धर्म की राष्ट्रीय परंपरा के साथ संयुक्त कर दिया था । उनके लिए स्वराज राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार था। उदारवादी नेताओं के साथ तिलक का मतभेद केवल स्वराज के स्वरूप के विषय में नहीं अपितु उसे प्राप्त करने के साधनों के संबंध में भी था। जबकि उदारवादी प्रार्थना याचिका व विरोध प्रदर्शन जैसे संविधानिक साधनों में विश्वास करते थे, तिलक एक अधिक स्वावलंबी साधन को अपनाना चाहते थे उनका मानना था कि, स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के पास नहीं आती अपितु उसे अनुपयुक्त हाथों से छीनना पड़ता है। संवैधानिक साधनों की निष्फलता का अनुभव करते हुए उन्होंने जन जागरण एवं जन आंदोलन का मार्ग अपनाया। उन्होंने इतिहास से सीखा था कि निरंकुश शासको को जनमत की शक्ति की समक्ष झुकना पड़ता है अतः उन्होंने कांग्रेस को एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति उन्होंने साहित्य का सहारा लिया। तिलक एक सिद्धांत के रूप में अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। अतः उन्होंने क्रांतिकारियों को सदैव तैयार रहने की सलाह देते थे।तिलक की इस संबंध में नीति व्यवहार प्रधान यथार्थवादी थी। यद्यपि तिलक का प्रार्थना और याचिका की पद्धति में कोई विश्वास नहीं था तब भी वह किन्ही परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते थे।
यह भी पढ़े :- अल्फ्रेड टेनीसन (6 अगस्त, 1809– 6 अक्टूबर, 1892)
तिलक ने भारतीय समाज के अंदर एकजुटता और जागरूकता लाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उपयोग किया। गणेश उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्होंने भारतीयों को एकत्र किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तिलक के स्वराज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता था वह चाहते थे कि भारत विदेशी वस्त्रों सामानों और उत्पादन पर निर्भर ना रहे, इसके लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और खादी को प्रोत्साहित किया तिलक ने यह भी महसूस किया की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शिक्षा एवं जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने भारत में शिक्षा प्रसार पर बल दिया और प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धतियों की पुनर्स्थापना की वकालत की। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक कर्तव्य है और एक धर्म भी है उनके अनुसार स्वराज प्राप्ति के साधन भी स्वराज की धारणा के समान ही शाश्वत सत्य पर आधारित है। उनका मानना था कि स्वराज दिया नहीं जाता, बल्कि प्राप्त किया जाता है उनका कहना था कि स्वराज किसी विदेशी सत्ता द्वारा किसी अधीन राज्य को नहीं दिया गया जितने राष्ट्रों ने भी स्वराज प्राप्त किया है उन्होंने अपने प्रयत्नों से ही प्राप्त किया है। याचिका की पद्धति को संघर्ष की पद्धति में बदलकर कर ही किसी राष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। यदि किसी राष्ट्र में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है तो वह निश्चित ही अत्यंत पिछड़ा हुआ है। स्वराज के लिए तिलक क्रियात्मक उपाय को अपनाने पर बल देते हैं। लोकमान्य तिलक आधुनिक भारत के महान निर्माता थे।
देश भक्ति उनका धर्म था और भारत माता की इष्ट देवी थी। लोकमान्य तिलक के स्वराज की अवधारणा भारतीय राजनीतिक और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनका विचार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था बल्कि यह समग्र दृष्टिकोण से था जिसमें समाज,संस्कृति, शिक्षा और आत्म- निर्भरता के तत्व जुड़े हुए थे। एक अगस्त १९२० ईस्वी को मुम्बई में इस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। वर्तमान में भी उनके विचार भारतीय राजनीति और समाज के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तिलक के विचारों और कार्यों का राष्ट्रीय पुनर्जागरण व राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन मार्ग नवीन ऊर्जा और नवीन चेतना प्रदान किया।
डाॅ. जितेन्द्र प्रताप सिंह
रायबरेली,उ.प्र.
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0