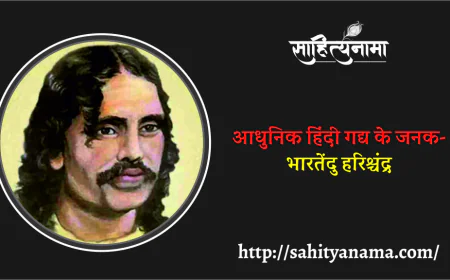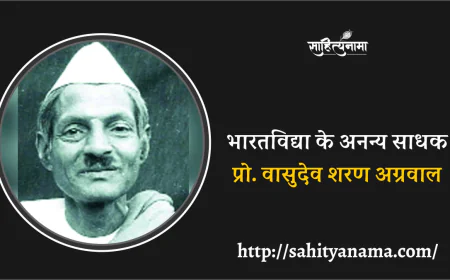यात्रा संस्मरण : "बनारस की गलियों में अवतरण”
बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीवंत अनुभूति है, जो आत्मा को गहराई से छूती है। पिता जी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थे- अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। बनारस की धूल-धूसरित सड़कों और इसके अल्हड़पन के बीच उनके जीवन का कठिन संघर्ष मुझे सिखाता रहा कि कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है

जब मैं इस दुनिया में आया, तो मेरा जन्म स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी। यह थी काशी, जिसे आज के समय में बनारस कहा जाता है। यह वह नगरी है, जो आदि-अनादि काल से मोक्ष की प्रतीक बनी हुई है। इस शहर के हर कण में आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई है, और इसी पवित्र धरा पर मेरी यात्रा आरंभ हुई। गंगा की लहरों की ठंडी फुहार, मंदिरों में गूंजती मंत्र ध्वनियाँ, और संकरी गलियों में बसी अपरंपार ऊर्जा ने मेरे बचपन को एक अद्भुत अनुभूति दी। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक जीवंत अनुभूति है, जो आत्मा को गहराई से छूती है।
पिता जी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थे- अनुशासन उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। बनारस की धूल-धूसरित सड़कों और इसके अल्हड़पन के बीच उनके जीवन का कठिन संघर्ष मुझे सिखाता रहा कि कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है। उनके कठोर व्यवहार के पीछे जो ममतामयी भावना थी, वह समय के साथ धीरे-धीरे स्पष्ट होती गई। अम्मा का व्यक्तित्व इसके विपरीत था- वे धर्मपरायण थीं, परंतु उनकी सोच आधुनिक और प्रगतिशील थी। उन्होंने हमें संस्कार दिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख दी, और यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक सफलता है।
सात भाई-बहनों के बीच सबसे छोटा होने के नाते मैं परिवार का `पेट पोछना' था। बड़े भाई-बहनों का स्नेह अपार था, परंतु इस स्नेह के साथ एक अदृश्य अपेक्षा भी था- एक ऐसा भार जो प्रेम के आवरण में छिपा हुआ था। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और मैं बनारस से दूर चला गया। गाजीपुर, बलिया, जौनपुर होते हुए जीवन मुझे गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली और न जाने कितने शहरों में ले गया। चौबीस वर्षों की इस यात्रा में बहुत कुछ पीछे छूटता गया- वह गलियां, वह अल्हड़ मस्ती, वह बेफिक्री और सबसे ज्यादा, वह आत्मीयता जो सिर्फ बनारस की हवाओं में घुली मिलती है।
जीवन ने बहुत कुछ दिया- एक सुंदर परिवार, पत्नी और दो प्यारे बच्चे, जिन्होंने मेरे जीवन में नए रंग भरे। परंतु, जीवन ने बहुत कुछ छीन भी लिया। पापा, अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब और दोनों छोटी भाभियाँ हमेशा के लिए इस संसार को अलविदा कह गए। जीवन की आपाधापी में बनारस छूटता गया, लेकिन बनारस कभी मुझसे दूर नहीं हुआ। वह हर समय मेरे भीतर कहीं गहरे बसा रहा, जैसे गंगा की धारा सदियों से बहती आ रही हो, अपने तटों पर स्मृतियों की लहरें उठाती हुई।
बनारस की अल्हड़ता, उसकी ठहरी हुई सादगी, और उसमें बसी मस्ती बार-बार मुझे बुलाती थी। मन करता था कि एक बार फिर से उन गलियों में भटकूँ, उस घाट की सीढ़ियों पर बैठूँ, किसी चायवाले की दुकान पर बिना वजह घंटों बिताऊँ। परंतु समय ने हमें जकड़ रखा था, और बाबा विश्वनाथ का बुलावा अभी तक नहीं आया था।
काशी की धरा पर कदम रखना सिर्फ यात्रा नहीं होता, वह आत्मा की पुनर्प्राप्ति होती है। यह शहर हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति देता है, हमारे अस्तित्व की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करता है। और शायद यही कारण था कि जब तक बाबा विश्वनाथ स्वयं नहीं बुलाते, कोई यहाँ आ नहीं सकता। मेरी यात्रा रुकी हुई थी, लेकिन बनारस मेरे भीतर निरंतर प्रवाहित था।
शायद एक दिन, जब बुलावा आएगा, मैं फिर से उन गलियों में लौटूँगा, गंगा की ठंडी हवाओं को महसूस करूँगा, और बनारस की गोद में फिर से खो जाऊँगा। क्योंकि बनारस केवल एक शहर नहीं, बल्कि आत्मा की वह पुकार है, जो हर जन्म में हमें वापस बुलाती रहती है।
समय की बहती धारा मुझे बनारस से बहा ले गई- बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, दिल्ली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेलीष्ठ ये शहर आते गए, जीवन की किताब के पन्नों में जुड़ते गए। चौबीस वर्षों की इस लंबी यात्रा में न जाने कितने मोड़ आए, कितने संगी-साथी छूटे, कितने नए लोग जुड़े। कुछ रिश्ते समय के साथ और गहरे होते गए, तो कुछ यादों में बदलकर एक कोने में सिमट गए।
इन वर्षों में जीवन ने मुझे बहुत कुछ दिया- नई भूमिकाएँ, नए अनुभव, और सबसे बढ़कर मेरी अपनी छोटी-सी दुनिया- मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे। उन्होंने मेरे जीवन में एक नई रोशनी भरी, जिसमें संभावनाओं के असंख्य द्वार थे, प्रेम था, आशाएँ थीं। लेकिन, इस सफर में कुछ ऐसा भी था जो सदा के लिए मुझसे दूर हो गया- पापा, अम्मा, बड़ी अम्मा, बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, और दोनों छोटी भाभियाँ। वे अब भौतिक रूप में मेरे साथ नहीं थे, लेकिन स्मृतियों के कोमल आँगन में वे आज भी जीवंत हैं।
अब बस यादें ही मेरी संगिनी हैं- कभी मद्धम मुस्कान बिखेरती, तो कभी आँखों को नम कर जातीं। कभी-कभी तो लगता है, स्मृतियाँ ही वह धरोहर हैं, जो समय के थपेड़ों से अडिग रहती हैं। बनारस की तंग गलियाँ, घाटों पर टहलते लोग, सुबह की आरती में उठती घंटियों की ध्वनि- ये सब कहीं न कहीं मेरे भीतर ही जीवित हैं। लेकिन फिर भी, जीवन की व्यस्तताओं और उत्तरदायित्वों की परिधि में घूमते हुए, कभी लौटकर बनारस जाना प्राथमिकताओं में नहीं आ पाया।
परंतु बनारस तो बनारस है! वह किसी शहर भर का नाम नहीं, वह एक भावना है, एक प्रतीक्षा है। वह जानता था कि मैं लौटूँगा, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं, उसकी शर्तों पर। बनारस की मस्ती मुझे पुकारती, उसकी अल्हड़ता और उसकी सादगी मुझे बाँहों में भर लेना चाहती, पर बाबा विश्वनाथ का बुलावा अभी नहीं आया था। और जब तक वह बुलावा नहीं आता, तब तक लौटने की राह भी अधूरी ही रहती।
शायद यह वही अटूट संबंध है जो काशी का अपने हर संतान से होता है। वह बुलाएगा भी, लेकिन तब, जब वह चाहेगा। और मैं, उसकी प्रतीक्षा में, बनारस को अपने भीतर ही जीता रहा हूँ।
चौबीस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बनारस लौटने का विचार मन में एक अजीब-सा रोमांच और उत्साह भर लाया। यह विचार न केवल एक यात्रा का संकेत था, बल्कि स्मृतियों की पुनरावृत्ति का निमंत्रण भी था। ऐसा नहीं था कि इन वर्षों में मैं पूर्वांचल की धरती पर कभी नहीं गया; जौनपुर के समारोहों में शामिल हुआ, वहाँ के घर-आंगन की धूल को अपने चरणों में समेटा, परंतु बनारस हमेशा एक अधूरी प्रतीक्षा की तरह रहा। उसकी गलियाँ, उसकी हवा, उसकी गंगा- सब जैसे मेरी प्रतीक्षा में रुकी थीं, और मैं, जीवन की आपाधापी में उलझा, कभी लौट नहीं सका।
परंतु २०२४ का अगस्त कोई साधारण माह नहीं था। इस बार निर्णय लिया नहीं गया, बल्कि स्वयं बनारस ने मुझे बुलाया था। एक अनकही पुकार, जो हृदय के किसी कोने में वर्षों से सोई थी, अब जाग उठी थी। और जैसे ही यह विचार जन्मा, यात्रा का संकल्प स्वयं आकार लेने लगा। यह यात्रा मात्र भौगोलिक नहीं थी; यह आत्मा की यात्रा थी, स्मृतियों के घाट पर एक बार फिर से डुबकी लगाने का अवसर।
यात्रा की योजना भी सहज नहीं बनी। पहले विचार था कि ट्रेन से जाया जाए, परंतु फिर लगा कि कार से जाना अधिक उपयुक्त होगा- अपनी गति, अपनी दिशा, और अपने समय के साथ। जैसे जीवन का हर निर्णय एक प्रवाह में आकार लेता है, वैसे ही यह निर्णय भी बिना किसी विशेष प्रयत्न के लिया गया।
पहले बनारस की गलियों में भटकना था- उन संकरी गलियों में, जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ हर मोड़ पर एक स्मृति सांस लेती है। फिर जौनपुर की हवाओं में एक बार फिर साँस लेने का मन था- उस भूमि पर जहाँ कदमों ने बचपन में दौड़ लगाई थी, जहाँ रिश्तों की मिठास आज भी हवा में घुली होगी।
यात्रा का समापन केवल स्मृतियों में नहीं होना था; यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी था। अयोध्या की ओर रुख करने का विचार आया- राजा राम की जन्मभूमि, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर नैमिषारण्य का तीर्थ, जहाँ ललिता माता के दर्शन की लालसा थी, जहाँ सृष्टि का पहला यज्ञ हुआ था, जहाँ ऋषियों की गूँज आज भी वायुमंडल में बसी है। और अंततः, नाथ नगरी बरेली की ओर वापसी, जहाँ जीवन की वर्तमान धारा फिर से गति पकड़ेगी।
यह केवल एक यात्रा नहीं थी; यह आत्मा का संधान था। स्मृतियों से वर्तमान तक की यह यात्रा एक सेतु थी, जो मुझे मेरे ही अतीत से जोड़ने वाली थी। बनारस बुला रहा था, और इस बार मैं रुकने के लिए नहीं, लौटने के लिए आ रहा था।
सफ़र एक सुहानी सुबह शुरू हुआ, जब सूरज की पहली किरणें सड़कों पर सुनहरे छींटे बिखेर रही थीं। कार की खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके बीते दिनों की किताब के धूल भरे पन्नों को पलट रहे थे। जैसे-जैसे बनारस नज़दीक आता गया, मन के किसी कोने में दबे पड़े स्मृतियों के बीज फिर से अंकुरित होने लगे। गंगा किनारे की अलसाई दोपहरें, संकरी गलियों की भीड़-भाड़, मंदिरों से गूंजते शंख और घंटियों की ध्वनि- सब कुछ जैसे समय की धारा से निकलकर फिर से मेरे सामने खड़ा हो गया था।
कई वर्षों से सुनता आया था कि बनारस अब पहले जैसा नहीं रहा। समय ने उसे आधुनिकता के नाम पर नया रूप दे दिया है। लेकिन मैं इसे सुनकर भी अनसुना कर देता था, क्योंकि मेरे मन में जो बनारस था, वह कभी बदल नहीं सकता था। परंतु आज, वर्षों बाद, यह बनारस स्वयं मेरे सामने खड़ा था, और मैं इसके बदलते स्वरूप से रू-ब-रू होने जा रहा था।
जैसे ही हम जौनपुर बाईपास से बनारस की ओर मुड़े, मेरा हृदय विस्मय से भर उठा। जहाँ कभी धूल भरी संकरी गलियाँ थीं, वहाँ अब चौड़ी, चमचमाती सड़कें थीं। ऊँचे-ऊँचे फ्लाईओवर उन गलियों को ढँक रहे थे, जिनमें मैंने अपना बचपन जिया था। अर्दली बाज़ार, कचहरी का गोल चक्कर जिसके बीचों-बीच एक बरगद का बड़ा ही विशालकाय पेड़ हुआ करता था, वरुणा पुल- सब कुछ नया था, और इस नयापन ने मुझे कहीं भीतर तक झकझोर दिया था। मेरा बनारस, जो मस्ती और अल्हड़ता का दूसरा नाम था, अब एक अनुशासित शहर बन चुका था।
पांडेपुर का रास्ता, भोजूबीर का तिराहा- जहाँ कभी सब्जीमंडी लगा करती थी, ठेले लगे होते थे, जहाँ जीवन अपनी सहजता में बहता था, वह अब बदल चुका था। बचपन की वे सड़के, जिन पर नंगे पाँव दौड़ा था, वे अब डामर और कंक्रीट की परतों से ढँक चुकी थीं। एक क्षण के लिए मुझे लगा जैसे मेरी यादें और यह नया बनारस एक-दूसरे के विपरीत दिशाओं में खड़े थे।
हवा में गंगा की वही ठंडक थी, लेकिन उसमें अब कुछ बदला-बदला सा महसूस हो रहा था। शायद यह परिवर्तन बनारस का नहीं, मेरा था। समय ने केवल शहर को नहीं बदला था, उसने मुझे भी ढाल दिया था। लेकिन फिर भी, बनारस की आत्मा तो वहीं थी- व्िाश्वनाथ की नगरी, जहाँ हर आहट में भक्ति की ध्वनि है, जहाँ हर साँस में गंगा की लहरों की नमी घुली है। यह वही बनारस था, लेकिन एक नए आवरण में।
मैं जानता था, चाहे बनारस की सड़कों पर कितने ही बदलाव आ जाएं, इसके घाटों पर समय कभी ठहरता है, कभी बहता है, लेकिन इसकी आत्मा कभी नहीं बदलती।
जैसे ही शहर के बाहरी हिस्सों से होते हुए अर्दली बाज़ार की ओर बढ़ा, एक विचित्र अनुभूति मन में जागी। अब रास्ते वैसा नहीं लग रहे थे जैसा स्मृति में बसे थे। पहचान के चिह्न कहीं धुंधले हो गए थे, तो कहीं वे आधुनिकता के नए रंग में रंग चुके थे। तभी गूगल मैप की याद आई। जीवन भर बनारस की गलियों में घूमता रहा था, लेकिन आज उसी शहर को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेनी पड़ रही थी- यह एक अजीब सा क्षण था। समय ने न केवल शहर को बदला था, बल्कि मेरे और इसके संबंधों को भी एक नया मोड़ दे दिया था।
फोन निकाला, गंतव्य सेट किया, और फिर सड़क से ज्यादा, स्क्रीन पर टिमटिमाते नीले मार्ग पर ध्यान देने लगा। गली-मोहल्लों से ज्यादा अब गूगल की निर्देशित आवाज़ पर विश्वास किया जा रहा था। यह स्थिति थोड़ी असहज था- क्या सच में मैं अपने ही शहर में किसी और की राहनुमाई में चल रहा था? परंतु यही समय का सच था। रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए, मेरे भीतर स्मृतियों और वर्तमान का द्वंद्व चलता रहा। अंततः, महावीर मंदिर के पास, बड़े भाई साहब के घर पहुँचकर यह यात्रा का पहला पड़ाव पूरा हुआ।
रात जैसे संचित स्मृतियों का उत्सव बन गई थी। हँसी-ठहाकों के बीच, पुरानी बातों की गठरी खुलती रही। कभी बीते दिनों के प्रसंगों पर हँसी गूंजती, तो कभी कोई चुप्पी उन यादों की गहराई को और गाढ़ा कर देती। किसे पता था कि वे बीते पल, जो कभी साधारण हुआ करते थे, आज इतने मूल्यवान लगेंगे?
कब आँख लगी, यह पता भी न चला। शायद नींद भी उन यादों की गहरी नदी में बहकर आई थी। सुबह होते ही, मन में वही पुरानी प्यास जाग उठा- सुबह-ए-बनारस का अनुभव करने की। बनारस की सुबह केवल सूर्योदय का दृश्य नहीं होती, वह समय का एक जीवंत एहसास होती है, जहाँ हर कण में भक्ति की ध्वनि है, जहाँ हवा में गंगा की शीतलता है, और जहाँ मंदिरों की घंटियों में आत्मा की शांति बसी होती है। हल्का नाश्ता किया और फिर निकल पड़ा उस बनारस को देखने, जिसे मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया था, और जो अब मुझे पुकार रहा था।
यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक पुनर्मिलन था- मेरे और मेरे बनारस के बीच, जहाँ समय की धारा में बहते हुए भी, कुछ स्थायी, कुछ अविनाशी हमेशा बना रहता है।
सुबह की ठंडी हवा बनारस की गलियों से बहकर हमारी साँसों में समा रही थी। इस नगरी की हवा में एक अद्भुत सुगंध थी- अगरबत्ती, जलते दीपों और कहीं-कहीं चढ़ते दूध की मिलीजुली गंध, जो इस शहर को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। मन में एक अजीब सा उत्साह था, और उस उत्साह ने हमें सीधे अस्सी घाट की ओर खींच लिया।
अस्सी घाट- जहाँ बनारस का दिल धड़कता है, जहाँ सुबह की पहली किरणें गंगा के जल पर नृत्य करती हैं, और जहाँ हर लहर में इतिहास का एक टुकड़ा बसा हुआ है। वहाँ पहुँचते ही मन पुराने दिनों की गलियों में घूमने लगा। याद आया कि कैसे हम पहले घंटों यहाँ बैठा करते थे, मित्रों के साथ ठहाके लगाते थे, गंगा किनारे बहसें छेड़ते थे, और दुनिया की न जाने कितनी उलझनों को हल कर डालते थे। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं था। भीड़ तो थी, पर चेहरों पर वो बेफिक्री नहीं दिख रही थी। घाट पर लोग अब भी बैठे थे, मगर बातचीत में वही पुरानी आत्मीयता नहीं थी।
गंगा का पानी इस बार बढ़ा हुआ था। लहरें उफान पर थीं, और स्नान का प्रश्न ही नहीं उठता था। परंतु गंगा के सान्निध्य का लोभ मन को रोक न सका, सोचा कि जब स्नान संभव नहीं, तो क्यों न स्टीमर की सवारी की जाए? यही विचार मन में आते ही हम स्टीमर की ओर बढ़ गए।
स्टीमर पर पाँव रखते ही, अतीत की परछाइयाँ मेरे चारों ओर घिर आईं। स्मृति के गलियारों में अब भी वे लकड़ी की पुरानी नावें थीं, जिन्हें मल्लाह भाई प्यार से खेते थे। वे नावों के साथ-साथ हमारे मन की भी पतवार थाम लेते थे। हर चप्पू के साथ वे हमें बनारस की एक नई कथा सुनाते- कभी तुलसीदास के रामचरितमानस की कोई चौपाई सुनाते, कभी कबीर की उलटबांसियों से हमें चौंकाते, तो कभी बनारस के राजा-महाराजाओं के किस्सों में हमें उलझा देते। वो आवाज़ें अब कहीं खो गई थीं। उनकी जगह मोटर स्टीमर की घर्र-घर्र थी, और गंगा के शोर में डूबे लोगों की आपसी बातचीत।
याद आया कि कैसे बचपन में जब नाव जरा सी भी डगमगाती थी, तो हाथ अनायास ही गंगा मईया की ओर जुड़ जाते थे। वो एक भय था, मगर उस भय में भी एक अद्भुत आनंद छिपा था- एक आत्मसमर्पण, एक विनम्रता, जो आज कहीं नहीं दिखती थी। अब मोटर स्टीमर मज़बूती से गंगा में तैर रहा था, ना कोई हिचकोला, ना कोई डगमगाहट। उस डगमगाहट का रोमांच नहीं था, ना ही गंगा मईया के साथ वो मौन संवाद था, जो हर नाव की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था।
आज भी यात्रा सुखद थी, पर वह आनंद कहीं खो गया था। मज़ा और आनंद में बस यही फर्क होता है- मज़ा बाहर से आता है, जबकि आनंद भीतर से। मज़ा हमें परिस्थितियों से मिलता है, लोगों के साथ मिल-बैठकर हँसने-गाने से आता है, लेकिन आनंद आत्मा की गहराई में उतरकर आता है। वह किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करता। शायद इसलिए, स्टीमर में बैठे-बैठे भी मन कहीं और भटकता रहा- पुराने दिनों की उन नावों में, उन मल्लाहों की आवाज़ों में, उन मासूम भय और श्रद्धा से भरे क्षणों में।
जब बनारस पहुँचा, तो उसकी धड़कनें दिल के भीतर तक दस्तक दे रही थीं। पहले भीड़ थी, आज भी भीड़ थी। पहले गंगा आरती की ध्वनि गूँजती थी, आज भी गूँज रही थी। मंदिरों की घंटियाँ पहले भी बजती थीं, आज भी उनकी अनवरत ध्वनि गगन में गुंजायमान थी। लेकिन जो बदला था, वह था मेरे भीतर का दृष्टिकोण। २४ सालों में शहर का चेहरा बदला था, लेकिन उसकी आत्मा वही थी।
यह शहर केवल मंदिरों और घाटों का समूह नहीं, यह एक जीवंत दार्शनिक संवाद है। यहाँ हर पत्थर बोलता है, हर गली एक कथा सुनाती है, और हर लहर में समय का प्रवाह प्रतिबिंबित होता है। मैं लौट तो आया था, लेकिन बनारस मुझमें अब भी बसा हुआ था- शायद हमेशा के लिए, समय के उस अनंत प्रवाह में, जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, सिवाय स्मृतियों के।
अस्सी घाट से अभी हम निकले ही थे कि एक टुकटुक वाला दिख गया। दुबला-पतला सा, लेकिन चेहरे पर एक अपनापन झलक रहा था। हमने बनारसी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, `चलबा गुरु?'
वो तुरंत हंसकर बोला, `काहे ना चलब? चलल खातीर ही त इहाँ खड़ा हइ!'
उसकी सहजता में कुछ ऐसा था कि मन खुश हो गया। हम सब झटपट उसकी टुकटुक में बैठ गए। जगह थोड़ी कम थी, सो मैं उसके बगल में, ड्राइवर सीट पर ही टिक गया। तय हुआ कि सबसे पहले `दुर्गा कुंड मंदिर' चलेंगे।
जैसे ही उसने अपनी बैटरी वाली टुकटुक को घुमाया, ऐसा लगा मानो अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। मैं हल्के मज़ाक में बोल पड़ा वही की भाषा में -
`बहुत ताकत लगावे के पड़त हव का?'
वो हंसते हुए बोला, `अरे भइया, गाड़ी जब खड़ी रहेला तबे ज़्यादा जोर लगावे के पड़ेला, चलत रहल त आपन आपे आसान हो जाला'
इस एक बात में जीवन का कितना बड़ा सच छुपा था! सच ही तो है, जब तक कोई चीज़ ठहरी रहती है, उसे हिलाने में ही सबसे ज्यादा ताकत लगती है। मगर एक बार चल पड़े, तो सफर खुद आसान हो जाता है।
इतने में उसकी नजर मेरे पैर पर पड़ी। अचानक उसने जल्दी से कहा,
‘भईया, जरा अपना पैरवा बचावा, अंदर कर ला'
मैं थोड़ा चौंका, मगर तुरंत पैर अंदर कर लिया। उसकी इस फिकर ने दिल को छू लिया। फिर वो हल्के से मुस्कुराया और बोला-
`भइया, जब ले तू लोग हमार गाड़ी में बाड़ा, तब ले सब आपन परिवार हउवा। ई - परिवार के सुरक्छा करल, देखभाल करल हमार धरम बाटे!'
उसकी इस बात में जितनी सादगी थी, उतनी ही गहराई भी। एक अनजान इंसान, जिसकी खुद की हालत कुछ खास नहीं थी, फिर भी हमारे लिए इतनी चिंता! उस पल एहसास हुआ कि अपनापन कोई बड़ा शब्द नहीं, बल्कि दिल का एहसास होता है। बनारस की तंग गलियों से गुजरते हुए वो छोटी-सी टुकटुक और उसमें बैठा वो आदमी, मानो जिंदगी का एक बड़ा सबक दे गया- रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं।
उस टुकटुक वाले की अपनत्व और आत्मीयता ने जैसे मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया था। अंदर तक उसकी सादगी महसूस कर रहा था, और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं खुद को रोक भी नहीं सका और पूछ बैठा, `का नाम हवे तोहार?’ क्या नाम है तुम्हारा?'
बिना मेरी तरफ देखे उसने सहजता से कहा, ‘अमरनाथ।'
लेकिन मेरे अंदर कहीं एक बेवजह की जिज्ञासा थी, जो मुझे खींचे जा रही थी। मैंने फिर से जानबूझकर पूछा, `आगे बतावा ?'
वो थोड़ा ठहरकर बोला, `बस अमरनाथ।'
उसके इस सीधे, थोड़े रूखे जवाब ने मुझे झटका दिया। कुछ असहज महसूस किया मैंने, तो फिर पूछ लिया, `अरे, कउन जाति का बाड़ा? ई बतावा मरदवा?'
उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जब उसने कहा, `जात-पात से का होई साहब? आदमी त हई ना! बाकि हां, हरिजन ही बानी साहब...'
उसके इस जवाब ने मेरे अंदर एक गहरी चुप्पी भर दी। उसकी साफगोई, उसकी सरलता ने मेरे सवाल को ही बेमानी कर दिया। कुछ पल के लिए मैं शब्दहीन हो गया, जैसे किसी ने मेरे भीतर के हर सवाल को शांत कर दिया हो। उस पल महसूस हुआ कि जाति पूछने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों मैंने उस आत्मीय इंसान से ऐसा सवाल किया, जिसका कोई मायने ही नहीं था?
उसकी आँखों में न शिकायत थी, न नाराजगी, बस एक सीधी सच्चाई थी। और मैंने उस सच्चाई के आगे खुद को बहुत छोटा महसूस किया।
मैंने फिर से बात का सिलसिला आगे बढ़ाया और पूछा -
`अच्छा, कहाँ रहेला हो ?'
वो बोला, `साहेब, एही बगले में मुगलसराय में रही ला....
मैंने फिर जानने की इच्छा से कहा, -
`अरे, मुगलसराय! उहवाँ से सबेरे रोजे आवल करेला? अरु सांझी के कब जाला तू? काहे से कि बनारस से मुगलसराय के दूरी त करीब बीस किलोमीटर होईबे करि।'
वो मुस्कुराते हुए बोला, `साहब, सबेरे नौ बजे तक आ जाइला अरु साँझ सात बजे तक रोजे चल जाइला। आज त तोहरा सब लोगन के घुमइले के बादे जाइब। अगर आप लोग महाराज कहब त सभे मंदिरवा घुमा देइब?'
(`साहब, सुबह ९ बजे तक आता हूँ और शाम ७ बजे तक चला जाता हूँ। आज्ा आप सबको घुमा कर ही जाऊंगा। अगर आप चाहें तो सभी मंदिर घुमा दूँ?')
मैंने उसकी ईमानदारी को महसूस करते हुए कहा, `हाँ, क्यों नहीं... तुम अच्छे आदमी हो, तुम ही घुमा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा।'
ये सुनकर अमरनाथ के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। अब उसे कोई और सवारी नहीं खोजनी थी, और वो पहले से भी ज्यादा आराम से हमें बनारस के मंदिरों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताने लगा। उसकी बातों में बनारस की संस्कृति और उसकी अपनी सादगी झलक रही थी।
अमरनाथ ने हमारी पत्नी से कहा, `अगर रउरा के साड़ी लेबे के होखे त बातवा, बहुते बढ़िया साड़ी के कारखाना बा इहवें बगलिया में, घुमा देब, पक्का आप लोगन के साड़ी पसंद आई और आप लोग सड़िया खरीदके जरुरे लेके जईबा' (`अगर आपको साड़ी लेनी हो तो बताइए। बहुत अच्छे साड़ियों का कारखाना है बगल में। मैं घुमा दूंगा, पक्का आप लोग जरूर साड़ी ले लेंगे।')
मैंने हंसते हुए कहा, `नहीं, साड़ी की जरूरत नहीं है।' ये सुनकर वो चुप हो गया।
मैंने फिर पूछा, `अमरनाथ भाई, और बताओ, घर पर कौन-कौन है?'
उसके चेहरे की हल्की मुस्कान अचानक गायब हो गई। मायूसी से भरी आवाज़ में बोला, `भइया, घरवा प अब केहू ना बा...' (`भैया, घर पर अब कोई नहीं हैष्ठ')
उसके इस जवाब ने जैसे मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। वो शब्द मेरे भीतर तक गूंज उठे। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। ऐसा नहीं लगा कि इस आदमी का कोई नहीं हो सकता। इतना सच्चा, इतना सरल इंसान, जो अपनी बातों में इतनी साफगोई और ईमानदारी रखता हो, उसका इस दुनिया में कोई न हो- ये सोच पाना मुश्किल था। उसकी आँखों में छिपे अकेलेपन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया।
मैंने फिर उससे पूछा, `यार अमरनाथ, तुम्हें तो रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा, खाना बनाना होता होगा। कितने बजे उठते हो? और शाम को जब वापस जाते हो तो ८-८:३० बज ही जाता होगा। फिर घर जाकर खाना बनाना और खाना, रात काफी हो जाती होगी, है ना?'
वो धीरे-धीरे मुस्कुराता हुआ बोला,
`भइया, हम त बस रातिए खाना बनाइलीं, आउर कुछ ना। सबेरे त यइसहीं पानी पीके चल आइल जाई। के बनई सबेरे-सबेरे खाना? पहिलें बनाव, फेर खाव, फेर बरतन माँज- ई सभ त रातिए कर लेईला। सबेरे बस उठीलीं, नहाइलीं, भगवान के आगे हाथ जोड़लीं आ निकल पड़लीं, भइया...' (`भैया, मैं तो बस रात का खाना ही बनाता हूँ, और कुछ नहीं। सुबह तो ऐसे ही पानी पीकर चला आता हूँ। कौन सुबह-सुबह खाना बनाए? खाना बनाओ, फिर खाओ, फिर बर्तन साफ करो, ये सब तो रात में ही करता हूँ। सुबह बस उठकर नहाता हूँ, भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ और निकल पड़ता हूँ, भैया...')
फिर वो हल्की हंसी के साथ बोला,
`जब साँझे लवटीला, त हमरा घर के आगु खटिया बिछल मिलेला। ओही प हमार यार लोग रोज बइठल इंतजार करत रहेला। रात में फेरू घर गइल के खाना बनाइलीं, नहाइलीं, आ फेर लगेला चिलम। सभे यार लोग मिलके चिलम सुलगावेला, गप्प-सप्प होखेला। ओकरे बाद खाना खा के अपना-अपना भाई लोग सुति जाला, आ सबेरे भोरे फेरू जाग जाला...'
(`जब शाम को लौटता हूँ, तो मेरे घर के सामने खटिया पड़ी रहती है। उस पर मेरे दोस्त रोज़ इंतजार करते मिलते हैं। रात को फिर घर जाकर खाना बनाता हूँ, नहाता हूँ, और फिर लगती है चिलम। सब दोस्त मिलकर चिलम मारते हैं, गपशप करते हैं। उसके बाद खाना खाकर अपने भाई सो जाते हैं और सुबह तड़के फिर उठ जाते हैंष्ठ')
उसकी बातों में एक साधारण जीवन की सच्चाई झलक रही थी, जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई शिकवा। बस एक सहजता, जो उसकी हंसी और शब्दों के बीच कहीं गहरी होती चली गई।
मैंने हंसते हुए कहा, `अमरनाथ भाई, पौवा भी लगा लेते हो क्या?'
वो भी हंसते हुए बोला,
`नाहीं भइया, ई सभ ना। नशा त शराबी करेला, भइया। हम त बस...' हम त बस बाबा भोलेनाथ के प्रसाद लेइलीं... बस चिलम पीइलीं, भइया, चिलम!'
(`नहीं भैया, ये सब नहीं। नशा तो शराबी करते हैं, भैया। हम तो बस...' और फिर एक हल्की सी शरारती हंसी के साथ कहा, `हम बाबा भोलेनाथ का प्रसाद लेते हैं... बस चिलम पीते हैं, भैया, चिलम')
उसकी मासूमियत पर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, वो कितने भोलेपन से सब कुछ मुझे बता रहा था। उसकी सीधी-सादी बातें दिल को छू रही थीं, लेकिन कहीं मेरे मन में सवाल बार-बार घूम रहा था- इतना सरल, सच्चा इंसान इस दुनिया में अकेला कैसे हो सकता है? क्या सच में ईश्वर इतना निर्दयी हो सकता है?
मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और अमरनाथ को फिर से कुरेदते हुए पूछा, `ये बताओ अमरनाथ, तुम्हारी पत्नी कब तुम्हें छोड़कर गई?'
मैंने ये बात बस अंदाज़े से ही कही थी, पर मेरे मन में कहीं गहरा संदेह था। उसकी बातों और जीवन के अकेलेपन के पीछे कुछ और छिपा हुआ था, जिसे मैं जानने के लिए बेचैन हो रहा था।
अमरनाथ मेरी बात सुनकर अचानक खामोश हो गया। कुछ पल बाद धीमी आवाज़ में बोला,
`भइया, हमार पाँच गो लइका बा... आ मेहरारू त जब ई छोटुआ होखे वाला रहे, ओही बेरा हमके छोड़ के चल गइल रहली। उ दिन त बहुते दौड़-धूप कईनी, भइया। भगवानो जइसे उ दिन झूम के बरसत रहस, आ मेहरारू दर्द से कराहत रहली। हम ओके ठेला प लाद के इधर-उधर दौड़त रहीं। पानी एतना जोर से बरसत रहे कि कुछुओ नइखि सूझत रहले।'
(`भैया, हमारे पाँच बच्चे हैं... और पत्नी तो जब सबसे छोटा वाला होने वाला था, तभी हमें छोड़कर चली गई थी। उस दिन बहुत भागा था, भैया। भगवान भी जैसे उस दिन बरस ही रहे थे, और पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। मैं उसे ठेले पर लादकर इधर-उधर भाग रहा था। बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ सूझ नहीं रहा था।')
उसकी आवाज़ भारी हो चली थी,
`उ दिन हम कल्लू सेठ से बारह सौ रुपइया उधार लिहनी, आपन रिक्शा गिरवी रख के। डाक्टर बाबू बबुआ के त बचा लिहलें, बाकिर मेहरारू ओहीं... हमेसा खातिर साथ छोड़ के चल गइल।'
(`उस दिन मैंने कल्लू सेठ से १२०० रुपये उधार लिए थे, अपना रिक्शा गिरवी रखकर। डॉक्टर ने बच्चे को तो बचा लिया, पर मेरी पत्नी वहीं... हमेशा के लिए साथ छोड़ गई।')
उसकी इस बात ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैंने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक गहरा दर्द था, जिसे वो शब्दों में बयां कर रहा था। मेरे मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। धीरे से कहा, `ओह, बहुत बुरा हुआ...'
वो हल्की मुस्कान के साथ बोला,
`भइया, स्वर्ग-नरक सभ यहीं बा। जे का भोगे के बा, सभ एही दुनियावा में भोगे के पड़ेला।'
(`भैया, स्वर्ग और नरक सब यहीं हैं। जो भी भोगना है, सब इसी दुनिया में भोगना होता है।')
उसके इन शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। जीवन की कड़वी हकीकत को उसने कितनी सादगी से स्वीकार कर लिया था, जैसे उसका दर्द अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो, और उसने उसे जीने का तरीका भी ढूंढ़ लिया हो।
मैंने अपने आपको समेटते हुए हल्के से पूछा, `तो फिर सारे बच्चों को तुमने ही पाला-पोसा होगा... ये बताओ, क्या तुमने उन्हें पढ़ाया भी? और ये पाँचों बच्चे आजकल कहाँ हैं?'
अमरनाथ ने धीरे से अपनी नज़रें सड़क की ओर फेर लीं, जैसे मेरे सवालों से बचना चाह रहा हो। उसने कुछ क्षण चुप रहकर, मेरे सवालों को अनदेखा करते हुए कहा,
`देखीं भइया, जे उल्टे हाथे देखत बानी ना, ईहे बा साड़ी के बड़ कारखाना। बहुते बड़ कारोबार बा ई... एकर मालिक हाजी मियाँ हउवें। आ जानतानी, ई लोग कारोबार में बहुते इमानदार होलें।'
`देखिए भैया, ये जो उल्टे हाथ पर देख रहे हैं न, यही है साड़ियों का बड़ा कारखाना। बहुत बड़ा कारोबार है ये... इसका मालिक हाजी मियाँ हैं। और जानते हो, ये लोग व्यापार में बहुत ईमानदार होते हैं।'
उसके लहजे में कुछ ऐसा था जैसे वह हाजी मियाँ को अच्छी तरह जानता हो। मैंने उसकी ओर मुखातिब होते हुए पूछा, `तो तुमको क्या मिलता है जब तुम पर्यटकों को यहाँ लाते हो?'
वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला,
`हाँ भइया... एही से त कहत रहीं कि रउरा लोग के साड़ी देखा देई। अगर देखत त जरूर खरिदत। हर साड़ी पर हमके पच्चीस से पचपन रुपइया ले मिल जाला।'
(`हाँ भैया... इसी लिए तो कह रहा था कि आपको साड़ियाँ दिखा देता। अगर आप लोग देखते तो ज़रूर खरीदते। हर साड़ी पर मुझे २५ से ५५ रुपए तक मिल जाते हैं।')
मैंने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, `तो एक दिन में कितने पर्यटकों को लाते हो?'
वह आत्मविश्वास के साथ बोला,
`भइया, कम से कम आठ-दस गो साड़ी त रोज बिकवा देइलीं। आ हाजी मियाँ कबहूँ भूललें नइखन। चाहें हफ्ता भर बाद जाईं कि महीना भर बाद, रुपइया पूरा मिलेला। भइया, ई लोग सचहीं कारोबार में बहुते इमानदार होलें, हर बात याद राखेलन।'
(`भैया, कम से कम ८-१० साड़ियाँ तो रोज़ बिकवा ही देता हूँ। और हाजी मियाँ कभी भूलते नहीं। चाहे हफ्ते भर बाद जाऊँ या महीने भर बाद, पैसा पूरा ही मिलता है। भैया, ये लोग व्यापार में वाकई ईमानदार होते हैं, हर बात याद रखते हैं।')
इतना कहते हुए उसने फिर से सड़क की ओर इशारा किया और कहा,
`आ देखीं, ई बा बनारस- भोले शिव के नगरी। इहाँ हर आदमी खातिर कुछ ना कुछ जरूर बा। आ जब कुछुओ ना रहेला, त मणिकर्णिका घाट बाँह पसार के गोदिया में लेल चाहेला... उहवाँ जा के बड़ा सुकून मिलेला, भइया।'
(`और ये देखिए, ये है बनारस- भोले शिव की नगरी। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और जब कुछ नहीं होता, तब मणिकर्णिका घाट बाहें फैलाए स्वागत करता है... वहाँ जाकर बड़ा सुकून मिलता है भैया।')
अमरनाथ की आवाज़ में जब उसने ये कहा, तो उसमें एक गहरी तसल्ली और ठहराव था, मानो बनारस और उसकी जीवन-दर्शन की जड़ें उसी की आत्मा में गहरे धंसी हुई हों।
मैंने फिर से उसे उसी बात पर लौटाते हुए कहा, `तुमने अब तक नहीं बताया कि बच्चे कहाँ हैं? तुमने उन्हें पढ़ाया या नहीं?'
अमरनाथ कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे शब्दों का बोझ उठाने को तैयार न हो। उसकी चुप्पी भारी थी, और ऐसा लगा मानो वह अपने टुकटुक के हॉर्न को बजाकर उस चुप्पी को तोड़ना चाहता हो। पर हॉर्न बजा नहीं- शायद टुकटुक पुराना था, इसी वजह से। अचानक, उसने अपना गुस्सा एक साइकिल वाले पर उतारा और चिल्लाकर बोला,
`अरे बगल हट जा... मरबा का हो!'
मैं समझ गया कि अमरनाथ इस सवाल पर बात नहीं करना चाहता। मगर मेरे बार-बार पूछने पर वह आखिरकार मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी, गला भर्राया हुआ था। जैसे दिल की एक गहरी परत खुल रही हो। उसने धीरे से कहा,
`साहब, हमार तीन गो बिटिया बा आ दू गो लइका। एही काम से तीनों बिटियन के बियाह कइनी। सभे आपन-आपन जिनगी में मजे में बा, बहुते खुश बा। सभे के पढ़वनी हई, साहब। तीनों बिटिया बीए कइले बा आ लइका के एमएयो करा देहनी।'
(`साहब, मेरी तीन बेटियाँ हैं और दो बेटे। मैंने इसी काम से तीनों बेटियों की शादी कर दी है। सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में मजे में हैं, बहुत खुश हैं। मैंने सभी को पढ़ाया है, साहब। तीनों बेटियाँ बीए कर चुकी हैं, और बेटे को एमए भी कराया है।')
उसकी आँखों में अजीब सी चमक था- गर्व और पीड़ा की मिली-जुली भावनाएँ। फिर उसने अपने जीवन के संघर्ष को बयां करते हुए कहा, `अभी तो मैं टुकटुक चला रहा हूँ, साहब। पिछले २८ साल से इन सड़कों को रिक्शे से नापा है।'
यह कहते-कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी, मानो दिल का कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। उसकी आँखों में आँसू झलकने लगे, जैसे वह अपनी ज़िंदगी के बोझ से थक गया हो, लेकिन फिर भी उस बोझ को ढोता जा रहा हो।
`साहब, बिटिया लोग त आवेले, जबे उ लोग के फुरसत रहेला, अपना बूढ़ बाप के देखे। आखिर कन्यादान कइले बानी, उ लोग के कवनो दोस नइखे।'
(‘साहब, बेटियाँ तो आती हैं, जब भी उनके पास वक़्त होता है, बूढ़े बाप को देखने। आखिर, उन्हें कन्यादान कर दिया गया है, उनका कोई दोष नहीं’)
मैंने हामी भरी, ‘बिलकुल सही कहते हो अमरनाथ, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं।' फिर पूछा, `अमरनाथ, और तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं?'
अमरनाथ की आँखों में अचानक एक कठोरता उभर आई। भारी मन से बोला,
‘बड़का लइका के पढ़वनी, लिखवनी, नौकरीयो लगवा देहनी। ननिहाल के संपत्ति मिलल आउर साहब, ऊ हमके छोड़ के चल गइल। कहेला, `रउरा हमार खातिर का कईनी?' अब ऊ आपन मेहरारू-बच्चा के साथे ओही रहेला, आउर साहब, अब ओकरा से कवनो वास्ता नइखे।'
(`बड़े वाले को पढ़ाया, लिखाया, नौकरी लगवा दी। उसे ननिहाल की संपत्ति मिली और साहब, वो हमें छोड़कर चला गया। कहता है, `आपने किया ही क्या है मेरे लिए?' अब वो अपने बीवी-बच्चों के साथ वहीं रहता है, और साहब, उससे अब कोई वास्ता नहीं।')
`और छोटा बेटा?' मैंने सवाल किया।
अमरनाथ की आवाज़ और भारी हो गई-
`साहब, ई छोटका के त अउरियो ज्यादा लाड़-प्यार से पाललीं। ओकरा माय के ना रहले के दुखो भुलावे के कोसिस कइनी, बाकिर ऊ त पूरा खानदान के नाक कटा दिहलस।'
(‘साहब, उस छोटे वाले को तो ज़्यादा ही लाड़-प्यार से पाला था। उसकी माँ के न होने का भी दर्द भुलाने की कोशिश की, पर उसने पूरे खानदान की नाक कटवा दी।')
‘क्या किया उसने?’
अमरनाथ की आँखों में क्रोध और बेबसी का संगम था। बोला,
`साहब, ऊ आपन से दस बरिस बड़ मेहरारू से दिल लगा लिहलस। लाख समझवनी, बाकिर इश्किया नशा में डूबल रहल। एगो दिन आके कहे लगल, `बियाह करब ओकरे से।' साहब, जइसे हमार दुनिया ही उजड़ गइल। बहुते बुझवनी, समाज के डर देखवनी, आपन इज्जत के दुहाई दिहनी, बाकिर साहब, ऊ माने के तइयारे ना रहल।
आखिर में, हम सख्त फैसला ले लीं- कह दिहनी, `अगर ओकरे से बियाह करब, त ई घर से आ हमसे कवनो नाता ना रही।' साहब, ऊ चल गइल, आ फेरु कबहूँ लवट के ना आइल। हम चुपके से ओकर खबर राखीला, बाकिर ऊ कबहूँ पलट के ना देखलस।'
(`साहब, उसने अपने से दस साल बड़ी औरत से दिल लगा लिया। लाख मना किया, मगर इश्क़ के नशे में डूबा था। एक दिन आकर बोला, `शादी करनी है उसी से।' साहब, मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। मैंने बहुत समझाया, समाज का डर दिखाया, अपनी इज़्ज़त की दुहाई दी, पर साहब, वो नहीं माना।'
आखिरकार, मैंने सख्त निर्णय लिया- ‘मैंने कह दिया, `अगर उससे शादी करनी है, तो इस घर और मुझसे कोई नाता नहीं रहेगा।' साहब, वो चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। मैं चुपके से उसकी ख़बर रखता हूँ, पर उसने कभी पलटकर नहीं देखा।')
मैंने धीरे से कहा, `अमरनाथ, तुम ही मान जाते। अगर उसे कोई परेशानी नहीं थी, तो तुम्हें क्या?' अमरनाथ ने गहरी सांस ली-
`साहब, भले जिंदगी में रिक्शा चलइलीं, बाकिर कबहूँ बेइमानी नइखीं कईली। हमरो समाज में इज्जत बा। हम वसीयत करवा दिहनी कि हमार जायदाद में ई दुनो लइकन के कवनो हक नइखी। हम मरला के बीस साल बाद ले, हमार कवनो संपत्ति प इनकर और इनकर लइकन के कवनो अधिकार ना रही। ई जे घर बा, ई हम जइसन कवनो बेसहारा आ गरीब आदमी के दे दिहल जावे। शायद कवनो पाप कईले रहीं, जे आज ई सब भोगत बानी, बाकिर बाबा विश्वनाथ त इहाँ बाड़ें।
साहब, मंदिर आ गइल। रउरा लोग दर्शन कर लीं आ बाहर आके खिचड़ी प्रसाद ले लिहीं। हम पहिलेयो कहिले रही, बनारस में बाबा कवनो के भूखा ना छोड़ेले। इहाँ फकीर, औघड़, बाबा- सबके खाना मिलेला। रउरा लोग दर्शन कई के आइ, तब तक हमहूँ आपन पेट पूजा कर लीं।' (`साहब, मैंने भले ही ज़िंदगी में रिक्शा चलाया हो, लेकिन कभी बेईमानी नहीं की। मेरी भी समाज में इज़्ज़त है। मैंने वसीयत करवा दी है कि मेरी जायदाद में इन दोनों लड़कों का कोई हक़ नहीं होगा। मेरे मरने के बीस साल बाद भी, मेरी किसी संपत्ति में इनका या इनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये जो घर है, इसे मेरे जैसे किसी बेसहारा और गरीब इंसान को दे दिया जाए। शायद मैंने कोई पाप किया होगा जो आज ये सब भ्ाोग रहा हूँ, पर बाबा विश्वनाथ तो हैं यहाँ।'
साहब, मंदिर आ गया। आप लोग दर्शन कर लो और बाहर आकर खिचड़ी प्रसाद ले लेना। मैंने पहले भी कहा था, बाबा किसी को भूखा नहीं छोड़ते बनारस में। यहाँ फकीर, औघड़, बाबा- सबको भोजन मिलता है। आप दर्शन करके आओ, तब तक मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ।’)
हम अंदर गए, दर्शन किए, और जब लौटे, तो अमरनाथ वहीँ खड़ा मिला। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
`चलीं साहब, रउरा के आखिरी पड़ाव ले छोड़ देब।'
(`चलो, साहब, मैं आपको अंतिम पड़ाव तक छोड़ दूँगा।' )
पूरे रास्ते वो मस्ती भरे अंदाज़ में बातें करता रहा। हम जब गाड़ी से उतरे, मैंने जितने पैसे उसने मांगे, उसे दिए और फिर ५०० का एक नोट बढ़ाया। `ये रख लो,' मैंने कहा, `जब बेटियाँ आएं तो उनके बच्चों के लिए मिठाई खिला देना।'
अमरनाथ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला
`साहब, जरूर। शायद अब रउरा से फेरु भेंट ना हो सके, काहे कि सफर में मुसाफिर अक्सर एक-दूसरा से बिछड़ जालन। बाकिर बाबा विश्वनाथ से आपन लोगन के सलामती के पार्थना जरूर करब... जय बाबा विवश्वनाथ के, भइया, जीता रहा ष्ठ. जिया राजा बनारस।'
(`साहब, ज़रूर। शायद अब आपसे दोबारा मुलाक़ात न हो सके, क्योंकि सफ़र में मुसाफ़िर अक्सर एक-दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मगर बाबा विश्वनाथ से आपकी सलामती की दुआ जरूर करूंगा... जय बाबा विश्वनाथ की , भैया जीता रहा ..... जिया राजा बनारस ।')
इतना कहकर, अमरनाथ अपनी टुकटुक में बैठा और धीरे-धीरे बनारस की गलियों में ओझल हो गया।
लेकिन उसकी बातें, उसकी सादगी, उसकी ज़िन्दगी का फलसफा मेरे मन में कहीं गहरे उतर गया- जैसे गंगा में पड़ा कोई पत्थर, जो पानी की सतह पर हलचल मचा कर अंततः गहराइयों में समा जाता है। अमरनाथ जैसे साधारण इंसान ने जीवन की हर चोट, हर दर्द को इतनी सहजता से स्वीकार किया था, मानो वही उसकी तक़दीर हो, और तक़दीर से शिकायत करने का उसे कोई हक़ ही न हो।
उसने कोई संघर्ष नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया- बस हर दुख को, हर ठोकर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानकर जीता रहा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हममें से अधिकतर लोग नसीब से लड़ते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, मगर अमरनाथ ने तक़दीर से कोई जंग नहीं लड़ी। उसने बस अपने हिस्से का दुःख जिया- बिना किसी शिकायत, बिना किसी उम्मीद, पूरी सहजता के साथ।
शायद यही जीवन का सबसे गहरा सबक था- जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना, जैसा वह आता है। न भाग्य को कोसना, न भविष्य से लड़ना- बस बहते जाना, गंगा की धार की तरह।
जब हम बरेली लौटे, तो महसूस हुआ कि २४ साल बाद बनारस की यह यात्रा महज़ एक सफर नहीं थी- यह एक आत्मिक पुनर्जन्म था। यह शहर सिर्फ मंदिरों और घाटों का नगर नहीं, यह जीवन के सत्य को गहराई से समझने की भूमि भी है। बनारस ने मुझे बदल दिया था- या शायद, मुझमें कुछ नया जगा दिया था।
आमोद कुमार श्रीवास्तव
बरेली, उत्तर प्रदेश
What's Your Reaction?
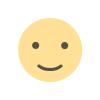 Like
4
Like
4
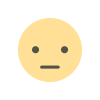 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
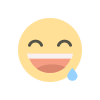 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
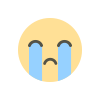 Sad
0
Sad
0
 Wow
1
Wow
1