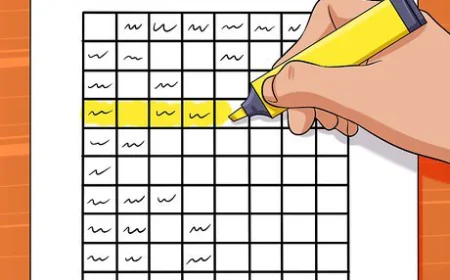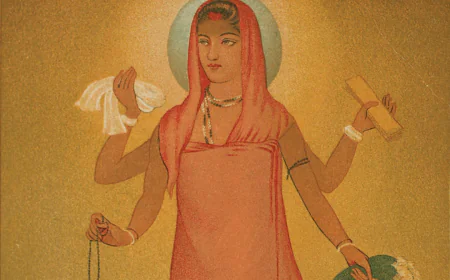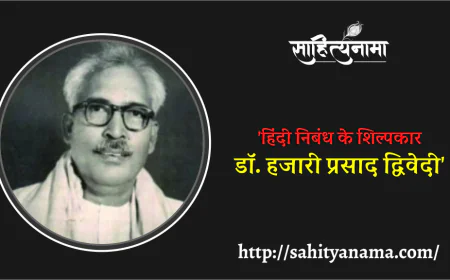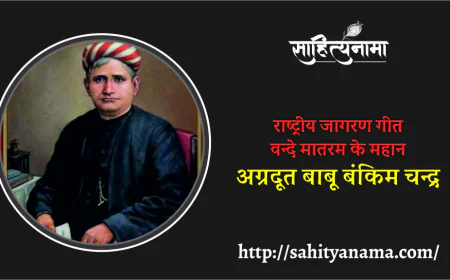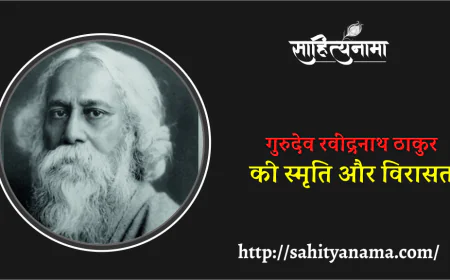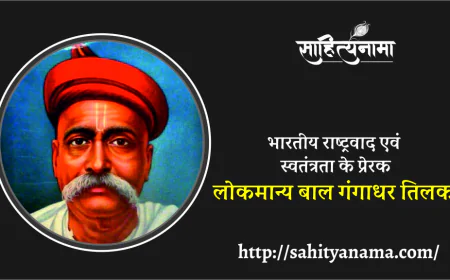शब्द-सौंदर्य
श्रीरामचरितमानस के रामविवाह प्रसंग में परशुरामजी के उग्र वचनों के उत्तर में लक्ष्मणजी कहते हैं- पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू।। (बालकांड दोहा २७३, चौपाई संख्या २) अर्थात् `मुझे बार-बार कुठार दिखाते हो। पहाड़ को फूँककर उड़ाना चाहते हो।'

श्रीरामचरितमानस के रामविवाह प्रसंग में परशुरामजी के उग्र वचनों के उत्तर में लक्ष्मणजी कहते हैं-
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू।
चहत उड़ावन फूँकि पहारू।।
(बालकांड दोहा २७३, चौपाई संख्या २)
अर्थात् `मुझे बार-बार कुठार दिखाते हो। पहाड़ को फूँककर उड़ाना चाहते हो।'
पहाड़ को फूँककर उड़ाना निश्चित ही असंभव है। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे इसके जैसा कुछ किया जा सके? चलिए, देखते हैं।
दरअसल संस्कृत शब्दकोश में पहाड़ का एक पर्यायवाची `पराग' भी बताया गया है। जैसा कि सबको मालूम है, फूलों के अंदर `पराग', बारीक चूर्ण के रूप में होता है। उन फूलों पर तितलियाँ बैठती हैं, फिर यह उनके पैरों में लगकर दूर-दूर के अन्य फूलों तक पहुँच जाता है। और तब परागण की प्रक्रिया घटित होती है। `दूर तक जाता है', इसीलिए इस पदार्थ को `पराग' कहा गया है (पराृदूर; परा गच्छतिृदूर तक जाता है)-
पराग: (परा गच्छति इति डः) पुं० पुष्परज (फूल का पराग), धूल, सुगंधित चूर्ण, पहाड़, चन्दन रज (अमरकोश २.४.१७, ३.३.२१)।
आप कहेंगे यह क्या बात हुई? पराग और पहाड़ को एक ही तरह का बता दिया गया? पराग तक ठीक है कि दूर तक जाता है। लेकिन पहाड़ तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। कहीं जाने और उसमें भी `दूर तक' जाने की बात कहाँ से आ गयी? नहीं चलने या नहीं हिलने के कारण ही तो पहाड़ को `नग' और `अग' भी कहा गया है-
नगः अगः (न गच्छति इति डः, `नगोप्राणिष्व:'
इति नञ् वा प्रकृत्या, नलोपे तु अगः)
पुं. पर्वत, वृक्ष, सूर्य, सर्प। (अमर- ३.३.१९)
ध्यान देने की बात है कि कई बार किसी से रास्ता हम इस तरह पूछते हैं- `भाई साहब, यह रास्ता शहर तक जाता है क्या?' उस हालत में रास्ता उठकर तो कहीं नहीं जाता। हाँ, वह वहाँ तक फैला हुआ होता है। तभी कहा जाता है, `हाँ, यह रास्ता शहर तक जाता है।' इसी प्रकार, पहाड़ दूर तक फैला हुआ होता है, इसलिए कहा गया कि `दूर तक जाता है।' और इस प्रकार `परा गच्छति' से हुआ `पराग', जो पहाड़ का पर्यायवाची माना गया।
अब लगभग हर पर्वत का एक शिखर भी है, जो उसका सबसे ऊँचा बिंदु होता है। इस बिंदु को इस तरह देख सकते हैं जैसे मनुष्य के शरीर पर शिखा, मस्तक के सबसे ऊपर होती है। और जैसे, पर्वत की भी एक शिखा हो (सबसे ऊपर)-
शिखरम् (शिखास्यास्ति)- अमर० २.३.४
इस प्रकार पर्वत के सबसे ऊँचे बिंदु का नाम हुआ `शिखर'।
पर्वतों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सारे पर्वतों में कई चट्टानों के बीच में जोड़ हुआ करते हैं। भूविज्ञान (ुादत्दुब्) में पर्वतों के अंदर इस तरह के बहुत-से जोड़ होने के दो-तीन कारण गिनाये जाते हैं। दूसरी ओर, जोड़ (गणित वाला नहीं) को संस्कृत में `पर्व' भी कहते हैं। (पर्व का ही तद्भव रूप `पोर' है। अगर शरीर के जोड़ों में दर्द हो तो कहा जाता है कि 'पोर-पोर में दर्द है।)-
पर्व (पर्वतीति कनिन्) नपुं. वंशादि के पोर (ग्रन्थि)-
अमर० २.४.१६२
इसलिए पहाड़ों को `पर्वत' नाम दिया गया (क्योंकि उनमें कई जोड़ होते हैं)-
पर्वतः (पर्वाणि सन्त्यत्र इति अतच्)
पुं० पहाड़- अमर० २.३.१
अब पहाड़ को फूँकने वाली बात। यह काव्यशास्त्रविनोद है कि कोई बालक अगर किसी फूल के पराग को फूँककर उड़ा दे, तो वह ऐसा सोचकर आह्लादित हो सकता है कि `हमने पहाड़ (पराग) को फूँककर उड़ा दिया'!
आशुतोष
पटना बिहार
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
1
Love
1
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0