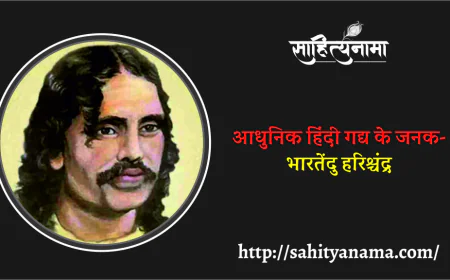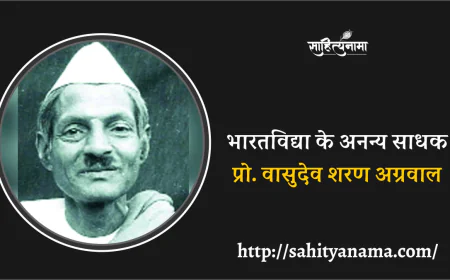साहित्य और सिनेमा
हिंदी सिनेमा कला के तादात्म्य की एक बेमिसाल कहानी है। दुनिया के किसी भी देश के सिनेमा ने इतने सालों तक लगातार करोड़ों-करोड़ों की आबादी के सौंदर्य बोध और मनोजगत को गढ़ने का काम इतनी शिद्दत से नहीं किया। सिनेमा की इस यात्रा ने विज्ञान, कला और विचार के विविध रूपों को पर्दे पर उतारा, मगर दर्शकों को जिसने सबसे जज़्यादा आकर्षित किया वो साहित्यक कृति पर बने सिनेमा ने। दूसरे शब्दों मे इसे हम साहित्यकारों का सिनेमा भी कह सकते हैं

हिंदी सिनेमा कला के तादात्म्य की एक बेमिसाल कहानी है। दुनिया के किसी भी देश के सिनेमा ने इतने सालों तक लगातार करोड़ों-करोड़ों की आबादी के सौंदर्य बोध और मनोजगत को गढ़ने का काम इतनी शिद्दत से नहीं किया। सिनेमा की इस यात्रा ने विज्ञान, कला और विचार के विविध रूपों को पर्दे पर उतारा, मगर दर्शकों को जिसने सबसे जज़्यादा आकर्षित किया वो साहित्यक कृति पर बने सिनेमा ने। दूसरे शब्दों मे इसे हम साहित्यकारों का सिनेमा भी कह सकते हैं।
जब साहित्य और सिनेमा मिलकर सामने आते हैं, तो एक मुल्क की सच्ची तस्वीर सामने आती है।
फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी `मारे गए गुलफाम' पर बनी फिल्म को भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों में शुमार किया जाता है जो ठेठ ग्रामीण परिवेश या असली भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। ध्यान से देखें तो पूरी फिल्म मे कैमरा एक शॉट के लिए भी शहर की तरफ नहीं घूमता।
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यह फिल्म जिसमे राजकपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई, जी हां, मैं बात कर रही हूं बासु भट्टाचार्य द्बारा निर्देशित तथा कवि शैलेन्द्र द्बारा निर्मित `तीसरी कसम' की। यह हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है, जिसे देखकर गांव की मिट्टी की गंध का अनुभव होता है। कहानी के पात्र, पाठकों से साकार रूप मे बोलते से प्रतीत होते हैं। इस फिल्म के संवाद और पटकथा हिंदी के यशस्वी कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने ही लिखे थे और ज़ाहिर सी बात है यह फिल्म उनकी ही कृति `मारे गए गुलफाम' पर आधारित थी।
पहले वहीदा रहमान की भूमिका के लिए नूतन का चुनाव किया गया था किंतु नूतन के पति उनको किसी गांव में शूटिंग के लिए भेजना नही चाहते थे। सो यहां बात बनी नही और फिर यह बात तो सभी जानते हैं कि हीराबाइ की अविस्मरणीय भूमिका मे वहीदा रहमान जीती-जागती मिसाल बन गईं।
यह कहानी बस दो पात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है-राज कपूर अपनी संपूर्ण भावनाओं के साथ,`हीरामन' की भूमिका के लिए पर्दे पर उतरे। और नीली आंखों वाला यह अभिनेता जब बैलगाड़ी मे मुकेश जी की आवाज़ के साथ पर्दे पर अपने होंठ हिलाकर गाना शुरू करता है - `सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है' तो जाने अंजाने बोले गए झूठ पर मन डर-डर जाता है। यहाँ दार्शनिकता से भरी बातों में इतनी सहजता है कि कुछ देर को लगता है हम कबीर का लिखा कोई दोहा रजतपट के पर्दे पर पढ़ रहे हैं। वह जिन-परी से बहुत डरता है। रात को जब उल्लू, सियार की आवाज़ आती है तो वह कहता है- `है महादेव, रक्षा करो, सवा रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा', उन्होंने अपनी छवि को `तीसरी कसम' के यथार्थ में ढाल दिया था। हिंदी सिनेमा में ही नही, समूचे विश्व सिनेमा में ऐसा बहुत ही कम घटित हुआ है कि साहित्य से प्रेरित फिल्म को उसकी सटीक साहित्यिक गहराई के साथ पर्दे पर सफलता से प्रस्तुत करा गया। साहित्य से बनी फिल्में सिनेमा को समरस बनाने मे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इस मामले मे फिल्म `साहिब, बीबी और गुलाम' जिसे विमल मित्र के उपन्यास पर गुरुदत्त ने पर्दे पर साकार किया था। यह वो फिल्म है जो अपने पूरे कथ्य के साथ पर्दे पर प्रस्तुत हुई है और सफल भी। साहित्यकारों के सिनेमा के अंतर्गत हम कैसे भूल सकते हैं आर के नारायण की `गाइड', जो फिल्म में शीर्ष सितारों के होते हुए भी गहरी दार्शनिक बातें कहने की चेष्टा की और सफलता का परचम लहराया। यह फिल्म उनमें से एक है और निस्संदेह जब भी `गाइड' की बात होगी तो हम कैसे भूल सकते हैं विजय आनंद के चुस्त निर्देशन को। संपादन और तकनीकी पक्ष का उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वाह किया। वहीदा रहमान के हवाले से होली वाला नृत्य समूचे ब्रम्हांड को रंगने वाला दृष्य एक आर्ट है और यह सिर्फ विजय आंनद के ही बूते की बात थी।
शेक्सपियर को अगर पता होता कि भविष्य मे उनके नाटकों पर इतनी ज्यादा फिल्में बनने वाली हैं और बनी फिल्मों को इतने-इतने पुरस्कार मिलने वाले हैं तो वे कितने खुश होते। `ओंकारा' को 'कान फिल्म समारोह' मे प्रदर्शित होने का अवसर मिला, तीन शेक्सपियर नाटकों को फिल्म में गूंथने वाले लारेंस ओलिवियर के `हैमलेट' को सर्वोत्तम फिल्म, सर्वोत्तम अभिनेता का अकादमी पुरस्कार मिला था। बीबीसी ने शेक्सपियर के नाटकों पर अनेक सीरीज़ बनाई है, आज शेक्सपियर अकादमिक घेरे से बाहर निकल कर आम जन तक पहुँच गए हैं। एक बार नाटककार विजय तेंदुलकर ने कहा था कि शेक्सपियर के बिना साहित्य गरीब है, ऐसे और बहुत से उदाहरण मौजूद हैं वस्तुतः किसी भी साहित्यिक कृति को संदूक और डायरी के कारावास से मुक्त करने, गोष्ठियों और पत्रिकाओं के पन्नों के बाहर लाकर जब कोई निर्देशक उसे पर्दे पर लाता है तो यह सुनिश्चित करना निर्देशक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस कृति का मूल नष्ट न होने पाए। साहित्य पढ़ने-सुनने-समझने वालों का दायरा बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी साहित्य से जुड़े लोग महसूस करें। प्रयोगधर्मी सिनेमा अस्सी-नब्बे के दशक में खूब सुना और सराहा गया मगर यह बात कम लोग ही जानते हैं कि किशोर साहू फिल्म लेखन के साथ-साथ साहित्यिक लेखन्ा भी खूब करते रहे हैं। `टेसू के फूल', `घोंसला' और `छलावा' नाम से उनके कहानी संग्रह को हिंद पॉकेट बुक ने छापा, अभिसार नाम से उनका गीत संकलन भी छपा और उस दौर मे कहानी लेखन के साथ-साथ उन्होने सिनेमा में साहित्यिक कृति पर फिल्मे बनाने का जोखिम भी उठाया। किशोर साहू का स्वप्न, `हैमलेट' पर फिल्म बनाने का यह प्रयोग अपनी मंजिल न पा सका। किशोर साहू जैसा साहस आज कितने फिल्मकारों के अंदर है, सच तो यह है साहित्यकारों का सिनेमा रचने के लिए यह जवाबदेही अकेले साहित्यकारों के कंधों पर छोड़कर हम एक अच्छे सिनेमा की उम्मीद नही कर सकते। सिनेमा अंततः मनोरंजन का माध्यम है तो यह जिम्मेदारी एक निर्देशक की भी होती है कि वह किसी भी साहित्यिक कृति पर बिना उस कृति की आत्मा को नष्ट किए एक फिल्म को कैसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो आज के निर्देशकों को गुरुदत्त और विजय आंनद का सिनेमा बतौर पाठ्यक्रम की हैसियत से देखना और समझना चाहिए, दोनो दो अलग जीवन-दृष्टि और शैलियों के फिल्मकार हैं। गुरूदत् का सिनेमा उनके अपने अर्जित अनुभवों और संघर्षों के बीच से विकसित हुआ, तभी उन्होंने विमल मित्र के उपन्यास पर `साहिब बीबी और गुलाम' बनाई जो आज आधी शताब्दी बाद भी अपने आकर्षण से चमक रही है, और आर के नारायण के उपन्यास पर विजय आनंद द्बारा निर्देशित `गाइड' जितनी बार देखो हर बार नए अहसास नई ताज़गी से मन को भर देती है।
साहित्यकारों का सिनेमा एक अलग धारा है जिसका जनमानस पर गहरा असर हुआ है। साहित्यिक कृति को पढ़ते समय एक गहरा दार्शनिक आस्वाद आप मन मे महसूस कर सकते हैं मगर वही साहित्यिक कृति जब सृजन के दौर से गुजर कर पर्दे पर आती है तो वो कला के चरम संधान की उत्कृष्ट खोज बन जाती है। सिनेमा ही एक ऐसा पटल है जहां कला की सभी नदियों का संगम होता है।
हिंदी फिल्मों में साहित्य की अनेक कालजयी कहानियां दर्ज हैं, जिनहे हम शान से हिंदी सिनेमा कह सकते हैं, जरूरत है थोड़े से सदप्रयास की, आज के निर्देशकों को ज़िन्दगी से छोटे-छोटे पल चुराकर वो दिखा सकें जो गुरुदत्त और विजय आंनद ने संभव कर दिखाया।
यह सही है कि साहित्य अमूर्त कला है मगर उसमें निहित सौंदर्य की अनुभूति विरल है। साहित्यकारों का सिनेमा तभी सफल हो सकता है जब इसके लिए सम्यक और सकारात्मक संवेदना के अंकुरण निर्देशक के मन में घने वृक्ष की तरह फ़ैल जाए।
साहित्य और सिनेमा
What's Your Reaction?
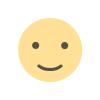 Like
0
Like
0
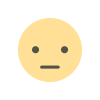 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
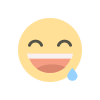 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
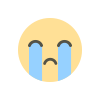 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0