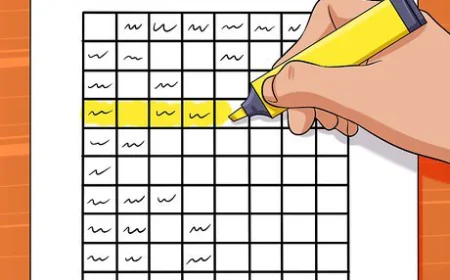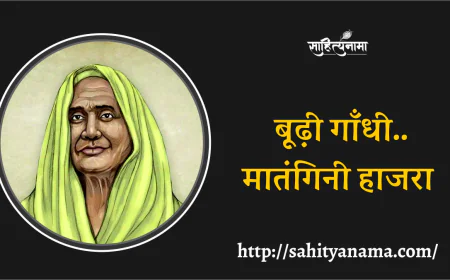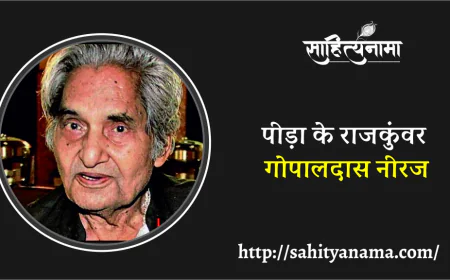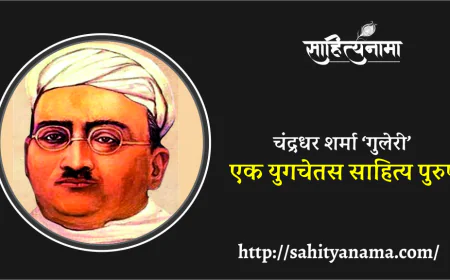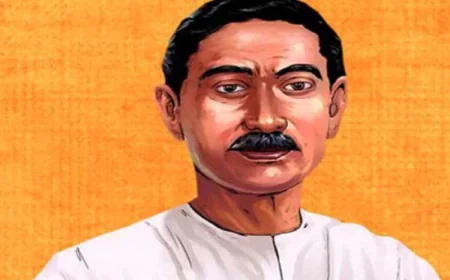समरस थे या चेतन
सुंदर साकार बना था
चेतना एक विलसती
आनंद अखंड घना था ?
कालजयी रचना ‘कामायनी’ महाकवि जयशंकर प्रसाद ने गोवर्धन सराय स्थित शिवालय में लिखी थी। यह शिवालय उनके पितामह शिवरतन साहू द्वारा निर्मित किया गया था, इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं प्रसाद जी के पूर्वज व्यवसाय के साथ ही शिव साधक थे, और भारतीय दर्शन, अध्यात्म , भारतीय कला, संस्कृति एवं दान आदि का भी ज्ञान रखते थे। इसलिए उनकी कृतियों में भारतीय संस्कृति, परंपराओं,और मानवीय संवेदनाओं की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी लेखनी न केवल साहित्य की ऊंचाइयों तक पहुंची, बल्कि उनके पारिवारिक संस्कार और परंपराओं ने उनकी रचनात्मकता को एक अद्वितीय आयाम भी दिया। उनके जीवन और रचनाओं को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उनके परिवार ने उन्हें किन परंपराओं और मूल्यों का उपहार दिया। प्रसाद जी का जन्म ३०/३१ जनवरी १८९० में काशी के समृद्ध परिवार में हुआ। प्रसाद जी का अद्भुत व्यक्तित्व था। प्रसाद जी के आदि पूर्वज जो कन्नौज से अपने धर्म और प्रतिष्ठा को बचाते हुए गंगा नदी जल मार्ग से पूर्व की ओर बढ़े और सैदपुर भीतरी की भूमि पर अपनी विचलित कुल-लक्ष्मी के प्रतिष्ठापनार्थ उनके पूर्वजों ने कन्नौज से आकर प्रायः तीन शताब्दियों तक अधिवास किया। मुगल-पठान संघर्ष वाले शेरशाही काल में सोलहवीं शताब्दी के मध्य हमारे पूर्वजों को वहाँ से हटना पड़ा और पुनः गंगा के तट से काशी के पश्चिम कुछ ही आगे अवस्थित मौजा बैरवन में वंश का दूसरा पड़ाव पड़ा। बैरवन और महाराजगंज में स्थापित चीनी कारखानों के अन्तिम पुरुष मनोहर साहु रहे। इनके जीवन के शेष दिनों में- अठारहवी शती के उत्तरार्द्ध में- कानपुर जा रही सात नाव चीनी गंगा में डूब गई, फलतः व्यवसाय उच्छिन्न हो गया। कारखानों में केवल शीरा और जूसी बचा-पूंजी भी नहीं रही जिससे उत्पादन हो सके। बैरवन के कारखाने के आसपास कुछ कृषि-भूमि थी जिसका उपयोग प्रायः चीनी उत्पादन से सम्बन्धित रहा। अब उस पर हल चलने लगा और कारखानों में बचे शीरे-जूसी से बनी पीनी तम्बाकू समीपवर्ती बाजार मोहन- सराय में बिकने लगी। मोहनसराय बनारस से प्रायः पाँच कोस दूर कलकत्ता से पेशावर जाने वाले मुख्य मार्ग (ग्राण्ड ट्रंक रोड) पर अवस्थित है। बनारस आने और यहां से जाने वालों का एक पड़ाव था जिसे यात्री और फौजी सैनिक पोषित करते थे। बन-बन कर उजड़ने और फिर बसने वाले इस केन्द्र पर विस्थापित और पुनः स्थापित होनेवाली हमारी वंश-परम्परा के शेष- पुरुष श्री मनोहर साहु विपन्न-प्राय जीवन का यापन पुरुषार्थ और साहस से करने लगे। तीसरे पुत्र श्री जगन साहु पिता का हाथ बटाते रहे। मोहनसराय के अध्यवसाय को पारिवारिक योगक्षेम के लिए अपर्याप्त देखकर वे उत्पादनों को बनारस लाकर बेचते और यहां से कुछ खूशबू मसाले भी तम्बाकू के लिए ले जाते। फलतः इस संकल्प की सिद्धि मे वे- जगन साहु अरुणोदय होते-होते माल और काँटा-वटखरा सिर पर लेकर चलते और सूर्यास्त तक बैरवन लौट जाते। श्री जगन साहू के उत्पादन की लोकप्रियता बढ़ती गई। जितना माल वे प्रातः लाते सब दोपहर तक बिक जाता। तब,वहीं माल बनाने के लिए किराये पर उन्होंने घर लिया। उसकी बाहरी दालान में दुकान चली। बैरवन से सम्पर्क कम होने लगा। महराजगंज का कारखाना तो समाप्त हो ही चुका था किन्तु बैरवन में कारखाने की भूमि और खेत बचा रहा, घर और कारखाना गिर कर डीह बन गया जिस पर अधुनापि शिवलिंग स्थापित है पुरोहित को उसे दान कर दिया। डीह और पुराने कारखाने का समीपवर्ती ध्वंस अभी विद्यमान है जिसे स्थानीय लोग सुंघनी साहू का डीह कहते हैं।
श्री जगन साहू के पुत्र श्री गुरुसहाय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और उनके दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती केसरा जी ने अपने पुत्रों (श्री गणपति और गोवर्द्धन) से कहा कि उस भूमि को लेकर उस पर शिवालय बनवाओ जहाँ बैठकर तुम्हारे पितामह( श्री जगन साहू) ने व्यवसाय आरंभ किया था। माता, भूमि तो सदयय ले लेंगे किन्तु शिवालय बनवाने में विशेष द्रव्य लगेगा उसकी व्यवस्था करके वह भी हम लोग करेंगे। माता कैसरा ने कहा तुम लोगों को इस काम की केवल व्यवस्था करनी है रुपया नहीं लगाना है वह मैं दूँगी। इस प्रकार गणपतेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा हुई जो वर्तमान में टेढ़ी नीम नाम का एक मोहल्ला वाराणसी में स्थित है। यह अठारहवीं शती के उत्तर भाग की कथा है। प्रायः उसी काल में अहिल्याबाई के द्वारा १७८५ में विश्वनाथ लिंग भी प्रतिष्ठित हुआ था।श्री गणपति एवं श्री गोवर्द्धन में परस्पर सौहार्द का अभाव होता गया। तब तक ये लोग २४ किता मकानों और हरहुआ स्थित एक बाग के स्वामी हो चुके थे। श्री गणपति साहू को, जिनका निधन चैत्र शु. सप्तमी सं. १८१८ को हुआ, एक मात्र पुत्र बी शिवरत्न साहू थे वे टेढ़ीनीम-हौजकटोरा छोड़कर गोवर्द्धन सराय में बस गए और शिवालय बनवाकर शिवरत्नेश्वर लिंग की स्थापना की। इस वंश परंपरा को शिवरत्न साहू जी के चौथे पुत्र देवी प्रसाद जी ने बहुत ही मनोयोग से आगे बढ़ाया वह अपने पिता के समान ही शिव भक्त दानी थे। उनके घर में विद्वानों एवं कलाकारों का बहुत ही सम्मान होता था। अध्यात्म एवं दर्शन म्ों जुड़े विद्वानों का भी आना- जाना लगा रहता था। उनकी धर्मपत्नी मुन्नी देवी भी इन सभी व्यवस्थाओं पर अलग से ध्यान दिया करती थी। देवी प्रसाद जी के दो पुत्र शम्भू रत्न एवं जयशंकर प्रसाद हुए। वे हमेशा से चाहते थे की प्रथम पुत्र व्यवसाय पर ध्यान दें और दूसरा पुत्र साहित्य और भारतीय संस्कृति परंपरा पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रसादजी की प्रारंभिक शिक्षा हेतु घर पर संस्कृत, उर्दू, फारसी एवं अनेक विषयों के विद्वानों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन माँ सरस्वती ने अपने इस साधक की पूर्ण रूप से परीक्षा ली, उन्हें अपने प्रियजनों का वियोग सहना पड़ा।
सबसे पहले अपने पिता का वियोग के साथ ही गृह कलह एवं संपति विवाद का भी उन्होंने सामना किया, पर इस समय वह अकेले नहीं थे। उनके बड़े भाई एवं माता उनके साथ घी पर कुछ ही दिनों में उनकी माता और बड़े भाई ने श्री उनका साथ छोड़ दिया। उनका वियोग साथ ही यह विवाद जो आगे चल रहा था उसका भी उन्होंने अकेले सामना किया। उनकी रुचि हमेशा साहित्य में रही फिर भी उन्होंने अपनी पूर्वजों द्वारा स्थापित तंबाकू के साथ पर पूर्ण ध्यान दिया और उसको पुनः स्थापित किया। इन सभी स्थितियों में उनका किसी ने अगर अंतर तक साथ दिया तो था। यह है उनकी बड़ी भाभी लखरानी देवी थी, जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रसाद जी का ध्यान रखा और उनका मार्ग प्रशस्त किया। प्रसादजी का प्रथम विवाह विध्यवासिनी देवी जी से हुआ, विवाह के कुछ वर्षों बाद ही विध्यवासिनी देवी जी यक्ष्मा रोग से ग्रसित हो गई, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी को बहुत ही बड़ा आघात लगा। परंतु वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद जी ने अपने भाभी के आग्रह को मानते हुए दूसरा विवाह उनकी चचेरी बहन सरस्वती देवी से किया। विवाह के एक वर्ष के अंतराल में ही प्रसव के दौरान सरस्वती देवी जी और नवजात शिशु दोनों का निधन हो गया। इसकी वजह से प्रसाद जी अत्यंत विक्षिप्त हो गए और वह किसी की ना सुनते हुए अष्टभुजा मंदिर विध्याचल पर्वत पर चले गए। वहीं उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की पर अपनी भाभी के आग्रह पर उन्हें पुनः लौटना पड़ा और फिर उनका तीसरा विवाह कमला देवी जी से हुआ जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई श्री रत्न शंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जीवन वैविध्यपूर्ण था। अपने जीवनकाल में उन्होंने अनेक तरह के उतार-चढ़ाव देखे थे। कहा जाये तो प्रसाद जी ने वैभव और विनाश का साक्षात्कार एक साथ किया था। बनारस के जिस परिवार की तूती बोलती थी, प्रसाद के समय में वह ऋणग्रस्त था। एक तरफ गिरती हुई आर्थिक स्थिति का कष्ट और दूसरी तरफ पारिवारिक जीवन की व्यथा को प्रसाद जी ने साहस के साथ झेला और मुक्ति के लिए अनवरत प्रयास किया। प्रसाद जी का जीवन काल छोटा था। १९३६ के अन्त में या १९३७ के आरंभ में वे लखनऊ गये थे। तब तक ‘कामायनी’ लिखी जा चुकी थी। वहाँ से लौटकर आते ही उन्हें ज्वर आने लगा। जाँच से राजयक्ष्मा होने का पता लगा और हर तरह का उपाय करने और न करने के बीच आखिर १५ नवम्बर १९३७ ई. की सुबह प्रसाद ने इस संसार से विदा ले ली। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में एक साथ लगभग समान साहित्यिक स्तर का लेखन कार्य किया है। एकांकी, नाटक, काव्य-नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास और निबंध आदि विद्याओं में फैला हुआ उनका विपुल साहित्य संसार उक्त तथ्य की गवाही देता है। प्रसाद जी की रचनायें सन् १९०९ (इन्दु के प्रकाशन से) लगातार प्रकाशित होने लगी थीं और १९३७ में मृत्यु के कुछ दिनों पूर्व तक प्रसाद रचनारत रहे।
काव्य- कामायनी,चित्राधार, प्रेमपथिक, कानन कुसुम, झरना, आँसू, लहर ।
नाटक- सज्जन, वभ्रुवाहन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राज्यश्री, प्रायश्चित, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कन्दगुप्त, एक प्रैट, चन्द्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी।
कहानी संग्रह- छाया, प्रतिधविनि, आकाशदीप, आँधी, इन्द्रजाल।
उपन्यास- कंकाल, तितली ।
काव्यकला और अन्य निबंध, इरावती’ (अपूर्ण अपन्यास), अग्निमित्र (अपूर्ण नाटक) का प्रकाशन प्रसाद की मृत्यु के बाद हुआ ।
प्रसाद की काव्यकला का सर्वोत्तम प्रस्फुटन ‘कामायनी’ में हुआ है।
भारतीय अतीत और उसकी प्राचीन संस्कृति के प्रेमी होते हुए भी प्रसाद जी ने कामायनी में नवीन वैज्ञानिक तथ्य का भी यचेष्ट उपयोग किया है। उनकी यही विशेषता उनके काव्य की आधुनिकता प्रदान करती है। मानव जीवन आज अनेकानेक जटिलताओं और विषमताओं से ग्रस्त है। उन जटिलताओं का दिग्दर्शन कराना और उनके निवारण का उपाय बताना हर क्रान्तिदर्शी कवि का धर्म है। प्रसाद जी ने कामायनी में अपनी इसी क्रांतिदर्शिता का परिचय दिया है। प्रसाद जी को काशी से अगाध प्रेम था। वे काशी छोड़ और कहीं भी नहीं जाना चाहते थे। राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो जाने पर लोगों की सलाह थी कि उन्हें किसी सेनीटोरियम में रखा जाय। पूरी तैयारी के बाद भी प्रसाद ने काशी छोड़ना स्वीकार नहीं किया। प्रसाद को काशी से प्यार था, सारनाथ से प्यार था, काशी के कण-कण से प्यार था। सारनाथ में मूलगंध कुटी विहार की स्थापना के समय प्रसाद स्वयं वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने यह गीत सुनाया था- ‘अराr वरुणा की शान्त कछार। तपस्वी के विराग की प्यार। यह गीत आज भी वरुणा नदी के पुल पर अंकित है।
साभार:ञ्डॉ. कविता प्रसाद (पड़पौती)
डॉ. विजय पाटिल
बड़वानी, म.प्र.
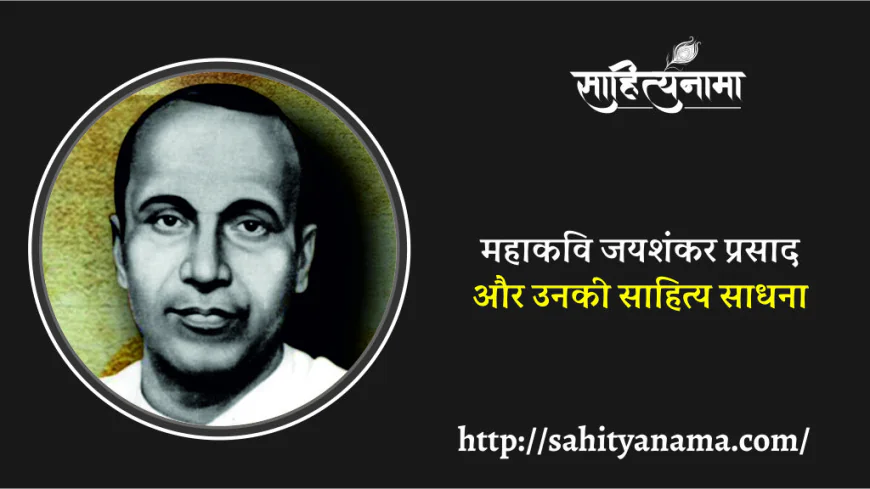
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
1
Sad
1
 Wow
0
Wow
0