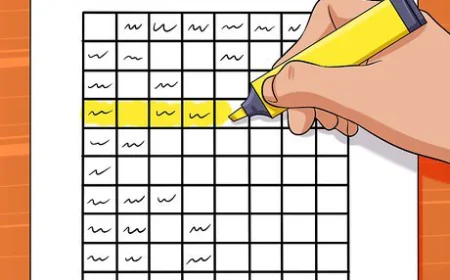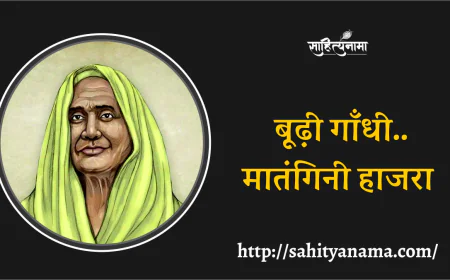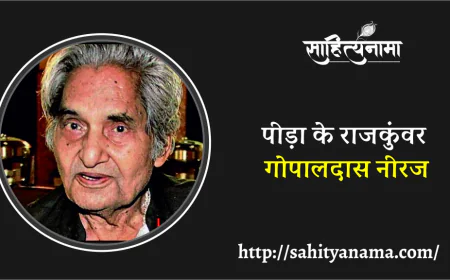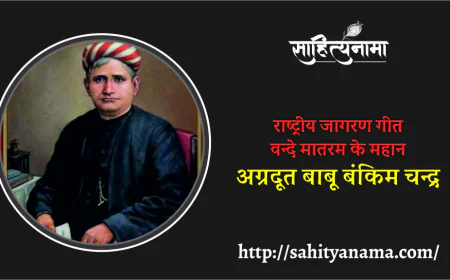शताब्दी वर्ष में मानवीय सरोकारों के चितेरे कृष्ण बलदेव वैद के साहित्य का पुनर्पाठ आवश्यक !
Krishna Baldev Vaid was one of the pioneering experimental writers in Hindi literature who blended global literary trends with Indian emotions and realism. His works like “Uska Bachpan,” “Woh Guzra Zamana,” “Ek Naukarani Ki Diary,” and “Kaala Kolaj” depict partition trauma, social conflict, and human psychology. Vaid’s unique fusion of Hindi, Urdu, and Punjabi redefined modern Hindi prose with unmatched linguistic creativity.कृष्ण बलदेव वैद को भाषा के नए सौंदर्यशास्त्र गढ़ने और अपनी तरह का मुहावरा गढ़ने के लिए लिए जाना जाता है। उनका गल्प संसार ने हिंदी के पाठकों को दशकों तक चमत्कृत किया और गद्य को नया आयाम दिया। भाषा का यह चमत्कार उन्होंने हिंदी की पड़ोसी जुबानों उर्दू और पंजाबी को मिलाकर किया क्योंकि उर्दू उनके बचपन के परिवेश की भाषा थी और पंजाबी उनकी मां की बोली। हिंदी-उर्दू-पंजाबी से गुंथा ऐसा अद्भुद शब्द संसार हिंदी साहित्य में किसी अन्य लेखक के पास उपलब्ध नहीं है।
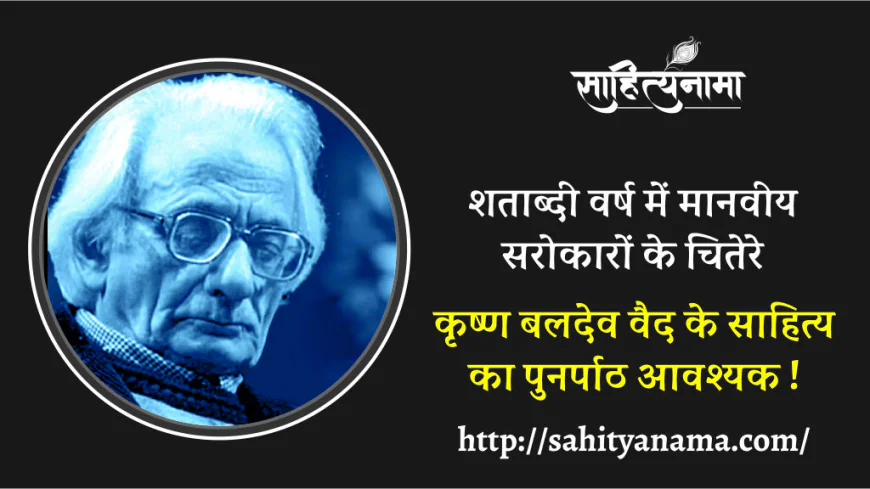
कृष्ण बलदेव वैद हिंदी साहित्य के पहले प्रयोगधर्मी रचनाकार थे जिन्होंने वैश्विक साहित्य के रुझानों को भारतीय संवेदना के साथ जोड़कर विपुल साहित्य की रचना की। उनका साहित्य संसार जहाँ एक और अपने संरचना मैं वैश्विक है तो वहीं अपने कंटेंट में विशुद्ध भारतीय।
कृष्ण बलदेव वैद का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब के डिंगा कस्बे जो कि अब पकिस्तान का हिस्सा है, में २७ जुलाई १९२७ को हुआ था। विभाजन के बाद उन्हें भारत आना पड़ा जिसकी पीड़ा उनके साहित्य में झलकता है। वर्ष १९४९ में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और फिर १९६१ में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की। कृष्ण बलदेव वैद भारत के विभिन्न कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी और ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में रहे। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई भी की और पढ़ाया भी, लेकिन लिखने के लिए हिंदी को चुना। प्रायः यही कारण है कि वैद ने हिंदी में लिखते हुए ऐसे भाषागत प्रयोग किए जो उनसे पहले या उनके बाद के किसी लेखक ने नहीं किए। हिंदी साहित्य में निर्मल वर्मा और कृष्णा सोबती जैसे लेखकों ने भी भाषा के स्तर पर कई प्रयोग किये किन्तु बलदेव वैद ने यह काम अलग किस्म की विलक्षणता के साथ किया।
कृष्ण बलदेव वैद को भाषा के नए सौंदर्यशास्त्र गढ़ने और अपनी तरह का मुहावरा गढ़ने के लिए लिए जाना जाता है। उनका गल्प संसार ने हिंदी के पाठकों को दशकों तक चमत्कृत किया और गद्य को नया आयाम दिया। भाषा का यह चमत्कार उन्होंने हिंदी की पड़ोसी जुबानों उर्दू और पंजाबी को मिलाकर किया क्योंकि उर्दू उनके बचपन के परिवेश की भाषा थी और पंजाबी उनकी मां की बोली। हिंदी-उर्दू-पंजाबी से गुंथा ऐसा अद्भुद शब्द संसार हिंदी साहित्य में किसी अन्य लेखक के पास उपलब्ध नहीं है। अपने इस शब्द संसार को वे स्मृतियों की बुनियादी जमीन कहा करते थे जिससे उन्होंने सफलता के शिखर पर चढ़कर भी अपने कदम नहीं हटाए।
स्मृतियों की बुनियादी जमीन पर उनके पैर टिके तो थे लेकिन विभाजन के कांटे उन्हें चैन से रहने नहीं दिया और यही उथल-पुथल उनके दो उपन्यासों `उसका बचपन' और `वो गुज़रा ज़माना' में अभिव्यक्त हुआ। जहाँ `उसका बचपन' विभाजन के पहले की पृष्टभूमि पर लिखा गया हैं वहीँ `वो गुज़रा ज़माना' विभाजन की त्रासदी के गर्भकाल और जन्म पर लिखा गया है जिसे हम आज भी विभाजन के ऐतिहासिक, सामजिक और साहित्यिक एवं भावनात्मक दस्तावेज के तौर पर देख सकते हैं। `वो गुजरा जमाना' हिंदी का कालजयी उपन्यास है और विश्व स्तरीय कृतियों में शुमार है। इस उपन्यास अपनी भाषात्मक विविधता, कलात्मक जटिलता और सम्वेदनात्मक चेतना के कारण कालजयी बना है। यह उपन्यास हिंदी साहित्य के उपन्यास के पारम्परिक संरचना को बार बार तोड़ता है। कृष्ण बलदेव वैद ने कहा था कि 'वो गुजरा जमाना' सरीखी रचना बने-बनाए सांचों में संभव ही नहीं क्योंकि विभाजन की प्रक्रिया इतनी जटिल और संक्रमण भरी थी। जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितयां देश में हैं, जिस तरह की समकालीन परिस्थियों और असहिष्णुता एवं अविश्वास के दौर से देश गुज़र रहा है `वो गुजरा जमाना' अपनी प्रासंगिकता का खुद पुनर्जन्म करता है। कृष्ण बलदेव वैद की बड़ी/कालजयी साहित्यिक कृति का 'सबकुछ' बदले हुए हालात में भी प्रासंगिक बना हुआ है। ‘काला कोलाज’, ‘बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहां’, ‘नसरीन’, ‘दूसरा न कोई’, ‘दर्द ला दवा’, ‘मायालोक’, ‘नर-नारी’, ‘एक नौकरानी की डायरी’ उनके अन्य उपन्यास हैं। उन्होंने बीस से ज्यादा कहानी संग्रह और नाटक भी लिखे। कृष्ण बलदेव वैद की सभी रचनाएं सामाजिक द्वंदात्मक मनोविज्ञान की यथार्थवादी छवियों से ओतप्रोत हैं और इनकी भाषा का सौंदर्य खिली धूप जैसा है। आलोचनाओं की परवाह किये बिना उन्होंने अपनी अलग रचनात्मक दुनिया बनाई।
उनकी प्रतिनिधि कृतियां मानवीय सरोकार से भरे हुए थे जो `साहित्यिक आनंद' के लिए नहीं थे बल्कि `बेचैनी भरे आत्मिक संवाद' के लिए थे। मुक्तिबोध ने एक बार कहा था कि जब जीवन इतना जटिल है तो उसे साधारणता से व्याखित नहीं किया जा सकता है और वैद ख़ामोशी के साथ मुक्तिबोध की इस अवधारणा को अचेतन रूप से सार्थक करते रहे। वे प्रगतिशील और अप्रगतिशील की व्याख्या से परे भी अपनी रचनाधर्मिता को मानवीय चेतना के प्रति प्रतिबद्ध रहे।
कृष्ण बलदेव वैद से पहले भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी साहित्य, कविता, कहानी और उपन्यास की विधा थी। सम्पूर्ण भारतीय साहित्य विशेषकर हिंदी साहित्य को कृष्ण बलदेव वैद की एक बड़ी देन साहित्य की अनौपचारिक विधाओं, डायरी, पत्र-संवाद और अपने समकालीनों, विशेषकर कृष्णा सोबती के साथ मौखिक संवाद है। पांच खंडों में अलग-अलग समयकाल की उनकी प्रकाशित डायरियां उनकी समस्त जीवन यात्रा सामने रखती हैं। ढलती उम्र में लिखी डायरियों के पन्नों में `मौत के दस्तखत/आभास' जगह-जगह मिलेंगे। एक बड़ा लेखक-बुद्धिजीवी, `महान बुद्धिमान शब्दजीवी' मौत का कैसे इंतजार करता है और जिंदगी की निरंतर स्थगित अथवा लुप्त होती धूप को किस मनोदशा के साथ भुगतता है- इससे साक्षात्कार करने के लिए कृष्ण बलदेव वैद की डायरी से गुज़रना होगा।
कृष्ण बलदेव वैद किसी खेमे, किसी वाद से जुड़े नहीं रहे किन्तु उनके उपन्यास और नाटक उनके मानवीय सरोकारों से जुड़े होने का सबूत देते रहे। उदहारण के तौर पर हम उनके नाटक 'भूख आग है' को देख सकते हैं जिसका कथासार यह है कि एक अमीर परिवार की लड़की ‘भूख की तलाश’ विषय पर निबंध लिखना चाहती है। उस दरम्यान उसे भूख के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, संवेदना के अलग-अलग स्तर पर। जिंदगी की सच्चाइयों के प्रति हमारी असंवेदनशीलता और उदासीनता उजागर होती हुई। कृष्ण बलदेव वैद ने खुद इस नाटक पर टिप्पणी की है, ‘युवा दिनों में मैं सुनहरे वर्गहीन समाज का स्वप्न देखा करता था, जिसमें गरीबी नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, ऊंच-नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, भूख नहीं होगी। उन्हीं स्वप्नों की राख में फूंक मारने की कोशिश है यह नाटक, उसमें अब प्रश्न उठता है कि रचनाकार को वाद से जुड़ा होना जरुरी है या वाद के अंतिम उद्देश्य से ?
ये भी पढ़ें- प्रेम और सौंदर्य के कवि धर्मवीर भारती
मानवीय चेतना के विविध पक्षों के प्रति सरोकार और भारतीय तथा विश्व साहित्य पर सारगर्भित चिंतन भी इनके साहित्य के स्वर में मिलेगा। कृष्ण बलदेव वैद की डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक तरफ समकालीन लेखकों पर उनका नजरिया मिलेगा तो दूसरी तरफ सपनों की अद्भुत दुनिया भी मिलेगी जो कि उनकी डायरियों के अहम आधार-वस्तु हैं। प्रवास के सुख-दुख और अपनी जमीन से कटने, मिट्टी जड़ से अलग होने की पीड़ा जैसा उनकी डायरी में व्यक्त हुआ हुआ है वह कहीं और नहीं है।
उन्होंने जालंधर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाया। मोहन राकेश और भीष्म साहनी से उनकी मुलाकात यहीं हुई। अलबत्ता करीबी दोस्ती, उर्दू के साहित्यकारों फिक्र तौंसवी और मख्मूर जालंधरी के साथ थी। साल १९६२ से १९६६ तक वह पंजाब विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में रहे। उसके बाद विदेश प्रवास का सिलसिला शुरू हुआ और वहां के नामी विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण किया। लेखन हिंदी-उर्दू-पंजाबी की संयुक्त `हिंदुस्तानीयत' में जारी रखा।
कृष्ण बलदेव वैद की भारत और अमेरिका के बीच उनकी आवाजाही बराबर रही, लेकिन उनकी लेखनी की धारदार निब भारत की मिटटी में ही सनी-डूबी थी। उनपर पश्चिम के प्रभाव के आरोप लगते रहे लेकिन जो आदमी एक नौकरानी की डायरी सरीखी रचना हमें दे सकता है, वह भला बाहरी प्रभावों में एक मौलिक रचनाकार कैसे बना रह सकता है। यह कृति नागर जीवन के उन जरूरी लोगों के जीवन की कहानी है, जो हमारी सोच और व्यवहार में उपेक्षित रहते हैं, लेकिन उनके बिना नगरीय जीवन विकलांग हो जाता है। इसमें एक युवा होती नौकरानी की मानसिक स्थिति और उसके भीतर उथल-पुथल को बड़े मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। डायरी शैली में लिखे हिंदी के पहले उपन्यास में उपेक्षित-वंचित वर्ग और कुलीन समाज के अंतर्विरोधों और विडंबनाओं को चित्रित किया गया है।
उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अभाव को देखा और समझा तथा उस अभाव के भीतर की भूख और आग को देखा। उन्होंने विभाजन का दंश देखा, असहिष्णुता देखी, साम्प्रदायिकता देखी। आज इस शताब्दी वर्ष में कृष्ण बलदेव वैद की रचनाएं पुनर्पाठ की मांग कर रही हैं क्योंकि वे अपनी सामाजिक समझ, विद्रूपताओं एवं विडंबनाओं को उद्घाटित करने की कला के कारण प्रासंगिक बने हुए हैं, बने रहेंगे।
अरुण चंद्र राय
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0