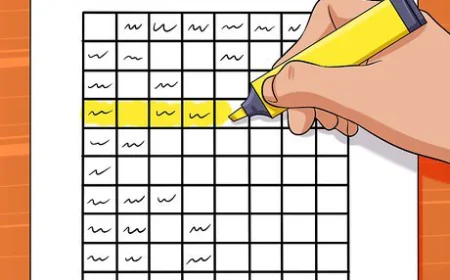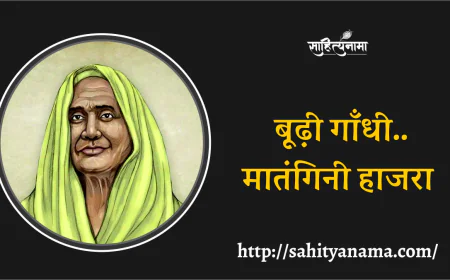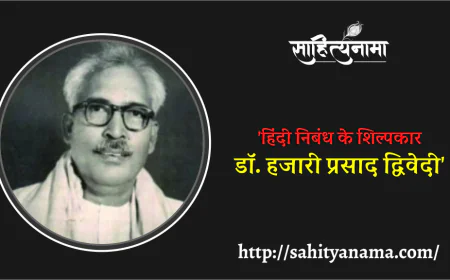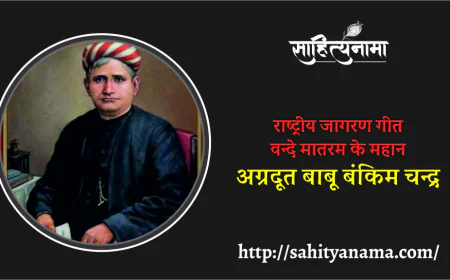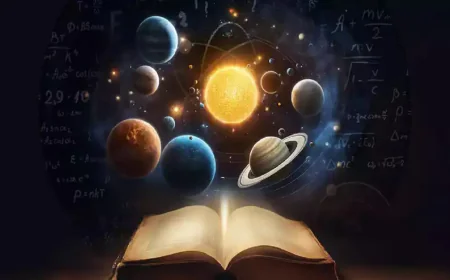माई
आजकल एक बच्चे पालन-पोषण में मानों पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, घर-परिवार सब परेशान हैं। बच्चे मोबाइल देखकर खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। मेरी माँ अकेले ही खाना बनाती, बर्तन मांजती,घर साफ करती, कपड़े धोती, सबको खाना परोसती,उतना ही अनाज भी जाँत में पीसती,ओखली में धान भी कूटती, स्वेटर भी बुनतीं, सिलाई भी कर लेती। माँ कब सोती पता नहीं। उस पर बाबूजी का ठाकुरी दरबार' दरवाजे पर पंचायत चलती रहती थी। चाय-पानी का दौर चलता रहता था।

माँ को स्वर्गवासिनी हुए लगभग सत्ताइस वर्ष हो गए किंतु आँखों के समक्ष सदैव दिखलाई पड़ती है माँ। खुली आँखों से दिखता है सारा संसार किंतु दर्द में, दुख में, पलक बंद करते ही, आर्तस्वर में पुकारते ही खड़ी हो जाती है माँ। सिर पर हाथ फिराने लगती है, दुख दर्द पूछने लगती है, समझाने लगती है। माँ जैसा रिश्ता इस संसार में कोई नहीं है। यदि है तो वह कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं। आज तो सब माँ को अम्मा, माँ, मम्मी, मम्मा, ममा कहकर पुकारते हैं किंतु बचपन में हम सब पिता को बाबू तथा माँ को माई कहते थे।
माँ की हम सब तीन भाई तीन बहन कुल छः संतानें थीं। पिताजी मध्यमवर्गीय किसान थे। गरीबी थी, संसाधनों का अभाव था किंतु माँ के प्यार, दुलार, मनुहार की कमी नहीं थी। आजकल एक बच्चे के पालन-पोषण में मानों पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, घर-परिवार सब परेशान हैं। बच्चे मोबाइल देखकर खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। मेरी माँ अकेले ही खाना बनाती, बर्तन मांजती, घर साफ करती, कपड़े धोती, सबको खाना परोसती, उतना ही अनाज भी जाँत में पीसती, ओखली में धान भी कूटती, स्वेटर भी बुनतीं, सिलाई भी कर लेती। माँ कब सोती पता नहीं। उस पर बाबूजी का ठाकुरी दरबार दरवाजे पर पंचायत चलती रहती थी। चाय-पानी का दौर चलता रहता था। उस पर मेहमान भी आजकल की तरह एक मीटिंग के लिए नहीं आते थे, दो-तीन दिन के लिए आते। भैने-भैनवार तो हफ्तों टिके रहते थे। किंतु माँ को परवाह नहीं, गिला-शिकवा नहीं, मशीन की तरह माँ दिन-रात खटती रहती थीं। पिताजी कभी प्रशंसा नहीं करते थे बल्कि नुक्स ही निकालते थे।
कोई शिकायत करता तो उसकी आँखे नम हो जातीं, और अपने आँचल से आँसुओं को पोंछ लेतीं। कोई भी बच्चा बीमार हो, वह देशी दवा, काढ़ा, चूरन देतीं। एक कुशल नर्स की तरह उसके पास खड़ी रहतीं। देवी- देवता, पूजा, देवस्थान दर्शन की मन्ता-मन्नत मनाने लगतीं।
मेरी माँ निरक्षर थीं किंतु धर्मपरायण थीं। पूजा-पाठ पूरे मन से करती थीं। संस्कार से माँ को रामायण तथा महाभारत का काफी ज्ञान था। अनपढ़ माँ की बार-बार प्रयुक्त की गई उक्ति ‘नन्हें गियान का एक-एक शब्द अशरफी के बराबर समझ के सीखा, तबई गियानी बनबा।' का मेरे अनगढ़ मन पर विशेष छाप पड़ी। यद्यपि मुझे कक्षा ८वीं से स्कालरशिप मिलती थी। जब इण्टरमीडिएट तक पैदल ही कॉलेज जाता था तो आर्थिक समस्या नहीं थी किन्तु जब टी़ डा़० कालेज जौनपुर में रूककर पढ़ने लगा तो पैसे कम पड़ते थे। माँ अरहर, सरसों बेचकर पैसे देती थी। गेहूँ, गुड़ बेचकर कभी-कभी। माँ की बडी संदूक अक्षय पात्र थी। जब कोई मेहमान आता तो उस काठ के बक्से में रखे संदूक से कुछ न कुछ सामान निकलता, कभी-कभी कपड़े में बांधकर रखे मुड़ी-चौपत्ती नोटें, सिक्के निकलते। कुछ विशेष अवसर पर पहनने वाली धराऊँ साड़ियों के अलावा गहनों की एक छोटी गठरी बाँधकर उसमें रखती थी। पिताजी क्रोधी स्वभाव के थे। अनुशासन बनाए रखने के लिए डांटते रहते थे किंतु जब मारने के लिए बढ़ते तो वह बीच में आकर बोलती ‘लड़िकन से दुई जबान प्रेम से बोलि नाइ सकथ। जब देख तबई डेरवावत रहथ।' पैदा होते ही मैंने माँ को बहुत दुःख दिया। जब मैं गर्भ में था, माँ बहुत बीमार रहती थीं। बहुत कमजोर हो गई थीं। उस समय नजदीक में डॉक्टर, अस्पताल नहीं होते थे।
बाजार में इक्के-दुक्के वैद्य, हकीम होते थे जो आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाएं देते थे, जड़ी बूटियाँ देते थे। किसी तरह माँ के महीने पूरे हुए, घंटों प्रसव-पीड़ा होने के बाद भी मैं पैदा नहीं हुआ। गाँव की बुजुर्ग महिलाएँ ही दाई का काम करती थीं। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया किंतु धीरे-धीरे हार मानने लगीं। माँ रोए जा रही थीं। सभी ने कहा, ‘अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।’ आज तो गाँव -गाँव तक सड़कों का जाल बिछा है। एक फोन करने पर गाँव में गाड़ी दरवाजे पर आ जाती है किंतु उस समय देश को आजाद हुए भले दशकों बीत चुके थे किंतु आवागमन की साधन सम्पन्नता नहीं' थी।
गाँव के प्रधान और वरिष्ठ लोग विचार विमर्श कर रहे थे। अब क्या किया जाय? उस दिन रंग और भंग का त्योहार होली था किंतु पास-पड़ोस में रंग में भंग पड़ने के हालात दिख रहे थे। गाँव-की स्त्रियाँ माँ को देखकर आपस में काना-फूसी करने लगीं। एक दूसरे से बतियाती- ‘अब तो ठकुराइन का बचना मुश्किल है।’ एक खाट में बाँस लगाकर डोरी की सहायता से डोली बनाई गई। गाँव से बाजार लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के बाद ही इक्का, तांगा अथवा अन्य साधन मछलीशहर जाने के लिए मिलता था। पहलवान होने के कारण पिताजी हनुमानजी के भक्त थे। माँ भी देवियों की पूजा करती थीं। माँ रोते-रोते थक चुकी थीं। पिताजी मन ही मन भगवानका सुमिरन कर रहे थे। कई महिलाओं ने माँ को उठाने का प्रयास किया जिससे दरवाजे पर लाकर डोली में बैठा सकें किंतु माँ उठते-उठते जमीन पर गिर गई। पड़ोस की दादी लगने वाली काको ने सबको रोका। माँ को उठाने के कारण प्रसव पीड़ा बढ़ गई जिससे मैं तो पैदा हो गया किंतु माँ बेहोश हो गईं। काको के प्रथमोपचार करने के बाद माँ होश में आ गई। माँ के होश म्ों आते ही महिलाओं ने सोहर गाना शुरू किया। विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है। दुख के थपेड़े से जो रंग में भंग पड़ गया था मेरे पैदा होते ही होली का हुड़दंग शुरू हो गया।
माँ ने तीन बेटे, तीन बेटियों का पालन पोषण बड़ी तन्मयता से किया। बाबूजी खाने-पहनने के बहुत शौकीन थे। माँ खाने-पहनने में अपने ऊपर कम से कम खर्च करती थीं। स्वयं कम खाती थी, बच्चों को खिला देतीं। जिससे शारिरिक रूप से माँ कमजोर रहती थीं। जिसके भाग्य में जितना लिखा था पढ़ाया-लिखाया। बाबूजी के ज्यादा सामाजिक होने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियाँ माँ ने अधिक निभाया। छः बेटे-बेटियों की शादी करना आसान नहीं होता। आर्थिक विपन्नता होने के बाद भी यथोचित विवाह किया गया किंतु कई बीघे खेत बिक गए।
माँ पेट की रोगी थीं। उनके पेट में गैस होती थी जिससे दर्द होता था। पेट की मालिश करने पर राहत हो जाती थी। हर्रे-बहेड़ा का चूरन बनाकर खाती रहती थीं। धीरे-धीर वह कमजोर होने लगी। वर्ष में मैं दीपावली, ग्रीष्मावकाश के अलावा एक बार आकस्मिक अवकाश लेकर घर जाता था। पत्नी को आँगनवाडी में पढ़ाने की नौकरी गाँव में लग चुकी थी किंतु विवाह के छः बर्ष बीत चुके थे, अब तक कोई संतान नहीं थी। तीन वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद, कर्ज लेकर किसी तरह चाल में एक रूम लिया गया। दीपावली के समय में माँ और पत्नी को मुंबई लाया। माँ को अस्थमा की शिकायत थी उसके लिए डॉक्टर को दिखाया गया, जिससे उसे कुछ राहत हुई। मेरा घर छोटा था। तीन भाई, माँ और पत्नी रहने वाले थे।
माँ तीन महीने मुंबई में रही। मुंबई के दर्शनीय स्थलों को दिखाया गया। माँ को गाँव की याद सताने लगी तो भला उसका मन यहाँ कैसे लगता? महिलाओं को बतियाने, निंदा रस लेने का आनंद जो गाँव में है वह भला शहर में कहाँ? आते-जाते चाल की महिलाएँ केवल एक ही बात पूछती केवल एक ही प्रश्न पूछती, ‘माताजी खाना खाई। चाय पी?' माँ केवल हाँ या न में उत्तर देकर चुप हो जातीं। उसका ध्यान गाँव के पोतों पर भी लगा रहता था। आँगनवाड़ी की परीक्षा के कारण पत्नी को भी गाँव जाना था। माँ भी गाँव चली गई उसके बाद बहुत कहने के बाद भी माँ मुंबई नहीं आई।
कई वर्ष तक पेट के रोग एवं अस्थमा के कारण माँ कमजोर हो गई थी। खाना भी बराबर नहीं खा पाती थीं। भूख भी नहीं लगती थी। गाँव से सत्यनारायण पांडेय मुंबई आए। माँ की बीमारी की चर्चा करते-करते रो पड़े और बोले, ‘चाची का अंतिम समय आ गया है। परिवार भर एक बार जाकर मिल लो।’ अप्रैल का महीना दिवसकालीन और रात्रिकालीन दो-दो विद्यालयों की परीक्षा गाँव जाने के लिए टिकट की विकट समस्या, तीन महीने का बेटा। सारी परिस्थितियाँ एक तरफ माँ का अंतिम दर्शन एक तरफ। किसी तरह दो वीआईपी कोटे से टिकट मिला। किसी तरह पूरा परिवार गाँव पहुँचा। अस्पताल में दिखाने, जाँच कराने से पता चला माँ को अल्सर था। शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन भी संभव नहीं था। इसलिए माँ की सेवा-सुश्रूषा, दवा घर पर ही होने लगी। उस वर्ष मई महीने में बीएम.सी. का चुनाव घोषित हो गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं चुनाव अधिकारी का आदेश रजिस्ट्री द्वारा मुंबई वापस आने के लिए आया। मैंने तय कर लिया माँ को अंतिम समय में छोड़कर नहीं जाऊँगा।’ माँ ने अन्न लेना छोड़ दिया। अब जूस, दाल का पानी, दूध पर रहने लगीं। खाट पर पड़ी रहती। ऐसे समय में प्रतिदिन सुबह स्नान करके तथा शाम को भी चटाई पर बैठकर गीता-रामायण सुनाता। वह घंटो हाँ-हाँ करती, कभी-कभी सो जाती। कभी-कभी दर्द से कराहती तो दर्द की दवा दी जाती।
३० अप्रैल की शाम माँ का बोलना बंद हो गया। गरमी बहुत थी। बहुएँ बच्चे छत पर सोने चले गये। माँ की खाट आँगन में थी। बगल में एक खटोला था। जिसपर कोई न कोई माँ की देखरेख करता था। बाबूजी, भाई साहब एवं मेरी खाट दरवाजे पर बिछी थी। एक बजे मेरी चार वर्षीय बेटी छत पर जोर-जोर से रोने लगी। दरवाजे पर मेरे पास आने की जिद कर रही थी। जिससे सब जग गए। मेरी पत्नी ने दरवाजा खोलकर मुझे पुकारा, ‘गुड़िया के पापा देखो अम्मा कैसी हो गई हैं?’
मैं दरवाजे से घर के अंदर गया। माँ की आखें बंद थीं। साँसे धीरे-धीरे चल रही थीं। माँ का हाथ अपने हाथ मे लेकर माई-माई' कई बार बुलाया। वह नहीं बोली। परिवार के सभी सदस्य आँगन में खड़े थे। बाबूजी ने दबी आवाज में कहा, ‘इसका अंतिम समय आ गया है। अब तुलसी गंगाजल पिलाओ।' परिवार के सभी सदस्यों ने मुँह में गंगाजल डाला। यहाँ तक कि तीन महीने के बेटे अनुराग से भी माँ के मुँह में गंगाजल डलवाया गया। तीन बहुएँ, दो-दो बेटे पोते-पोतियाँ, पति सब खड़े थे। लाचार, विवश मौन। माँ के सिर को गोद में रखकर बोला, ‘माई राम-राम कहो।' माँ की धीमी चलने वाली साँसें खरखराने लगीं। कुछ देर बाद एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ की साँसें सदा-सदा के लिए बंद हो गईं। पूरे घर में कोहराम मच गया। सभी जोर-जोर से रोने लगे। पड़ोसी और गाँववाले भी आ गए। बाबूजी मुझे रोता देख बोले, ‘रामसिंह तुम भी रो रहे हो। सुबह लगन है। गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। तुरंत बाजार जाओ। तीन-चार गाड़ियों की व्यवस्था करो।’
डेढ़ बजे रात तीन लोग साइकिल से बंधवा बाजार गए। तीन जीपों की व्यवस्था हुई। पुरोहित को बुलाकर पिंडदान की व्यवस्था सेवान के बाहर किया गया। चौबीस-पचीस लोग बनारस गए। गंगातट पर माणिकर्णिका घाट पर दाह-संस्कार हुआ। बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। धू- धू करके माँ की चिता जल रही थी। सबकी आँखों में आँसू थे। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। राजा, रंक, फकीर यहाँ सब बराबर हो जाते हैं।
राम सिंह
कांदिवली, मुंबई
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0