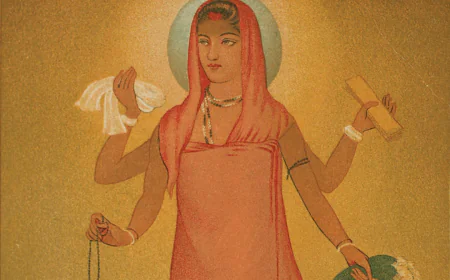इतिहास शब्द संस्कृत के ‘इति’ त्र्‘ह’त्र्‘आस’ शब्दों के मेल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है-‘ऐसा ही था’ या ऐसा ही हुआ। इस व्युतपत्तिगत अर्थ से दो बातें उभर कर सामने आती है-१ इतिहास का संबंध अतीत से है। २ इतिहास का संबंध यर्थाथ घटनाओं से है। अतीत के तथ्यों का वर्णन-विश्लेषण, जो कालक्रमानुसार किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमे तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो, उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे ‘कलात्मक’ रूप देते हेै।
इतिहास विज्ञान है या कला इस पर विद्वानों के विभिन्न मत है। डा० नगेन्द्र ने इस पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए लिखा है-‘‘जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषयवस्तु के आधार पर नहीं, अपितु उसकी अध्ययन-पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत प्रदान करता है, किन्तु यह हम पर निर्भर है कि उस इतिवृत्त का उपयोग हम किस प्रकार करते है। यदि अतीत के इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोंण, वैयक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली मे प्रस्तुत करते है तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो सकता है, जबकि वस्तुपरक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति से प्रस्तुत किया अतीत का विवरण ‘विज्ञान’ की विशेषताओं से युक्त माना जा सकता है.....फिर भी आधुनिक युग मे इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। इतिहास को भी हम उसी श्रेणी के विज्ञान मे स्थान दे सकते है, जिस श्रेणी मे भाषाविज्ञान व सामाजिक विज्ञान को देते है।’’१ (स० डा नगेन्द्र-हिन्दी साहित्य का इतिहास)
इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ‘अथर्ववेर्द’ मे मिलता है। ‘शतपथ ब्राहम्ण’ जैमिनीय वृहदाराण्यक तथा ‘छान्दोग्योपनिषद्’ में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति मे सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन तत्वों का अधिक महत्व रहा है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। जिसमें ‘सत्यम, शिवम, सुन्दरम’ का समन्वय की ओर ध्यानाकर्षण रहा है। महाभारत के रचियता वेदव्यास जी के अनुसार-
धर्मार्थकामोक्षणामुपदेशसमन्वितम्।
पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते।।
भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक सीमित नहीं रहा वह उसे शिव एवं सुन्दर रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास मे कला एवं नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया।
पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः यथार्थवादी, वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते है। इतिहास के चार लक्षण यूनानी विद्वान ‘हिरोदोतस’ ने निर्धारित किये है-
१. इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है।
२. यह मानविकी के अन्तर्गत आता है, अतः मानव जाति से सम्बन्धित है।
३. इसके तथ्य, निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते है।
४. यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है।
पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद प्राणिशास्त्र पर, मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर, स्पेन्सर का विकासवाद भौतिकशास्त्र पर लागू होता है।
साहित्य के इतिहास मे हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे करते है। साहित्य के इतिहास को समझने के लिये तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है,साथ ही इनके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक है।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ‘‘साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते है। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियो के अनुरूप बदलता है।’’ शुक्ल जी की यह भी धारणा है कि साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखण्डों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप साहित्य मे जो प्रवृत्तियां प्रवर्तित होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिये।
डा. गणपति चन्द्र गुप्त ने भारत के इतिहास संबंधी परम्परागत दृष्टिकोण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है-
१. भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास लेखन में उन्होंने काल, तिथि, सन्-सम्वतों को महत्व नहीं दिया।
२. व्यक्तियों का मूल्यांकन उन्होंने लौकिक सफलताओं के आधार पर न करके चारित्रिक महत्व के आधार पर किया।
३. उनकी शैली विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक न रह कर संश्लेषणात्मक एवं भावात्मक रही।
४. उन्होंने इतिहास को विज्ञान के रूप मे नहीं, कला के रूप मे ग्रहण किया।
इतिहास-दर्शन
‘इतिहास दर्शन अंग्रेजी शब्द ‘फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री’ का पर्याय है। सर्वप्रथम वाल्तेयर ने इस शब्द का प्रयोग किया और उसके अर्थ को ‘आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास’ तक सीमित रखने का प्रयास किया। डा० नगेन्द्र के शब्दों में ‘‘इतिहास-दर्शन’ को हमें उसी व्यापक एवं समन्वित अर्थ मे ग्रहण करना होगा। जिसके अनुरूप ‘इतिहास-दर्शन’ उन दृष्टिकोणो, विचारों एवं अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है, जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन मे संभव है।’’
साहित्येतिहास की परिभाषा और स्वरूप
साहित्येतिहास व्िाâसी भाषा के साहित्य के आरंभिक काल से लेकर आज तक के विकास की यात्रा को प्रस्तुत करता है। इसलिये साहित्येतिहास को इतिहास से अलग करके नहीं समझा जा सकता । डा० गणपति चन्द्र गुप्त के अनुसार ‘‘साहित्येतिहास की विकासवादी व्याख्या के लिय उन सभी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है, जो साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उससे सम्बन्धित पूर्व परंपरा, युगीन वातावरण, द्वन्द के स्तोत्र, अभीष्ट लक्ष्य आदि पर प्रकाश डालते है। साहित्येतिहास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए डा० मैनेजर पाण्डेय कहते है-‘‘साहित्य के इतिहास का आधार है, साहित्य के विकासशील स्वरूप की धारणा।’’ साहित्य की प्रगति, निरंतरता और विकाशीलता मे आस्था के बिना साहित्य का इतिहास असंभव है।’’ डा हरमहेन्द्र सिंह बेदी के अनुसार ‘‘ साहित्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे विकासात्मक एवं तर्क संगत अध्ययन, अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर साहित्येतिहास की विशेषतायें निम्नांकित है-
१ साहित्येतिहास केवल लेखकों और उनकी कृतियों का अध्ययन न होकर युग-विशेष की समूहगत कृतियों का समन्वित अध्ययन होता है।
२ साहित्येतिहास में कारण कार्यमूलक संबंध का निर्धारण किया जाता है।
३ साहित्येतिहास में युग तथा साहित्यिक प्रवृतियों के विकास की चेतना का अनुसंधान होता है।
४ साहित्येतिहास मे निहित अनेकता मे एकता के सूत्र की खोज की जाती है।
५ साहित्य के इतिहास मे साहित्य के परिवर्तित रूप-तत्तवों और भाषायी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
साहित्येतिहास-दर्शन के प्रमुख तत्व
फे्रंच इतिहासकार ‘तेन’ ने अपने साहित्येतिहास मे प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृतियो के मूल मे मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व सक्रिय रहते है-जाति, वातावरण, क्षण विशेष। साहित्येतिहास को समझने के लिये उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन-विश्लेषण आवश्यक है।’’
‘हडसन’ ने इस मत की आलोचना यह कहकर कि है कि इसमें कृतिकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की उपेक्षा की गई है।
जर्मन चिन्तको की दृष्टि मे भी साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिये।
कारलाईल के अनुसार ‘‘किसी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वंहा के धर्म, राजनीति और विज्ञान के इतिहास का सार होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमागत दिशा और विकास को देखना अत्यन्त आवश्यक है। इससे राष्ट्र का निर्माण होता है।’’
डा. गणपति चन्द्र गुप्त ने साहित्येतिहास-दर्शन व साहित्य की विकास-प्रक्रिया के सामान्य पांच सूत्र प्रतिपादित किये है।
१ प्राकृतिक सृजन शक्ति
२ परम्परा
३ वातावरण
४ द्वन्द या आकर्षण-विकर्षण
५ सन्तुलन
प्राकृतिक सृजन शक्ति साहित्यकार की प्रतिभा से जुडी होती है। प्रतिभा व उसके व्यक्तित्व को जाने बिना साहित्यकार की सृजन शक्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसीलिये साहित्येतिहास दर्शन व साहित्य की विकास प्रक्रिया मे साहित्यकार की सृजन शक्ति, उसकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की भूमिका महत्वपूर्ण हुआ करती है।
जिस प्रकार जीवो की उत्पति एवं विकास मे उनकी पूर्व वंश परम्परा का आधार होता है, उसी प्रकार साहित्य की रचनाओं, धाराओं एवं कृतियों के विकास मे साहित्य की सम्यक व्याख्या उससे सम्बन्धित पूर्ववर्ती परंपराओं के अध्ययन के बिना संभव नहीं। यदि हम भक्तिकाल में बहने वाली भक्ति की निर्गुण-सगुण भक्ति का उत्स खोजने का प्रयास करे, तो उसके सूत्र ७वी-८वी शताब्दि के दक्षिण मे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से जुडे मिलते है। अतः साहित्येतिहास-दर्शन के विकास मे परंपरा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। द्वन्द या आकर्षण-विकर्षण को स्वतंत्र सूत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये रचनाकार की सृजनशील मानसिकता के ही अंग होते है। ‘द्वन्द में यदि कवि-मानव का युगीन परिवेश से विकर्षण, विद्रोह या टकराव होता है तो ‘संतुलन’ में शाश्वत जीवन-मूल्यों की खोज होती है। इन दोनों तत्वों को मूल चेतना का नाम दिया जा सकता है। अतः वर्तमान मे साहित्येतिहास-दर्शन के चार सूत्र प्रतिभा, परंपरा, युगीन परिवेश और मूल्य चेतना माने जाते है, जिनके आधार पर साहित्य का मानक इतिहास लिखा जा सकता है।
इससे स्पष्ट होता है कि साहित्य का इतिहास आलोचना नहीं है। इतिहासकार कृति का मूल्यांकन युगीन प्रवृतियों के संदर्भ मे करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। आलोचना मे जंहा मूल्यांकन पर बल दिया जाता है,वही इतिहास मे युगीन प्रवृतियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साहित्येतिहास लेखन एक जटिल प्रक्रिया है। साहित्यिक-कृतियां तथा अन्य तथ्य तो साहित्येतिहास लेखन के लिये उपकरण मात्र है। इन उपकरणों की सहायता से साहित्येतिहास लेखक अपने साहित्येतिहास को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। एक युग की विभिन्न एवं असंबद्व लगने वाली विभिन्न रचनाओं के मध्य एक सूत्रता की तलाश करता है। इस तलाश के लिये वह साहित्येतिहास के विकास की विभिन्न सूत्रों की सहायता करता है। यही साहित्येतिहास-दर्शन है।
डॉ. गायत्री कोंपल ‘‘चन्नाया’

 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0