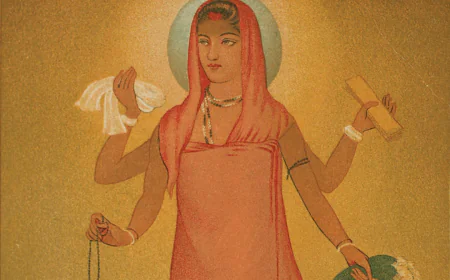संत साहित्य में रहस्यवाद
संत साहित्य के अंदर रहस्यवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रहस्यवाद का प्रभाव संत साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देता है। रहस्यवाद एक विशेष प्रकार की भावना है जो आध्यात्मिक और जीवन के रहस्यों को अनुभव करने की दिशा में जाता है। यह भावना संत साहित्य में अद्वैतवादी और भक्तिमार्गी सिद्धांतों के साथ जुड़ी होती है। अद्वैतवाद के अनुसार जगत् मिथ्या है। भ्रान्ति, अविद्या तथा अज्ञान के कारण जीव मिथ्या संसार को सत्य मान लेता है। इस दर्शन के अनुसार वास्तविक रूप में न तो किसी संसार की उत्पत्ति हुई, न कोई प्रलय आई। सत्य केवल ब्रह्मा है इसके अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है सब मिथ्या है।

संत साहित्य, भारतीय साहित्य की एक अद्वितीय धारा है जो आध्यात्मिकता, भक्ति और जीवन के रहस्यों को अपने शब्दों में व्यक्त करती है। मानव-मानव के मध्य जब मानवता का अतीत लोप हो चला था, मानवीय सद्वृत्तियाँ - प्रेम, क्षमा, करुणा, शील, सेवा, विनय, त्याग एवं अहिंसादि चिरंतन मूल्य जब लुप्तप्राय होते प्रतीत हुए, ऐसे संक्रांति-युग में मध्यकालीन चिरंतन भक्ति की जो भागीरथी प्रवाहित हुई उसने मानव में मानवता का संचार किया। निर्गुण भक्तिधारा प्रवाहित कर, रहस्यवाद एवं भक्तिवाद के राम-नामामृत में डुबोकर विच्छिन्न मानव-समुदाय में भावनात्मक एकत्व का मृदु संचार किया। निराकार ब्रह्म के प्रतीक रूप में धर्म, नीति, मानवता, मर्यादा, सत्य, शील, सदाचार एवं लोककल्याणपरक दिव्य मानवीय सद्गुणों का समारोहपूर्ण समावेश करके जनमानस में अपूर्व शक्ति, शील एवं सौंदर्यपरक आदर्श बना दिए।
संत साहित्य के अंदर रहस्यवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रहस्यवाद का प्रभाव संत साहित्य में विशेष रूप से दिखाई देता है। रहस्यवाद एक विशेष प्रकार की भावना है जो आध्यात्मिक और जीवन के रहस्यों को अनुभव करने की दिशा में जाता है। यह भावना संत साहित्य में अद्वैतवादी और भक्तिमार्गी सिद्धांतों के साथ जुड़ी होती है। अद्वैतवाद के अनुसार जगत् मिथ्या है। भ्रान्ति, अविद्या तथा अज्ञान के कारण जीव मिथ्या संसार को सत्य मान लेता है। इस दर्शन के अनुसार वास्तविक रूप में न तो किसी संसार की उत्पत्ति हुई, न कोई प्रलय आई। सत्य केवल ब्रह्मा है इसके अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है सब मिथ्या है। अद्वैतवाद वह दर्शन है जो ईश्वर को न एक मानता है और न ही अनेक। इसके अंतर्गत ईश्वर को "अगम, अगोचर, अचिन्त्य, अलक्षण तथा अनिर्वचनीय" माना जाता है। अद्वैतवाद का ब्रह्मसूत्र है- अहं ब्रह्मास्मि। इसके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म या ईश्वर अलग-अलग नहीं हैं। यह संसार ब्रह्म की माया है। जीव संसार में व्याप्त अज्ञान के कारण ही ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है जबकि ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करता है। मात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार करने के कारण इस दर्शन को अद्वैतवाद की संज्ञा दी गई।
संत साहित्य, भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रहस्यवाद का विशेष स्थान है। संत कवियों ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान को रचनाओं में व्यक्त किया है, जिसमें प्रेम, भक्ति, आत्म-साक्षात्कार और परमात्मा से मिलन का भाव निहित है।
रहस्यवाद अपने में बहुत ही व्यापक विषय है। जहां तक हम बात करें हिंदी काव्यधारा की तो उसमें रहस्यवाद अपनी अलग ही पहचान रखता है। रहस्यवाद वह भावनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें कोई साधक या ये कहें कि कोई रचनाकर उस अलौकिक, परम, अव्यक्त सत्ता से अपने प्रेम को प्रकट करता है और साथ ही उस अलौकिक तत्व में डूब जाना चाहता है। वास्तव में व्यक्ति जब इस परम आनंद की अनुभूति करता है। तो उसको वाह्य जगत में व्यक्त करने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पडता है, क्योंकि लौकिक भाषा, वस्तुएं उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकती, जो उसने पाया है इसलिए कवि, रचनाकार या अन्य कोई भी साधक उस पारलौकिक आनंद को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेता है, जो एक साधारण जन के लिए रहस्य बन जाते है। रहस्य का अर्थ है - ऐसा तत्त्व जिसे जानने का प्रयास करके भी अभी तक निश्चित रूप से कोई जान नहीं सका। ऐसा तत्त्व है परमात्मा। काव्य में उस परमात्म-तत्त्व को जानने की, जानकर पाने की और मिलने पर उसी में मिलकर खो जाने की प्रवृत्ति का नाम है - रहस्यवाद।
हिंदी काव्य और उसमें आए रहस्यवाद के विषय में विचारकों ने अपने अलग-अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार – “जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, उसे रहस्यवाद कहते हैं”। इसी बात को स्पष्ट करते हुए डॉ० श्याम सुन्दर दास ने लिखा है कि – “चिन्तन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर रहस्यवाद का रूप पकड़ता है”। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद के मतानुसार – “रहस्यवाद में अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अहं का इदं से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है”। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली रहस्यवादी कवयित्री महादेव वर्मा ने, “अपनी सीमा को असीम तत्त्व में खो देने को रहस्यवाद कहा है”। डॉ० रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता”।
वास्तव में रहस्यवाद काव्य की वह मार्मिक भावाभिव्यक्ति हैं, जिसमें एक भावुक कवि अव्यक्त, अगोचर एवं अज्ञात सत्ता के प्रति अपने प्रेमोद्गार प्रकट करता है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद पर प्रकाश डालें या रहस्यवाद के विषय में चर्चा करे तो हम पाते हैं कि यह परंपरा मध्य काल से शुरु हुई, निर्गुण काव्यधारा के संत कबीर के यहाँ तो प्रेममार्गी काव्यधारा या सूफी काव्यधारा में जायसी के यहाँ रहस्यवाद का प्रयोग हुआ है। विचार करें तो ये दोनों ही परम सत्ता से जुड़ना चाहते हैं और उसमे लीन होना चाहते हैं, कबीर योग के माध्यम से तो जायसी प्रेम के माध्यम से। विद्वानों की माने तो कबीर का रहस्यवाद अंतर्मुखी व साधनात्मक रहस्यवाद है और जायसी का रहस्यवाद बहिर्मुखी व भावनात्मक है। ऐसा नहीं है कि केवल इन दो ही कवियों ने रहस्यवाद पर अपनी लेखनी चलाई, बल्कि अन्य कवियों ने भी इसे अपनाया है। मध्यकाल से चली यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही है।
साधारणतया एक ही होने पर भी हम मध्य कालीन रहस्यवाद को दो शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर का रहस्यवाद और उसी काल की प्रेम मार्गी निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी का रहस्यवाद, दोनों ही कवियों के रहस्यवाद का मूल ईश्वरानुभूति है, किन्तु कबीर यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी करके अपने अन्दर ही ईश्वरानुभूति प्राप्त करते हैं और जायसी की दृष्टि ईश्वर के लिये घनीभूत तथा तीव्र प्रेम के कारण इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि वे सम्पूर्ण चराचर सृष्टि में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करने लगते हैं। संसार का सम्पूर्ण सुख-दुःख उन्हें चिरसुन्दर चिरन्तन तत्व के संयोग वियोग का सुखःदुःख प्रतीत होता है।
कबीर पहले यम नियम द्वारा मन तथा शरीर को पवित्र करते हैं। फिर आसन और प्राणायाम द्वारा शरीर तथा प्राणवायुको साधकर पूर्णतया अपने वश में करते हैं फिर प्रत्याहार और धारणा द्वारा सब स्थूल तथा सूक्ष्म इंद्रियों को उनके कार्यों से अलग हटाकर चित्त के अनुकूल करते हैं और एकाग्रचित्त द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार कमल में अवस्थित कुण्डलिनी को जागृत करके ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। और फिर जब ध्यान और समाधि की अवस्था में कुण्डलिनी जागृत होकर ब्रह्मरन्ध्र में पहुंच जाती है, तब वे ईश्वरानुभूति प्राप्त करते हैं और अमृतवर्षा, बिजली की चमक, सैकड़ों सूर्य के प्रकाश और अलौकिक स्वर्गीय संगीत आदि प्रतीकों द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हैं। उस अनुभूति के अभिव्यक्तिकरण में ही उनकी रहस्यवादी रचनाओं की सृष्टि होती है।
जायसी अपने हृदय के प्रेम को तीव्र, व्यापक और घनीभूत बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी साधना में एक समय आता है जब उनके लिये चराचर सृष्टि का सौन्दर्य उसी अमित चिरन्तन सौन्दर्य की प्रतिच्छाया हो उठता है और उनके हृदय की सम्पूर्ण रागात्मक प्रवृत्तियां उसी एक तत्व का आधार लेकर नाना रंगों सुगंधों के कलि-कुसुमों में प्रस्फुटित हो उठती हैं। वही अनुभूति उनके रहस्यवाद का मूल है।
कबीर ने मनुष्य की धन-संचय की स्वार्थी प्रवृत्ति पर भी चोट की है। आज समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की कसौटी मानव मूल्य न होकर केवल धन होता जा रहा है। हमारे सभी सामाजिक संबंधों और पारिवारिक रिश्तों पर अर्थतंत्र हावी हो गया है। प्रत्येक मनुष्य धन के पीछे बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। फलतः किसी के भी मन में ‘समाधान’ नदारद है। अतः कबीर ने मध्यकाल में ही मनुष्य की इस लोभी प्रवृत्ति पर चोट की है-
सांई इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए।
मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए॥
संवेदना की भाँति शिल्प के स्तर पर भी संत काव्य क्रांतिकारी व परिवर्तनशील मानसिकता का प्रतीक है। भाषा का ही उदाहरण लें। चूँकि, संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे इसलिये उनकी भाषा में भिन्न-भिन्न स्थानों के शब्द जुड़ गए हैं। ऐसी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है। हठयोग के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग हुआ है। ये (अन्तस्साधनात्मक) अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियाँ हैं-
बरसै कंबल भीजै पानी।
संतों का सारा साहित्य मुक्तकों के रूप में उपलब्ध है। जिस अमूर्त की चर्चा उन्होंने की और जिन अन्तः साधनात्मक अनुभूतियों को वे अभिव्यक्त करना चाहते थे, उनके लिये मुक्तक शैली ही उपयुक्त थी। रहस्यवाद मे चिंतन की प्रधानता हैं जबकि छायावाद मे कल्पना की प्रधानता हैं। रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धितत्व की प्रधानता हैं जबकि छायावाद मे भावना की प्रधानता हैं। रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है जबकि छायावाद के मूल मे प्रकृति है। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में रहस्यवाद के विभिन्न रूपों को व्यक्त किया है। इन रचनाओं का भारतीय साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भी संत साहित्य लोगों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
डॉ. रवीन्द्र कुमार दीक्षित
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0