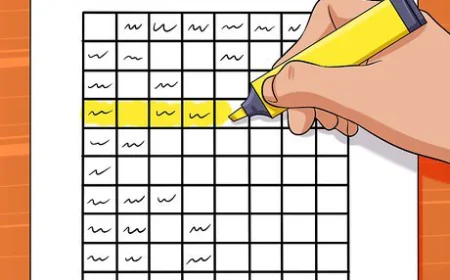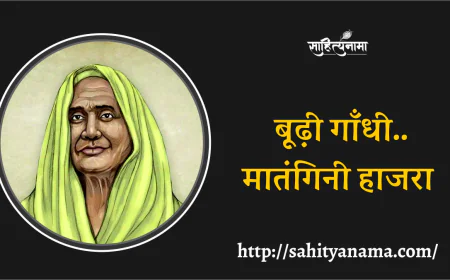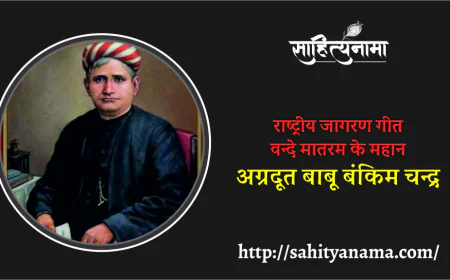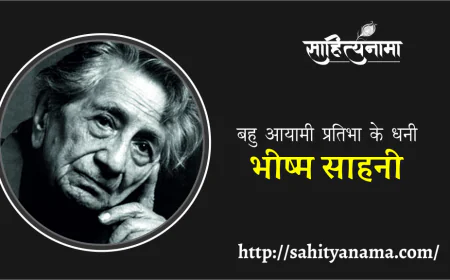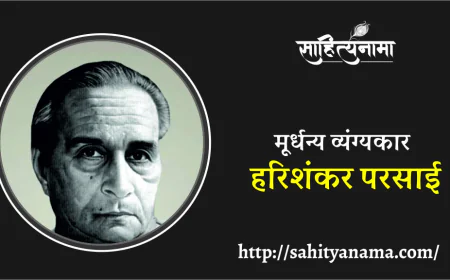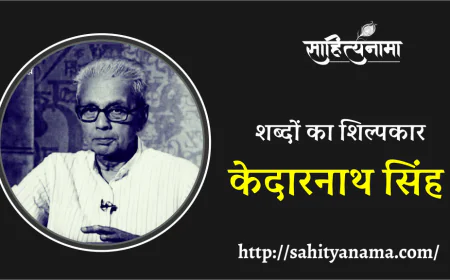Jaishankar Prasad in hindi : युग प्रवर्तक साहित्यकार : जयशंकर प्रसाद
जयशंकर प्रसाद विचार मंच,राँची के सचिव और प्रख्यात साहित्यकार सुरेश निराला जी लिखते है- "जयशंकर प्रसाद युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। उनका रचनाकाल 1909 ईस्वी से1936 ईस्वी तक माना जाता है।यह वह समय था जब भारत अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए कसमसा रहा था।भारत की अध्यात्मवादी जीवन दृष्टि और पश्चिम की सुधारवादी विचार धाराओं का टकराव चल रहा था।ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद ने अपनी सशक्त लेखनी से सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना को नई गति दी।उन्होने अपनी लेखनी से न केवल काव्य जगत को आलोकित किया ,बल्कि गद्य साहित्य में भी श्रेष्ठ रचनाएं की।" वे हिन्दी नाट्य जगत ,कथाऔर उपन्यास विधाओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं । तितली ,कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप , मधुआ ,पुरस्कार जैसी कहानियाँ उनके गद्य लेखन की विशिष्ट धरोहर हैं। वे एक प्रसिद्ध नाटककार और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं।उन्होंने अपने जीवन काल में बारह नाटकों की रचना की।अजातशत्रु , स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके अलावा पाँच कहानी संग्रह- छाया , प्रतिध्वनि,आकाशदीप, आँधी, इन्द्रजाल प्रकाशित हुए।
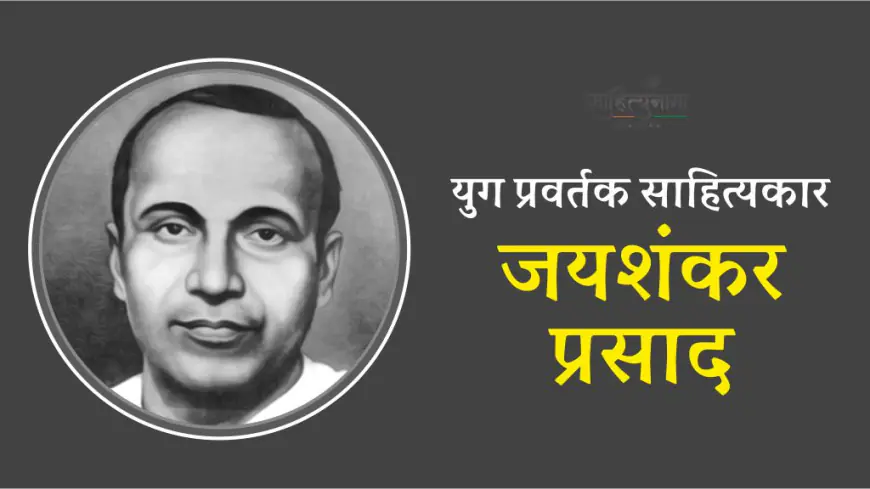
Jaishankar Prasad in hindi : जयशंकर प्रसाद विचार मंच,राँची के सचिव और प्रख्यात साहित्यकार सुरेश निराला जी लिखते है- "जयशंकर प्रसाद युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। उनका रचनाकाल 1909 ईस्वी से1936 ईस्वी तक माना जाता है।यह वह समय था जब भारत अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए कसमसा रहा था।भारत की अध्यात्मवादी जीवन दृष्टि और पश्चिम की सुधारवादी विचार धाराओं का टकराव चल रहा था। ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद ने अपनी सशक्त लेखनी से सम्पूर्ण राष्ट्रीय चेतना को नई गति दी।उन्होने अपनी लेखनी से न केवल काव्य जगत को आलोकित किया ,बल्कि गद्य साहित्य में भी श्रेष्ठ रचनाएं की।" वे हिन्दी नाट्य जगत ,कथाऔर उपन्यास विधाओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं । तितली ,कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप , मधुआ ,पुरस्कार जैसी कहानियाँ उनके गद्य लेखन की विशिष्ट धरोहर हैं। वे एक प्रसिद्ध नाटककार और निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं।उन्होंने अपने जीवन काल में बारह नाटकों की रचना की। अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके अलावा पाँच कहानी संग्रह- छाया , प्रतिध्वनि,आकाशदीप, आँधी, इन्द्रजाल प्रकाशित हुए।
प्रख्यात साहित्यकार और प्राध्यापक शिवानी सक्सेना लिखती हैं- " जयशंकर प्रसाद अपने गद्य साहित्य में इतिहास और कल्पना का अद्भुत सामंजस्य स्थापित करते हैं । वे इतिहास के चरित्रों में कल्पना का संयोग करके जो कथा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।,उसकी गूंज हमें उसके समकालीन समय की अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इसका एक उदाहरण हमें चन्द्रगुप्त नाटक में दिखाई पड़ता है,जब एक विदेशी पात्र कार्नेलिया से भारत की प्रशंसा में यह गीत प्रस्तुत करवाते हैं-
"अरूण यह मधुमय देश हमारा
जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को मिलता है सहारा "
' हिमाद्रि तुंग श्रृंग से ' गीत को ' चन्द्रगुप्त ' नाटक (1931 ईस्वी)
से लिया गया है। इस गीत को नाटक की प्रमुख पात्र अलका गाती है-
"हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती।
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती।।
अमर्त्य वीर पुत्र हो , दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो।
प्रशस्त पुण्य पंथ है ,बढ़े चलो बढ़े चलो।।
असंख्य कीर्ति रश्मियाँ ,
विकीर्ण दिव्य दाह-सी ।
सपूत मातृभूमि के,
रूको न शूर साहसी ।।
अराति सैन्य सिन्धु में , सुबाड़वाग्नि से जलो ।
प्रवीर हो जयी बनो ,बढ़े चलो ,बढ़े चलो।। "
यह गीत वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। काव्य-जगत में तो उनकी कीर्ति कस्तूरी की गंध की तरह सभी दिशाओं में फैलती चली गई। उनकी एक गेय कविता 'बीती विभावरी जाग री' में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रण करते हुए उषा का मानवीकरण किया गया है।
'बीती विभावरी जाग री।
अंबर - पनघट में डुबो रही-
तारा- घट उषा नागरी।
खग- कुल कुल - कुल- सा बोल रहा,
किसलय का अंचल डोल रहा,
लो यह लतिका भी भर लाई-
मधु- मुकुल नवल रस गागरी ।
अधरों में राग अमंद पिए ,
अलकों में मलयज बंद किए,
तू अब सोई है आली!
आँखों में भरे विहाग री!
महाकवि प्रसाद ने यहाँ उषा का मानवीकरण करते हुए संकेत किया है कि सभी सामर्थ्य रहते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है? तो फिर सोओ मत,जागो। उनकी इन पंक्तियों को पढ़िए-
" जिसके अरूण कपोलों
की मतवाली सुंदर छाया में
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में
उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की
सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की--------"
यह कविता 'हंस' के प्रसिद्ध आत्मकथा अंक में छपी थी ।इस कविता में एक तरफ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ उनकी विनम्रता भी।हिन्दी साहित्य में वे आधुनिक बोध और संवेदना के कवि हैं। छायावादी कवियों के आधुनिकता बोध में वैयक्तिक चेतना के साथ नयी सौंदर्य चेतना, नयी नैतिक चेतना, नयी प्रेम चेतना का संश्लिष्ट रूप देखा जा सकता है। डॉक्टर देवराज मानते हैं कि छायावाद अनाधुनिक पौराणिक- धार्मिक चेतना के विरूद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं कि नयी छायावादी काव्यधारा भी एक आध्यात्मिक पक्ष है ,परन्तु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय है। (आधुनिक हिन्दी समीक्षा / निर्मला जैन : प्रेमशंकर, पृष्ठ 82)
इस प्रकार छायावाद में लौकिक मानवीय संस्पर्श वाली कविता का अनादर नहीं है।यह जरूर है कि छायावादी कवियों के यहाँ लौकिक- मानवीय अनुभव पर अस्पष्टता का पर्दा पड़ा रहा है।जैसा प्रसाद की कृति 'आँसू' में देखा गया, या लहर की कई कविताओं में । इन कृतियों में प्रसाद संकेत से बहुत कुछ कह जाते हैं और ऐसी वेदना के चित्र भी उपस्थित कर जाते हैं जो लौकिक मानवीय है।प्रसाद जैसे कवि के आधुनिकताबोध को नयी सौंदर्य चेतना के आधार पर पहचानना होगा।यह सौंदर्य दृष्टि प्रकृति और मनुष्य के बीच नए संबंधों की पहचान में भी प्रकट हुई है।इसी नयी सौंदर्य चेतना के कारण अनुभव के स्तर पर एक नए प्रकार के आंतरिक द्वन्द्व का भी पता चलता है।अनुभव की प्रणाली और अभिव्यक्ति रूपों में जो नवीनता दिखाई देती है,उसे आधुनिक बोध से संबद्ध करके देखने की जरूरत है।' कामायनी ' के मनु के भीतर जो उद्विगनता है वह एक आधुनिक मन की उद्वगिनता जान पड़ती है :
'दुख का गहन पाठ पढ़कर अब
सहानुभूति समझते थे
नीरवता की गहराई में
मग्न अकेले रहते थे '
प्रसाद की भाषा में यहाँ एक विशेष प्रकार के नयेपन का आभास है। श्रद्धा मनुष्य को नूतनता के आनंद का रहस्य बताती है। कहा जा सकता है कि दुखवाद और आनंदवाद के द्वन्द्वपूर्ण साहचर्य में महाकवि ने आधुनिक बोध या आधुनिक संवेदना प्राप्त की। सचमुच 'कामायनी' आधुनिक बोध और संवेदना की महत्वपूर्ण फलश्रुति है। जलप्रलय की स्थिति में मनु का अकेलापन उन्हें जिन प्रश्नों से टकराने को बाध्य करता है , वे प्रश्न प्रायः आज के मनुष्य को बेचैन करते हैं :
' ओ चिंता की पहली रेखा ,
अरी विश्व - वन की व्याली
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण ,
प्रथम कंप - सी मतवाली
इस ग्रह कक्षा की हलचल री
तरल गरल की लघु लहरी
जरा अमर जीवन की , और न
कुछ सुनने वाली बहरी '
निस्संदेह ' कामायनी ' की आधुनिकता इसी से प्रकट है कि वह ' बड़े जीवन चक्रों ' की, जटिल राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं के बीच अभिव्यक्ति का प्रयास है। 'कामायनी ' एक अर्थ में सभ्यता- समीक्षा का काव्यात्मक प्रयास है। ' आँसू ' में महाकवि निजी वेदना को व्यापक रूप देते हुए आंतरिक तनाव को छिपाते नहीं हैं , फिर भीप्रेम के उदात्तीकरण का आदर्श उपस्थित करते हैं- उनकी आधुनिकता इसी तनाव में है।
' उसमें विश्वास घना था
उस माया की छाया में
कुछ सच्चा स्वयं बना था '
जयशंकर प्रसाद छायावाद के चार स्तम्भों (प्रसाद, पंत, निराला , वर्मा ) में प्रमुख हैं।महाकवि जयशंकर प्रसाद (1890-1937 )
का जन्म काशी के एक सम्पन्न घराने में हुआ था ,जो ' सुंघनी साहू ' के नाम से प्रसिद्ध था।इन्होंने आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिन्दी , उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। उन्हें इतिहास और दर्शन में विशेष रूचि थी।प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में कविता लिखना शुरू किए, परन्तु बाद में खड़ीबोली में कविता करने लगे।इनकी काव्य- कृतियों में भाषा , छन्द ,भाव आदि की दृष्टि से अनेकरूपता दिखाई देती है।कवि होने के साथ-साथ ये गंभीर चिंतक भी थे।इनकी आरम्भिक शैली बहुत कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय ' हरिऔध ' की संस्कृतगर्भित शैली से मिलती जुलती है,जो स्थूल और बहिर्मुखी है।छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले ' झरना ' (1918 ) में होते हैं।
इनकी अनेक कविताओं में अन्तर्मुखी कल्पना द्वारा सूक्ष्म भावनाओं को व्यक्त किया गया है।बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए भी इन्होनें उसके सूक्ष्म और मानसिक पक्ष को व्यक्त करने की ओर ध्यान दिया है। 'आँसू '(1925 ) का
आरम्भ कवि की विरह - वेदना
की अभिव्यक्ति से हुआ है :
' इस करूणा कलित हृदय में
अब विकल रागिनी बजती
क्यों हाहाकार स्वरों में
वेदना असीम गरजती ? '
इसके बाद ,
' सबका निचोड़ लेकर तुम
सुख से सूखे जीवन में
बरसो प्रभात हिमकण - सा
आँसू इस विश्व सदन में । '
इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि
महाकवि ने आरम्भिक व्यक्तिगत
वेदना को भूलकर अन्त में ' आँसू '
को विश्व- कल्याण की भावना के साथ सम्बद्ध कर लिया है । इस काव्य में कवि अन्त तक आते-आते अपने व्यक्ति- जीवन के नैराश्य और अवसाद से ऊपर उठकर अपनी वेदना को करूणा के रूप में , विश्व- प्रेम के रूप में रूपांतरित कर देता है।इसका कारण स्पष्ट है -छायावादी काव्य निराशावादी काव्य नहीं है ,वह मानव- समाज के लिए कल्याण की कामना से अलंकृत है।इसलिए छायावादी कवियों की व्यक्तिगत निराशा ही करूणा और विश्व- प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती है , जहाँ पहुँचकर कवि सारे संसार की वेदना को खुद स्वीकार करके विश्व - जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। इस दृष्टि से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि ' आँसू ' में प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकलकर विश्व- वेदना के साथ तादात्म्य स्थापित करती हुई मानव- जीवन को सुखी बनाने के लिए आकुल हो उठती है। ' लहर' ' (1933 ) में महावि की गीत- कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है।इन गीतों में कहीं तो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है , कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का ,कहीं करूणा की अभिव्यक्ति है तो कहीं रहस्यवादी संकेत दिखाई देते हैं।' लहर ' से ली गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए -
' मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी ,
मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी।
इस गम्भीर अनन्त नीलिमा में असंख्य जीवन- इतिहास ,
यह लो , करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य- मलिन उपहास। '
' ले चल वहाँ भुलावा देकर ' शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए-
' जिस गम्भीर मधुर छाया में ,
विश्व चित्र- पट चल माया में ,
विभुता विभु - सी पड़े दिखाई,
दुख- सुख बाली सत्य बनी रे।
श्रम- विश्राम क्षितिज - वेला से
जहाँ सृजन करते मेला से ,
अमर जागरण उषा नयन से
बिखरती हो ज्योति घनी रे। '
' मेरी आँखों की पुतली में ' शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए -
'मेरी आँखों की पुतली में
तू बन कर प्राण समा जा रे
जिससे कण कण में स्पंदन हो
वह जीवन गीत सुना जा रे। '
इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं-
'उर्वशी ' (1909 ) , ' वनमिलन '
(1909 ) , ' प्रेमराज्य '(1909 ) ,
' अयोध्या का उद्धार ' (1910) ,
शोकोच्छवास ' (1910) ,
' वभ्रुवाहन ' (1911 ) ,
' कानन - कुसुम '(1913 ) ,
' प्रेम पथिक ' (1913 ) ,
' करणालय ' (1913) ,
' महाराणा का महत्व ' (1914 ) ,
' कामायनी ' (1935 ) ।
' कामायनी ' महाकवि की अन्तिम कृति है । आलेख के प्रारम्भ में ही ' कामायनी ' का उल्लेख मैनें संदर्भ में किया है। इस महाकाव्य का आधार वह प्राचीन आख्यान है जिसके अनुसार मनु के अतिरिक्त सम्पूर्ण देव- जाति प्रलय का शिकार हो जाती है और मनु तथा श्रद्धा या कामायनी के संयोग से मानव सभ्यता का प्रवर्तन होता है इसका कथानक बहुत संक्षिप्त है, लेकिन कवि ने इसमें जीवन के अनेक पक्षों को समन्वित करके मानव- जीवन के लिए एक व्यापक
आदर्श व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया है।' कामायनी ' के एक संदर्भ का सम्बन्ध मनु और श्रद्धा के व्यक्तिगत -जीवन और प्रणय के साथ है।इड़ा के चरित्र का एक अंश भी इस प्रसंग से सम्बद्ध है।महाकवि ने इन प्रमुख पात्रों के
चरित्रांकन में मनुष्य की अनुभूतियों, कामनाओं और आकांक्षाओं की अनेकरूपता का वर्णन किया है। यह ' कामायनी ' की चेतना का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। महाकवि ने मनु आदि के माध्यम से मानव मात्र के मनोजगत के विविध पक्षों का चित्रण ' चिन्ता ' , ' आशा ' 'वासना ' , 'ईर्ष्या ' 'संघर्ष ' , 'आनन्द ' आदि सर्गों में किया है।' कामायनी ' में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय- तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए महाकवि ने शैव दर्शन के आनन्दवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन
माना है ,लेकिन इस कृति की आलोचना भी हुई है। 'अनेक विद्वानों का कहना है कि लोकमंगल की भावना को मुखरित करते हुए भी ' कामायनी ' की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी- अध्यात्मवादी चेतना है,जो अपने युग के यथार्थ की समस्याओं का यथार्थ के धरातल पर समाधान करने में असमर्थ रही है। ' (हिन्दी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेन्द्र ) फिर भी ' कामायनी ' अपनी सीमाओं के बावजूद हिन्दी - साहित्य की एक गौरवशाली उपलब्धि है।
- अरूण कुमार यादव
What's Your Reaction?
 Like
2
Like
2
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0