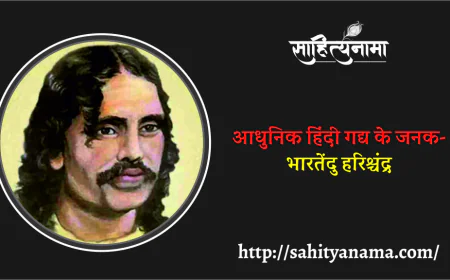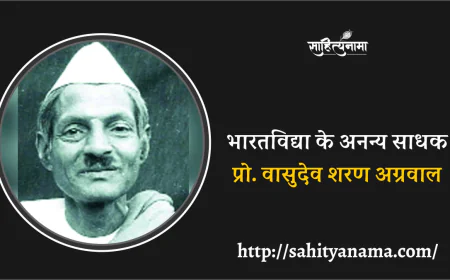लोकरंग की बहुआयामी सौगात : गवरी
गांव और नगर की सीमाएं अब मिटती जा रही है। अब तक हम समझते थे कि लोकनाट्यों के लिए गाँवो का विस्तृत क्षेत्र है, पर गाँवों की विद्युतीकरण की गति के साथ-साथ टी. वी., सिनेमा व साइबर दुनिया के प्रसार से भी इन लोक नाट्यों पर काफी घातक प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का अतिक्रमण इस हद तक बढ़ गया है कि हमारी अपनी सांस्कृतिक कला-निधि उपेक्षित होकर रह गई है।

अरावली की घाटियों में बसे राजस्थान के 'भील' वनवासियों का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। एकलव्य की संतान माने जाने वाले ये भील महाराणा प्रताप की गोरिल्ला फौज के बहादुर सैनिक थे। मेवाड़ राजवंश के राज-चिन्ह में भील को `भीलू राणा' के रूप में तीर-कमान लिए रक्षक के रूप में दिखाया गया है। अपने अंगूठे के रक्त से नये महाराजाओं के राजतिलक का विशेषाधिकार तक मिला हुआ था इन्हें।
राजस्थान के इन्हीं भीलों का परम्परागत लोकनाट्य है - `गवरी'।
गवरी को लोक-मानस में 'राई' के नाम से भी जाना-पहचाना जाता है। शिव और भस्मासुर की कहानी गवरी की मूल कथा मानी जाती है। गवरी में जो दृश्य अभिनित किये जाते हैं वे खेल, भाव अथवा सांग के नाम से पुकारे जाते हैं। गवरी के मूल में नृत्य की प्रधानता रही है जो आज भी देखी जा सकती है। प्रत्येक भील परिवार का सदस्य इसमें भाग लेना अपना नैतिक व धार्मिक कर्तव्य समझता है। फलतः गवरी में कलाकारों की संख्या चालीस-पचास से लगाकर सौ से भी ज्यादा तक हो जाती है।
मुहूर्त के अनुसार प्रायः रक्षाबंधन के बाद आने वाली ठण्डी राखी के दिन से ही गवरी प्रारम्भ हो जाती है जो लगभग ४० दिनों तक अनवरत चलती है। प्रत्येक भीली गांव में इस समय गवरी नाचना अनिवार्य-सा है। जिस गांव में गवरी नहीं ली जाती वहां वर्षा कम ज्यादा होने, अकाल पड़ने, भयंकर भूकम्प आने, आग लग जाने, चोरी-डाका पड़ने एवम् हरी-भरी खेती नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। ऐसी भील समुदाय की मान्यता है। भारत में कहीं भी ऐसा लोकनाट्य नहीं मिलेगा जो इतनी लंबी अवधी तक पात्रों के इतने बड़े समूह के साथ विविध गाँवो में इतने सुव्यवस्थित ढंग से सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रदर्शित किया जाता है।
इस नृत्य नाटिका में प्रमुख नायक बूड़िया है जिसे शिव का प्रतिक माना जाता है। इसके बदन पर भगवा साफा बंधा होता है। कमर में बड़े-बड़े घुंघरू बंधे रहते हैं। बूड़िया अपने मुँह पर भयानक मुखौटा बांधे रहता है। इसके हाथ में लकड़ी की बनी तलवार होती है। यह प्रत्येक स्वांग के पहले और अंत में दूसरे कलाकारों के विपरीत दिशा में नृत्य करता है। बूड़िये के साथ दो 'रायां' होती है, जिनमें अलौकिक शक्तियों का प्रवेश रहता है। वे मुँह को इस प्रकार बांधे रहती है कि केवल आँखें ही दिखाई पड़ती हैं। दो भोपे होते हैं जिनके गले में देवताओं के प्रतीक चिन्ह बंधे रहते हैं। ये हाथ में मोर-पंख, लोह-जंजीर आदि रखकर देवताओं से नृत्य परिसर में उपस्थित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं।
गांव का कोई मैदान, चौराया अथवा खुला आँगन ही गवरी का रंगमंच होता है। जहाँ-जहाँ गवरी वाले गांव की बहिन-बेटियां ब्याही हुई होती हैं, वहां-वहां इसके प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। गवरी में चार प्रकार के पात्र होते हैं जिनमें देवपात्र, मानव पात्र, दानव पात्र एवम् पशु पात्र होते हैं। देवपात्र सभी प्रकार के विकारों से रहित आदर्श के प्रतीक एवम् कालजयी होते हैं। कालका, शिव- पार्वती देव पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। गवरी में मानव पात्रों की बहुलता होती है जिनमें कंजर, नट, भोपा, संकरिया, बूड़िया, खेतूड़ी, देवर, भोजाई, बादशाह, बणियां, कानुगुजरी, कृष्ण आदि होते हैं। डाकण, भंवरा, हठिया, भियांवड़ तथा खड़ल्या भूत गवरी के दानव-पात्र हैं, इनका रूप भयानक होता है। सूअर, रीछ तथा शेर पशु पात्र होते हैं। गवरी में कभी पुरुष पात्र अपना शौर्य दिखाते हैं तो कभी अशुद्ध एवम् असत् वृत्तियों के दानव पात्र सृष्टि को अपने मनोनुकूल संचालित करने का प्रयत्न करने हैं एवं सृष्टि पर कब्जा करना चाहते हैं। गवरी में ये पात्र धाड़-फाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अंत में कालचक्र ऐसा आता है कि सभी नष्ट हो जाते हैं और देवसत्ता स्थापित हो जाती है।
गवरी धारण के पीछे मात्र मनोरंजन का उद्देश्य ही नहीं रहा और न ही आजीविका उपार्जन की भावना ही दृष्टिगोचर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य भीलों द्वारा अपने धार्मिक कर्तव्य की संपूर्ति तथा बाबा शिव को रिझाकर गांव की खुशहाली, जाति की सुरक्षा एवम् रोग-शोक, दुःख-दारिद्र तथा दुर्भिक्ष से छुटकारा पाने का रहा है।
गवरी में नृत्य की भी प्रधानता पाई जाती है। पात्रों में होने वाले संवाद बड़े नाटकीय एवम् मनोरंजक होते हैं। नृत्य के अलावा इसका गीत पक्ष भी बड़ा प्रबल होता है। कलाकारों की पोशाकें बड़ी कलात्मक सज्जा लिए पात्रों की भूमिका के अनुरूप होती है। इन्हें धारण कर पात्र अपने को साधारण व्यक्ति से अलग अनुभव करता है और सफलता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। गवरी में स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष ही अदा करते हैं। भीलों के जीवन में स्त्री-पुरुषों को बराबरी का अधिकार होते हुए भी गवरी में स्त्रियों का हिस्सा लेना वर्जित है। एक अतिशय धार्मिक एवम् ओजपूर्ण नृत्य होने के कारण इस दौरान स्त्रियों को पुरुषों के सहवास से अलग ही रखा गया है। प्रतिदिन नृत्योपरांत भी गवरी पात्र स्त्रियों से दूर ही रहते हैं। गवरी के दिनों में स्त्री गमन, मांस-मदिरा एवम् हरी सब्जी का सेवन भी गवरी पात्रों के लिए वर्जित है।
यह भी पढ़े:-भारत की नदियाँ : एक राष्ट्रीय परिदृश्य
`घलावण' और `बलावण' गवरी के अंतिम दिन होते हैं। ये दोनों दिन विशेष आयोजन के साथ मनाये जाते हैं। इस दिन गवरी पात्रों के सगे-सम्बंधी उनके लिए कपड़े आदि लाते हैं। मिठाइयां ख्िालाते हैं और एक त्यौहार की तरह इसे मनाते हैं।
लोक जीवन और संस्कृति किसी भी देश का वास्तविक दर्पण होती है और हमारा देश इस दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं जहां कितनी ही लोक परम्पराएं, संस्कृतियां, लोक भाषाएं जीवंत हैं। विभिन्नता में एकता का आभास भी इसी से होता है।
गांव और नगर की सीमाएं अब मिटती जा रही है। अब तक हम समझते थे कि लोकनाट्यों के लिए गाँवो का विस्तृत क्षेत्र है, पर गाँवों की विद्युतीकरण की गति के साथ-साथ टी. वी., सिनेमा व साइबर दुनिया के प्रसार से भी इन लोक नाट्यों पर काफी घातक प्रभाव पड़ता जा रहा है। आज भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का अतिक्रमण इस हद तक बढ़ गया है कि हमारी अपनी सांस्कृतिक कला-निधि उपेक्षित होकर रह गई है। इसके व्यवसायिक करण ने कमोबेस लोगों को इस कला से परिचय तो कराया पर यहां भी मूल स्वरूप खो जाता है। भूखे चेहरों वाले भील जन -जीवन के अशिक्षित मानस में विकृत संस्कृति के बीज बोए जा रहे हैं । विडम्बना है कि धीरे-धीरे लोकानुरंजन का यह माध्यम लुप्त होता जा रहा है। परम्परागत गवरी लोकनाट्य का स्वरुप बदल रहा है। फूहड़ पाश्चात्य संस्कृति इसे लगातार अपने बाहुपाश में लपेट रही है। गवरी का विनाश अत्यधिक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसे रोकना होगा, पर रोकेगा कौन? संस्कृति के मूल से यदि `लोक' का विलोप हो जाए तब वह उसी प्रकार जड़ हो जाती है जैसे प्राण के बिना देह।
यह सच है कि लोककलाएं प्रदर्शन के बिना जिन्दा नहीं रह सकती, और प्रदर्शन से उनकी कलाएं संवरती निखरती हैं, लेकिन इन कलाओं को सीख-समझकर उन्हें सरंक्षण देने वालों को सरंक्षण कहा है? हमें स्वयं व आने वाली पीढ़ी को लोक कलाओं से जोड़कर हर सम्भव हमारी महान विरासत को संरक्षित करना होगा। सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में व्यापक प्रयास होने चाहिए।
राजकुमार जैन राजन
चित्तौड़गढ़ राजस्थान
What's Your Reaction?
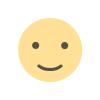 Like
0
Like
0
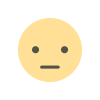 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
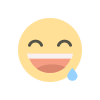 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
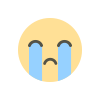 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0